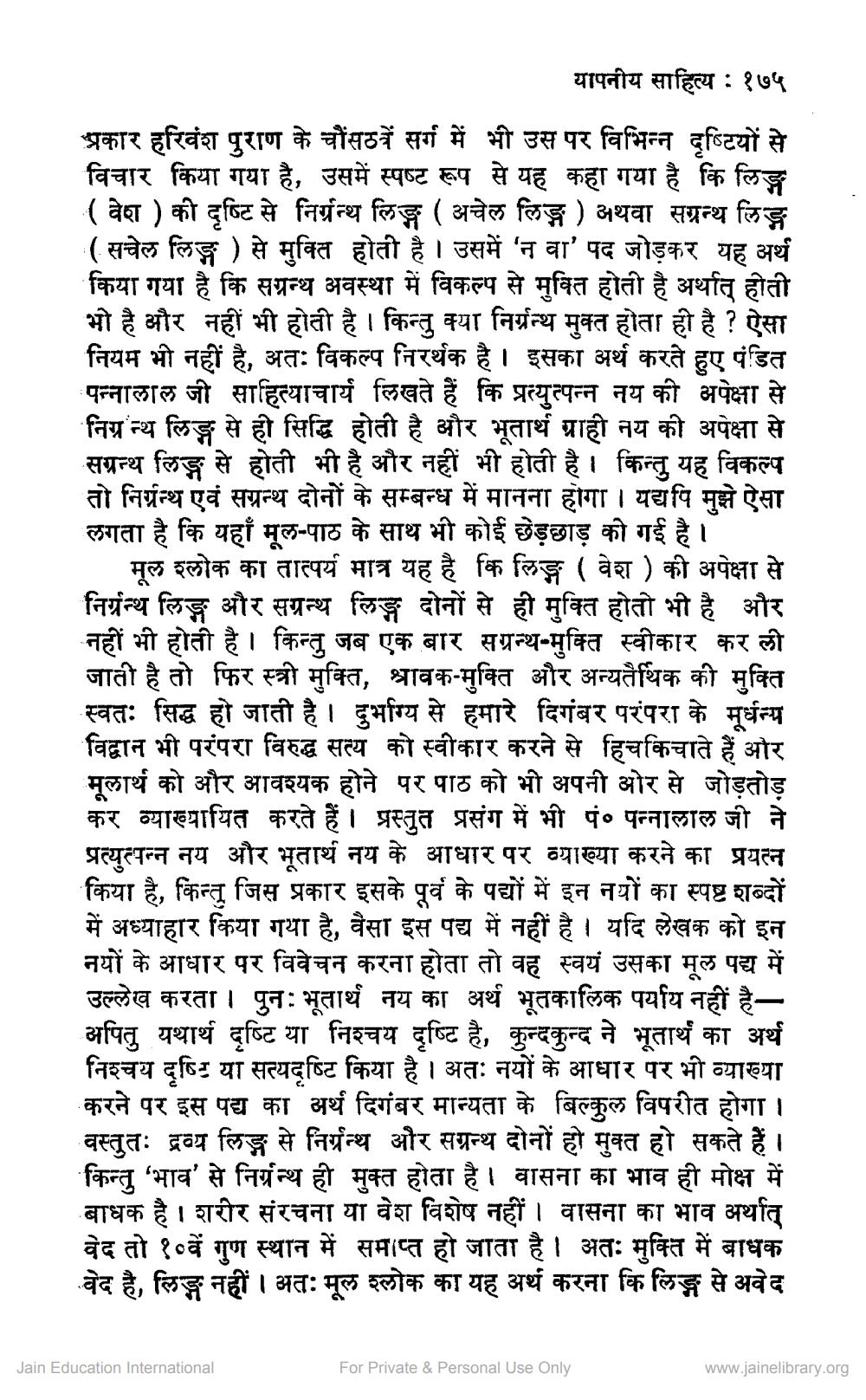________________
यापनीय साहित्य : १७५
प्रकार हरिवंश पुराण के चौंसठवें सर्ग में भी उस पर विभिन्न दृष्टियों से विचार किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि लिङ्ग ( वेश ) की दृष्टि से निर्ग्रन्थ लिङ्ग ( अचेल लिङ्ग ) अथवा सग्रन्थ लिङ्ग ( सचेल लिङ्ग ) से मुक्ति होती है। उसमें 'न वा' पद जोड़कर यह अर्थ किया गया है कि सग्रन्थ अवस्था में विकल्प से मुक्ति होती है अर्थात होती भी है और नहीं भी होती है । किन्तु क्या निम्रन्थ मुक्त होता ही है ? ऐसा नियम भी नहीं है, अतः विकल्प निरर्थक है। इसका अर्थ करते हुए पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य लिखते हैं कि प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से निग्रन्थ लिङ्ग से ही सिद्धि होती है और भूतार्थ ग्राही नय की अपेक्षा से सग्रन्थ लिङ्ग से होती भी है और नहीं भी होती है। किन्तु यह विकल्प तो निर्ग्रन्थ एवं सग्रन्थ दोनों के सम्बन्ध में मानना होगा । यद्यपि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मूल-पाठ के साथ भी कोई छेड़छाड़ को गई है।
मूल श्लोक का तात्पर्य मात्र यह है कि लिङ्ग ( वेश ) की अपेक्षा से निर्ग्रन्थ लिङ्ग और सग्रन्थ लिङ्ग दोनों से ही मुक्ति होतो भी है और नहीं भी होती है। किन्तु जब एक बार सग्रन्थ-मुक्ति स्वीकार कर ली जाती है तो फिर स्त्री मुक्ति, श्रावक-मुक्ति और अन्यतैर्थिक की मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। दुर्भाग्य से हमारे दिगंबर परंपरा के मूर्धन्य विद्वान भी परंपरा विरुद्ध सत्य को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं और मूलार्थ को और आवश्यक होने पर पाठ को भी अपनी ओर से जोड़तोड़ कर व्याख्यायित करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में भी पं० पन्नालाल जी ने प्रत्युत्पन्न नय और भूतार्थ नय के आधार पर व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, किन्तु जिस प्रकार इसके पूर्व के पद्यों में इन नयों का स्पष्ट शब्दों में अध्याहार किया गया है, वैसा इस पद्य में नहीं है । यदि लेखक को इन नयों के आधार पर विवेचन करना होता तो वह स्वयं उसका मूल पद्य में उल्लेख करता। पुनः भूतार्थ नय का अर्थ भूतकालिक पर्याय नहीं हैअपितु यथार्थ दृष्टि या निश्चय दृष्टि है, कुन्दकुन्द ने भूतार्थ का अर्थ निश्चय दष्टि या सत्यदष्टि किया है। अतः नयों के आधार पर भी व्याख्या करने पर इस पद्य का अर्थ दिगंबर मान्यता के बिल्कुल विपरीत होगा। वस्तुतः द्रव्य लिङ्ग से निर्ग्रन्थ और सग्रन्थ दोनों हो मुक्त हो सकते हैं। किन्तु 'भाव' से निर्ग्रन्थ ही मुक्त होता है। वासना का भाव ही मोक्ष में बाधक है। शरीर संरचना या वेश विशेष नहीं। वासना का भाव अर्थात् वेद तो १०वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है। अतः मुक्ति में बाधक वेद है, लिङ्ग नहीं । अतः मूल श्लोक का यह अर्थ करना कि लिङ्ग से अवेद
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org