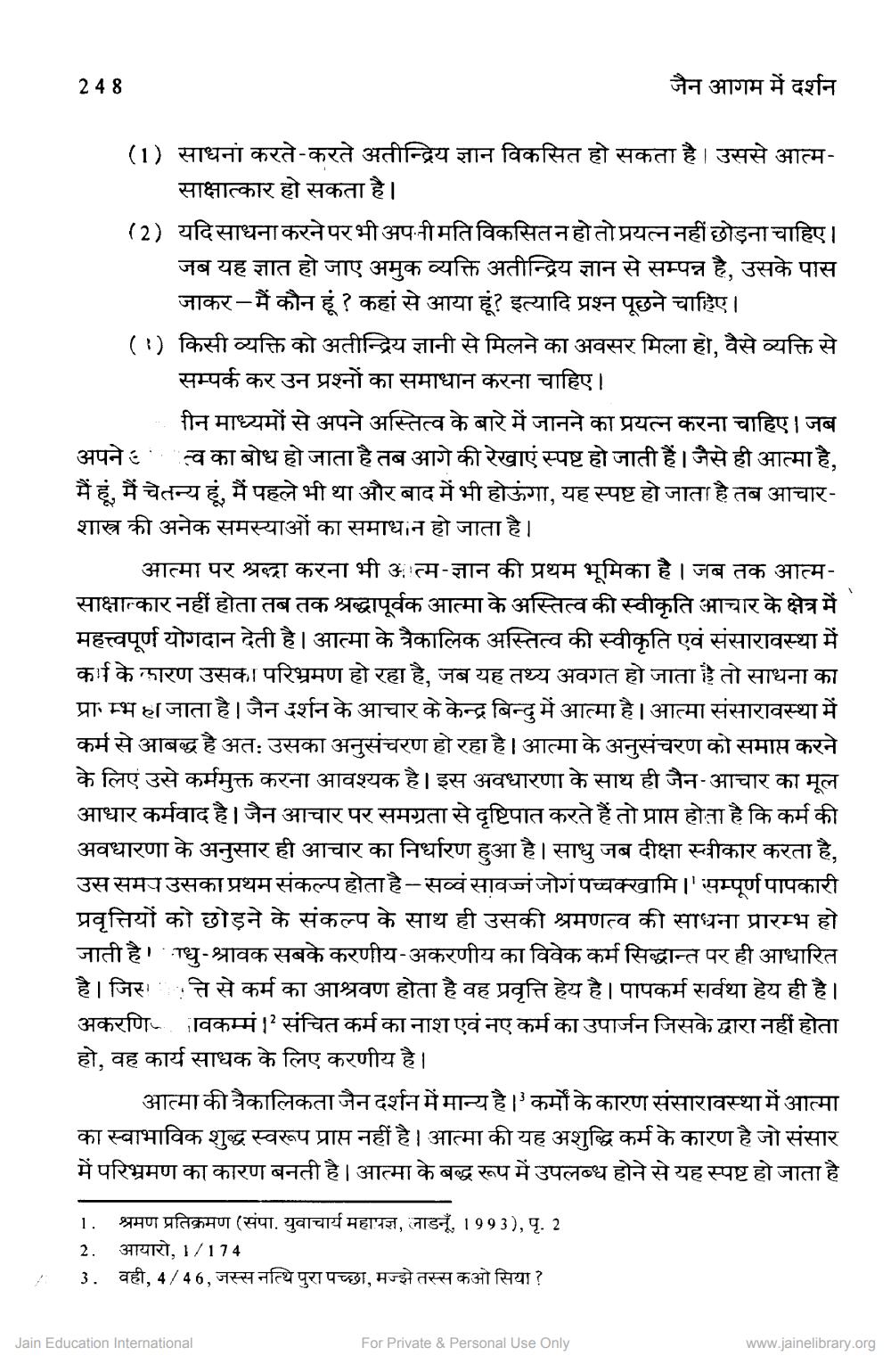________________
248
जैन आगम में दर्शन
(1) साधना करते-करते अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित हो सकता है। उससे आत्म
साक्षात्कार हो सकता है। (2) यदि साधना करने पर भी अपनीमति विकसितन होतो प्रयत्ननहीं छोड़ना चाहिए।
जब यह ज्ञात हो जाए अमुक व्यक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान से सम्पन्न है, उसके पास
जाकर-मैं कौन हूं ? कहां से आया हूं? इत्यादि प्रश्न पूछने चाहिए। (!) किसी व्यक्ति को अतीन्द्रिय ज्ञानी से मिलने का अवसर मिला हो, वैसे व्यक्ति से
सम्पर्क कर उन प्रश्नों का समाधान करना चाहिए।
तीन माध्यमों से अपने अस्तित्व के बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जब अपने ६ "त्व का बोध हो जाता है तब आगे की रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे ही आत्मा है, मैं हूं, मैं चेतन्य हूं, मैं पहले भी था और बाद में भी होऊंगा, यह स्पष्ट हो जाता है तब आचारशास्त्र की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है।
आत्मा पर श्रदा करना भी ॐ त्म-ज्ञान की प्रथम भूमिका है। जब तक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता तब तक श्रद्धापूर्वक आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृति आचार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व की स्वीकृति एवं संसारावस्था में कर्म के कारण उसका परिभ्रमण हो रहा है, जब यह तथ्य अवगत हो जाता है तो साधना का प्रा. म्भ हा जाता है। जैन दर्शन के आचार के केन्द्र बिन्दु में आत्मा है। आत्मा संसारावस्था में कर्म से आबद्ध है अत: उसका अनुसंचरण हो रहा है। आत्मा के अनुसंचरण को समाप्त करने के लिए उसे कर्ममुक्त करना आवश्यक है। इस अवधारणा के साथ ही जैन-आचार का मूल आधार कर्मवाद है। जैन आचार पर समग्रता से दृष्टिपात करते हैं तो प्राप्त होता है कि कर्म की अवधारणा के अनुसार ही आचार का निर्धारण हुआ है। साधु जब दीक्षा स्वीकार करता है, उस समय उसका प्रथम संकल्प होता है-सव्वं सावज्जोगंपच्चक्खामि । सम्पूर्ण पापकारी प्रवृत्तियों को छोड़ने के संकल्प के साथ ही उसकी श्रमणत्व की साधना प्रारम्भ हो जाती है। धु-श्रावक सबके करणीय-अकरणीय का विवेक कर्म सिद्धान्त पर ही आधारित है। जिस।त्ति से कर्म का आश्रवण होता है वह प्रवृत्ति हेय है। पापकर्म सर्वथा हेय ही है। अकरणि... विकम्म। संचित कर्म का नाश एवं नए कर्म का उपार्जन जिसके द्वारा नहीं होता हो, वह कार्य साधक के लिए करणीय है।
आत्मा की त्रैकालिकता जैन दर्शन में मान्य है। कर्मों के कारण संसारावस्था में आत्मा का स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं है। आत्मा की यह अशुद्धि कर्म के कारण है जो संसार में परिभ्रमण का कारण बनती है। आत्मा के बद्ध रूप में उपलब्ध होने से यह स्पष्ट हो जाता है
1. श्रमण प्रतिक्रमण (संपा. युवाचार्य महाप्रज्ञ, लाडनूं, 1 993), पृ. 2 2. आयारो, 1/174 3. वही, 4/46, जस्स नत्थि पुरा पच्छा, मज्झे तस्स कओ सिया?
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org