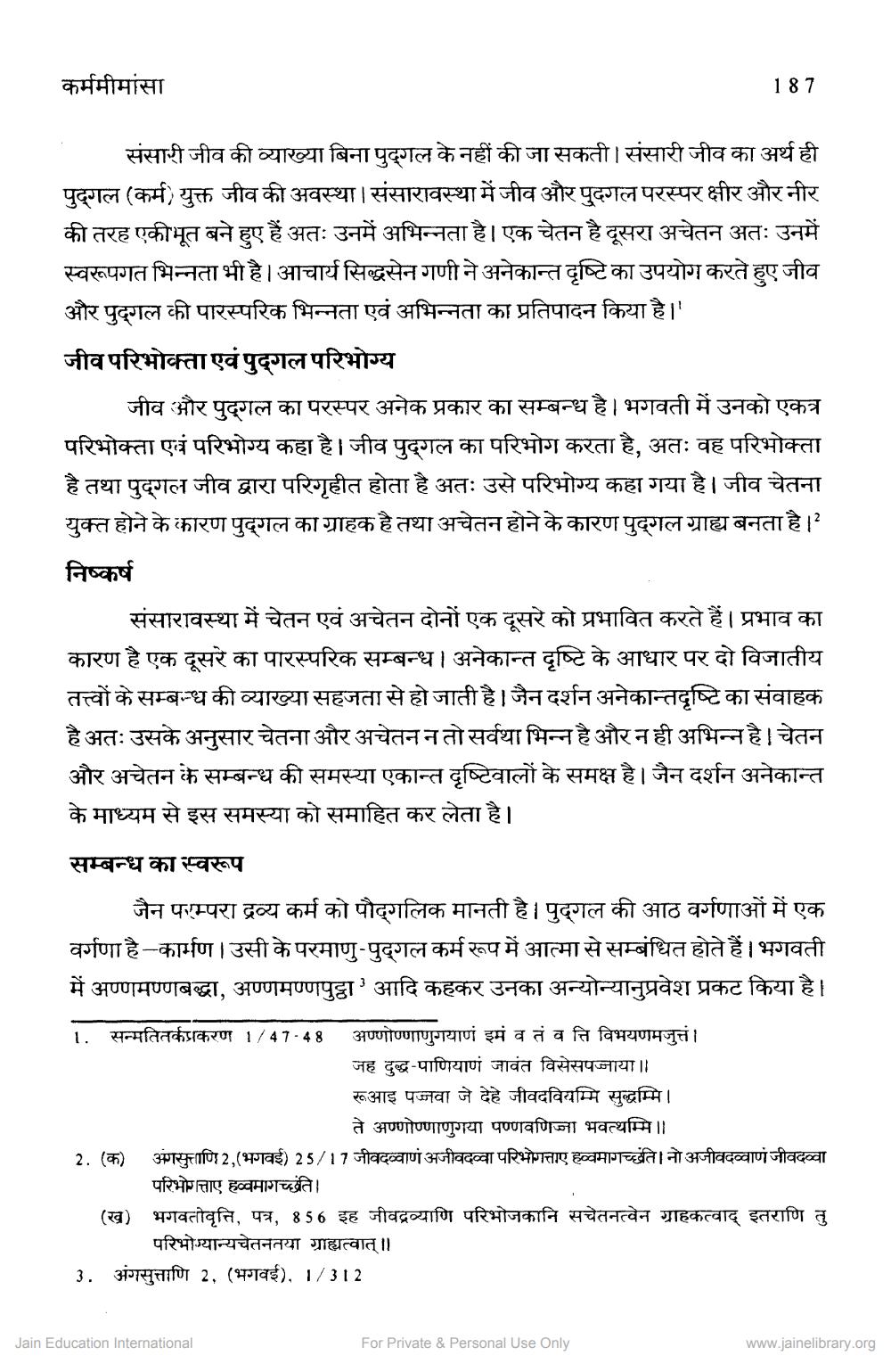________________
कर्ममीमांसा
संसारी जीव की व्याख्या बिना पुद्गल के नहीं की जा सकती। संसारी जीव का अर्थ ही पुद्गल (कर्म) युक्त जीव की अवस्था । संसारावस्था में जीव और पुदगल परस्पर क्षीर और नीर की तरह एक भूत बने हुए हैं अतः उनमें अभिन्नता है । एक चेतन है दूसरा अचेतन अतः उनमें स्वरूपगत भिन्नता भी है। आचार्य सिद्धसेन गणी ने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग करते हुए जीव और पुद्गल की पारस्परिक भिन्नता एवं अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। '
जीव परिभोक्ता एवं पुद्गल परिभोग्य
जीव और पुद्गल का परस्पर अनेक प्रकार का सम्बन्ध है । भगवती में उनको एकत्र परिभोक्ता एवं परिभोग्य कहा है। जीव पुद्गल का परिभोग करता है, अतः वह परिभोक्ता है तथा पुद्गल जीव द्वारा परिगृहीत होता है अतः उसे परिभोग्य कहा गया है। जीव चेतना युक्त होने के कारण पुद्गल का ग्राहक है तथा अचेतन होने के कारण पुद्गल ग्राह्य बनता है । ' निष्कर्ष
संसारावस्था में चेतन एवं अचेतन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभाव का कारण है एक दूसरे का पारस्परिक सम्बन्ध । अनेकान्त दृष्टि के आधार पर दो विजातीय तत्त्वों के सम्बन्ध की व्याख्या सहजता से हो जाती है। जैन दर्शन अनेकान्तदृष्टि का संवाहक है अतः उसके अनुसार चेतना और अचेतन न तो सर्वथा भिन्न है और न ही अभिन्न है। चेतन और अचेतन के सम्बन्ध की समस्या एकान्त दृष्टिवालों के समक्ष है। जैन दर्शन अनेकान्त माध्यम से इस समस्या को समाहित कर लेता है ।
187
सम्बन्ध का स्वरूप
जैन परम्परा द्रव्य कर्म को पौद्गलिक मानती है। पुद्गल की आठ वर्गणाओं में एक वर्गणा है - कार्मण । उसी के परमाणु- पुद्गल कर्म रूप में आत्मा से सम्बंधित होते हैं । भगवती में अण्णमण्णबद्धा, अण्णमण्णपुट्ठा' आदि कहकर उनका अन्योन्यानुप्रवेश प्रकट किया है।
1
1. सन्मतितर्कप्रकरण 1/47-48
अण्णोणाणुगाणं इमं व तं व त्ति विभयणमजुत्तं । जह दुद्ध- पाणियाणं जावंत विसेसपज्जाया ॥ रूआइ पज्जवा जे देहे जीवदवियम्मि सुद्धम्मि | ते अण्णोणाणुगया पण्णवणिज्जा भवत्थम्मि ॥
2. (क) अंगसुताणि 2, (भगवई) 25/17 जीवदव्वाणं अजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छेति । नो अजीवदव्वाणं जीवदव्वा
परिभोगताए हव्वमागच्छंति ।
Jain Education International
(ख) भगवतोवृत्ति, पत्र, 856 इह जीवद्रव्याणि परिभोजकानि सचेतनत्वेन ग्राहकत्वाद् इतराणि तु परिभोग्यान्यचेतनतया ग्राह्यत्वात् ॥
3. अंगसुत्ताणि 2, ( भगवई), 1 / 312
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org