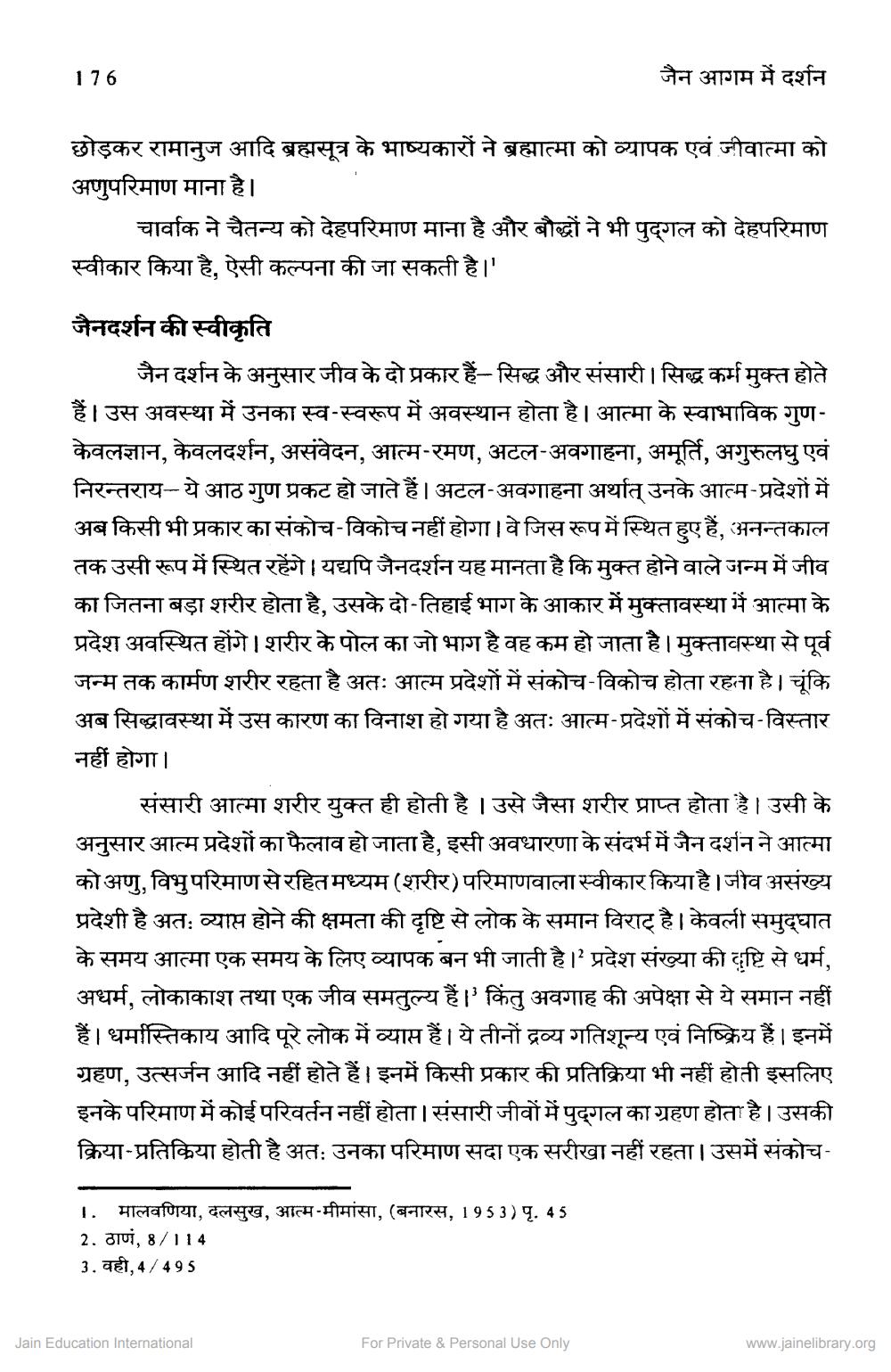________________
176
छोड़कर रामानुज आदि ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों ने ब्रह्मात्मा को व्यापक एवं जीवात्मा को
परिमाण माना है ।
चार्वाक ने चैतन्य को देहपरिमाण माना है और बौद्धों ने भी पुद्गल को देहपरिमाण स्वीकार किया है, ऐसी कल्पना की जा सकती है।'
जैन आगम में दर्शन
जैनदर्शन की स्वीकृति
-
जैन दर्शन के अनुसार जीव के दो प्रकार हैं- सिद्ध और संसारी । सिद्ध कर्म मुक्त होते हैं। उस अवस्था में उनका स्व-स्वरूप में अवस्थान होता है । आत्मा के स्वाभाविक गुणकेवलज्ञान, केवलदर्शन, असंवेदन, आत्म- रमण, अटल- अवगाहना, अमूर्ति, अगुरुलघु एवं निरन्तराय- ये आठ गुण प्रकट हो जाते हैं। अटल- अवगाहना अर्थात् उनके आत्म-प्रदेशों में अब किसी भी प्रकार का संकोच - विकोच नहीं होगा। वे जिस रूप में स्थित हुए हैं, अनन्तकाल तक उसी रूप में स्थित रहेंगे। यद्यपि जैनदर्शन यह मानता है कि मुक्त होने वाले जन्म में जीव का जितना बड़ा शरीर होता है, उसके दो-तिहाई भाग के आकार में मुक्तावस्था में आत्मा के प्रदेश अवस्थित होंगे। शरीर के पोल का जो भाग है वह कम हो जाता है। मुक्तावस्था से पूर्व जन्म तक कार्मण शरीर रहता है अतः आत्म प्रदेशों में संकोच - विकोच होता रहता है। चूंकि अब सिद्धावस्था में उस कारण का विनाश हो गया है अतः आत्म-प्रदेशों में संकोच - विस्तार नहीं होगा ।
संसारी आत्मा शरीर युक्त ही होती है । उसे जैसा शरीर प्राप्त होता है । उसी के अनुसार आत्म प्रदेशों का फैलाव हो जाता है, इसी अवधारणा के संदर्भ में जैन दर्शन ने आत्मा को अणु, विभु परिमाण से रहित मध्यम (शरीर) परिमाणवाला स्वीकार किया है। जीव असंख्य प्रदेशी है अत: व्यास होने की क्षमता की दृष्टि से लोक के समान विराट् है । केवली समुद्घात के समय आत्मा एक समय के लिए व्यापक बन भी जाती है ।' प्रदेश संख्या की दृष्टि से धर्म, अधर्म, लोकाकाश तथा एक जीव समतुल्य हैं।' किंतु अवगाह की अपेक्षा से ये समान नहीं हैं। धर्मास्तिकाय आदि पूरे लोक में व्यास हैं । ये तीनों द्रव्य गतिशून्य एवं निष्क्रिय हैं। इनमें ग्रहण, उत्सर्जन आदि नहीं होते हैं। इनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं होती इसलिए इनके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता । संसारी जीवों में पुद्गल का ग्रहण होता है । उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया होती है अत: उनका परिमाण सदा एक सरीखा नहीं रहता । उसमें संकोच
1.
मालवणिया, दलसुख, आत्म-मीमांसा, (बनारस, 1953) पृ. 45
2. ठाणं, 8/114
3. वही, 4/495
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org