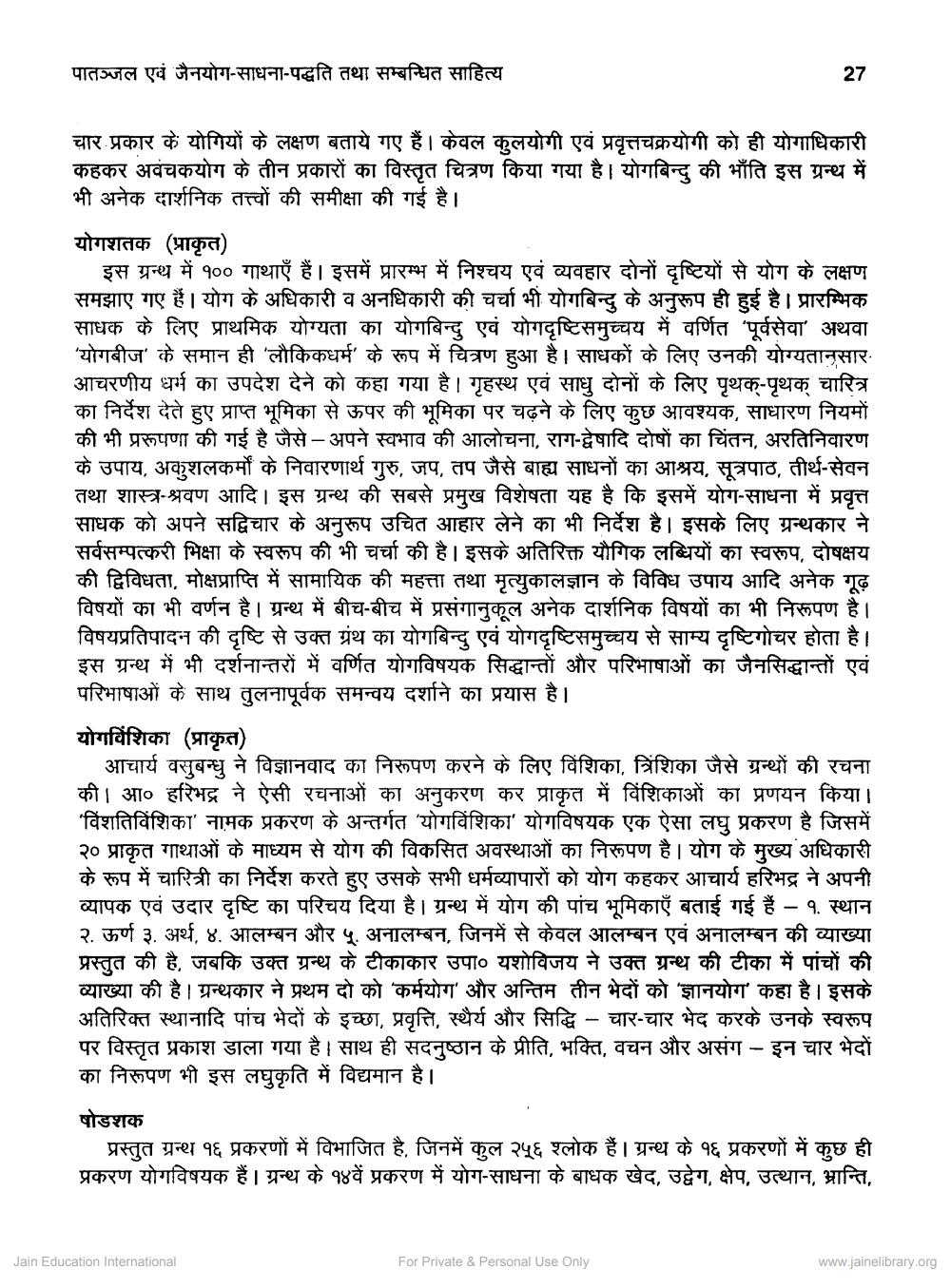________________
पातञ्जल एवं जैनयोग-साधना-पद्धति तथा सम्बन्धित साहित्य
27
चार प्रकार के योगियों के लक्षण बताये गए हैं। केवल कुलयोगी एवं प्रवृत्तचक्रयोगी को ही योगाधिकारी कहकर अवंचकयोग के तीन प्रकारों का विस्तृत चित्रण किया गया है। योगबिन्दु की भाँति इस ग्रन्थ में भी अनेक दार्शनिक तत्त्वों की समीक्षा की गई है।
योगशतक (प्राकृत) - इस ग्रन्थ में १०० गाथाएँ हैं। इसमें प्रारम्भ में निश्चय एवं व्यवहार दोनों दृष्टियों से योग के लक्षण समझाए गए हैं। योग के अधिकारी व अनधिकारी की चर्चा भी योगबिन्दु के अनुरूप ही हुई है। प्रारम्भिक
के लिए प्राथमिक योग्यता का योगबिन्दु एवं योगदृष्टिसमुच्चय में वर्णित "पूर्वसेवा' अथवा 'योगबीज' के समान ही 'लौकिकधर्म' के रूप में चित्रण हुआ है। साधकों के लिए उनकी योग्यतानुसार आचरणीय धर्म का उपदेश देने को कहा गया है। गृहस्थ एवं साधु दोनों के लिए पृथक्-पृथक् चारित्र का निर्देश देते हुए प्राप्त भूमिका से ऊपर की भूमिका पर चढ़ने के लिए कुछ आवश्यक, साधारण नियमों की भी प्ररूपणा की गई है जैसे-अपने स्वभाव की आलोचना, राग-द्वेषादि दोषों का चिंतन, अरतिनिवारण के उपाय, अकुशलकर्मों के निवारणार्थ गुरु, जप, तप जैसे बाह्य साधनों का आश्रय, सूत्रपाठ, तीर्थ-सेवन तथा शास्त्र-श्रवण आदि। इस ग्रन्थ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें योग-साधना में प्रवृत्त साधक को अपने सद्विचार के अनुरूप उचित आहार लेने का भी निर्देश है। इसके लिए ग्रन्थकार ने सर्वसम्पत्करी भिक्षा के स्वरूप की भी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त यौगिक लब्धियों का स्वरूप, दोषक्षय की द्विविधता, मोक्षप्राप्ति में सामायिक की महत्ता तथा मृत्युकालज्ञान के विविध उपाय आदि अनेक गूढ़ विषयों का भी वर्णन है। ग्रन्थ में बीच-बीच में प्रसंगानुकूल अनेक दार्शनिक विषयों का भी निरूपण है। विषयप्रतिपादन की दृष्टि से उक्त ग्रंथ का योगबिन्दु एवं योगदृष्टिसमुच्चय से साम्य दृष्टिगोचर होता है। इस ग्रन्थ में भी दर्शनान्तरों में वर्णित योगविषयक सिद्धान्तों और परिभाषाओं का जैनसिद्धान्तों एवं परिभाषाओं के साथ तुलनापूर्वक समन्वय दर्शाने का प्रयास है। योगविंशिका (प्राकृत)
आचार्य वसुबन्धु ने विज्ञानवाद का निरूपण करने के लिए विंशिका, त्रिंशिका जैसे ग्रन्थों की रचना की। आ० हरिभद्र ने ऐसी रचनाओं का अनुकरण कर प्राकृत में विंशिकाओं का प्रणयन किया। 'विंशतिविशिका' नामक प्रकरण के अन्तर्गत 'योगविंशिका' योगविषयक एक ऐसा लघु प्रकरण है जिसमें २० प्राकृत गाथाओं के माध्यम से योग की विकसित अवस्थाओं का निरूपण है। योग के मुख्य अधिकारी के रूप में चारित्री का निर्देश करते हुए उसके सभी धर्मव्यापारों को योग कहकर आचार्य हरिभद्र ने अपनी व्यापक एवं उदार दृष्टि का परिचय दिया है। ग्रन्थ में योग की पांच भूमिकाएँ बताई गई हैं - १. स्थान २. ऊर्ण ३. अर्थ, ४. आलम्बन और ५. अनालम्बन, जिनमें से केवल आलम्बन एवं अनालम्बन की व्याख्या प्रस्तुत की है, जबकि उक्त ग्रन्थ के टीकाकार उपा० यशोविजय ने उक्त ग्रन्थ की टीका में पांचों की व्याख्या की है। ग्रन्थकार ने प्रथम दो को 'कर्मयोग' और अन्तिम तीन भेदों को 'ज्ञानयोग' कहा है। इसके अतिरिक्त स्थानादि पांच भेदों के इच्छा, प्रवृत्ति, स्थैर्य और सिद्धि - चार-चार भेद करके उनके स्वरूप पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। साथ ही सदनुष्ठान के प्रीति, भक्ति, वचन और असंग - इन चार भेदों का निरूपण भी इस लघकति में विद्यमान है।
षोडशक
प्रस्तुत ग्रन्थ १६ प्रकरणों में विभाजित है, जिनमें कुल २५६ श्लोक हैं। ग्रन्थ के १६ प्रकरणों में कुछ ही प्रकरण योगविषयक हैं। ग्रन्थ के १४वें प्रकरण में योग-साधना के बाधक खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, भ्रान्ति,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org