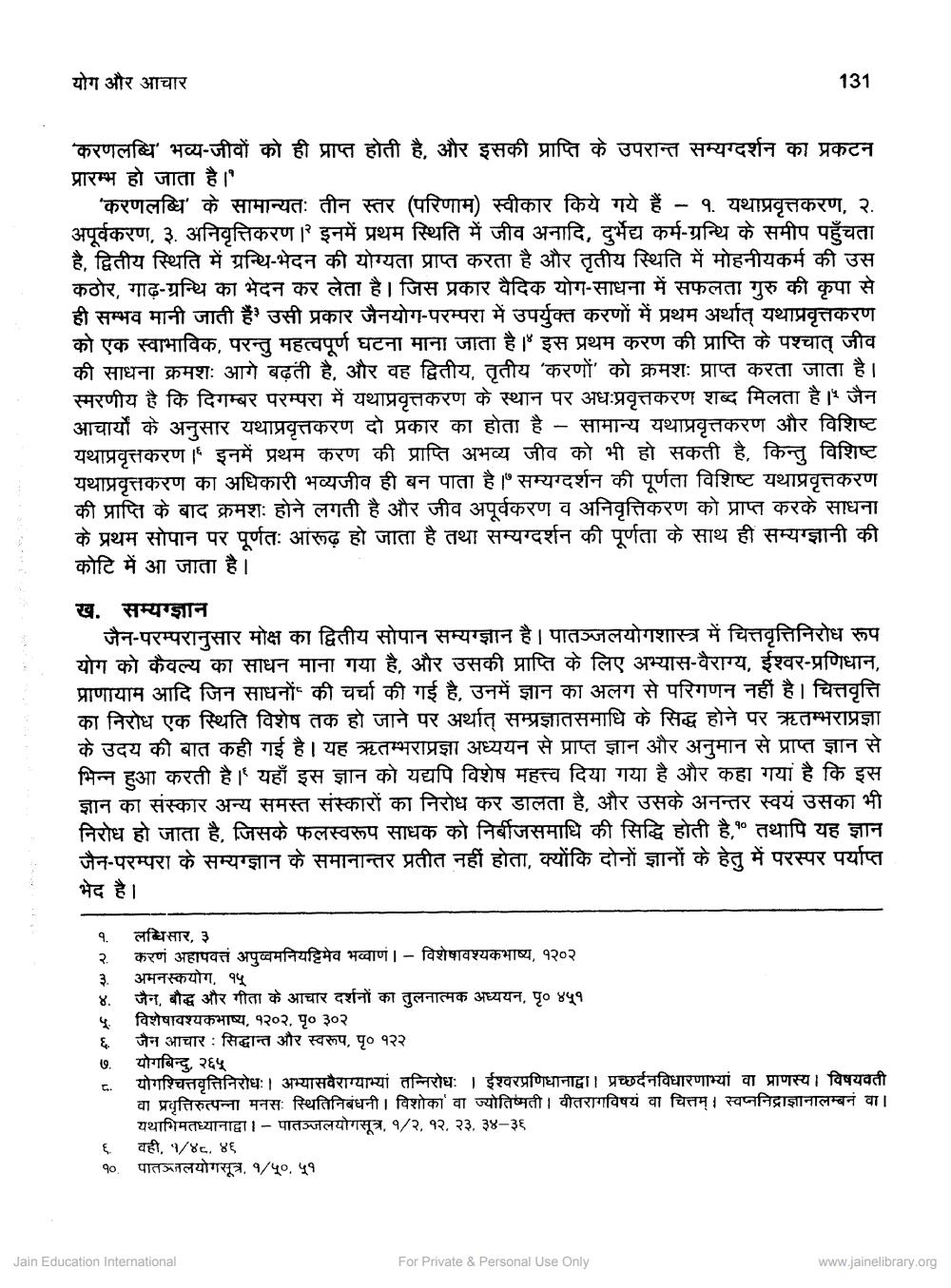________________
योग और आचार
131
'करणलब्धि' भव्य-जीवों को ही प्राप्त होती है, और इसकी प्राप्ति के उपरान्त सम्यग्दर्शन का प्रकटन प्रारम्भ हो जाता है।'
'करणलब्धि' के सामान्यतः तीन स्तर (परिणाम) स्वीकार किये गये हैं - १. यथाप्रवृत्तकरण, २. अपूर्वकरण, ३. अनिवृत्तिकरण। इनमें प्रथम स्थिति में जीव अनादि, दुर्भेद्य कर्म-ग्रन्थि के समीप पहुँचता है, द्वितीय स्थिति में ग्रन्थि-भेदन की योग्यता प्राप्त करता है और तृतीय स्थिति में मोहनीयकर्म की उस कठोर, गाढ़-ग्रन्थि का भेदन कर लेता है। जिस प्रकार वैदिक योग-साधना में सफलता गुरु की कृपा से ही सम्भव मानी जाती हैं उसी प्रकार जैनयोग-परम्परा में उपर्युक्त करणों में प्रथम अर्थात् यथाप्रवृत्तकरण को एक स्वाभाविक, परन्तु महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इस प्रथम करण की प्राप्ति के पश्चात् जीव की साधना क्रमशः आगे बढ़ती है, और वह द्वितीय, तृतीय 'करणों को क्रमशः प्राप्त करता जाता है। स्मरणीय है कि दिगम्बर परम्परा में यथाप्रवृत्तकरण के स्थान पर अधःप्रवृत्तकरण शब्द मिलता है। जैन आचार्यों के अनुसार यथाप्रवृत्तकरण दो प्रकार का होता है - सामान्य यथाप्रवृत्तकरण और विशिष्ट यथाप्रवृत्तकरण । इनमें प्रथम करण की प्राप्ति अभव्य जीव को भी हो सकती है, किन्तु विशिष्ट यथाप्रवृत्तकरण का अधिकारी भव्यजीव ही बन पाता है। सम्यग्दर्शन की पूर्णता विशिष्ट यथाप्रवृत्तकरण की प्राप्ति के बाद क्रमशः होने लगती है और जीव अपूर्वकरण व करण को प्राप्त करके साधना के प्रथम सोपान पर पूर्णतः आरूढ़ हो जाता है तथा सम्यग्दर्शन की पूर्णता के साथ ही सम्यग्ज्ञानी की कोटि में आ जाता है।
ख. सम्यग्ज्ञान
जैन-परम्परानुसार मोक्ष का द्वितीय सोपान सम्यग्ज्ञान है। पातञ्जलयोगशास्त्र में चित्तवृत्तिनिरोध रूप योग को कैवल्य का साधन माना गया है, और उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास-वैराग्य, ईश्वर-प्रणिधान, प्राणायाम आदि जिन साधनों की चर्चा की गई है, उनमें ज्ञान का अलग से परिगणन नहीं है। चित्तवृत्ति का निरोध एक स्थिति विशेष तक हो जाने पर अर्थात सम्प्रज्ञातसमाधि के सिद्ध होने पर ऋतम्भराप्रज्ञा के उदय की बात कही गई है। यह ऋतम्भराप्रज्ञा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान और अनुमान से प्राप्त ज्ञान से भिन्न हुआ करती है। यहाँ इस ज्ञान को यद्यपि विशेष महत्त्व दिया गया है और कहा गया है कि इस ज्ञान का संस्कार अन्य समस्त संस्कारों का निरोध कर डालता है, और उसके अनन्तर स्वयं उसका भी निरोध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप साधक को निर्बीजसमाधि की सिद्धि होती है, तथापि यह ज्ञान जैन-परम्परा के सम्यग्ज्ञान के समानान्तर प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दोनों ज्ञानों के हेतु में परस्पर पर्याप्त भेद है।
mous
१. लब्धिसार, ३ २. करणं अहापवत्तं अपुव्वमनियट्टिमेव भव्वाणं। - विशेषावश्यकभाष्य, १२०२
अमनस्कयोग, १५ जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन, पृ०४५१
विशेषावश्यकभाष्य, १२०२, पृ० ३०२ ६ जैन आचार: सिद्धान्त और स्वरूप, पृ० १२२
योगबिन्दु, २६५ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । ईश्वरप्रणिधानाद्वा। प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबंधनी। विशोका वा ज्योतिष्मती। वीतरागविषयं वा चित्तम् । स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा। यथाभिमतध्यानाद्वा। - पातञ्जलयोगसूत्र, १/२, १२, २३, ३४-३६
वही, १/४८, ४६ १०. पातञ्जलयोगसूत्र. १/५०. ५१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org