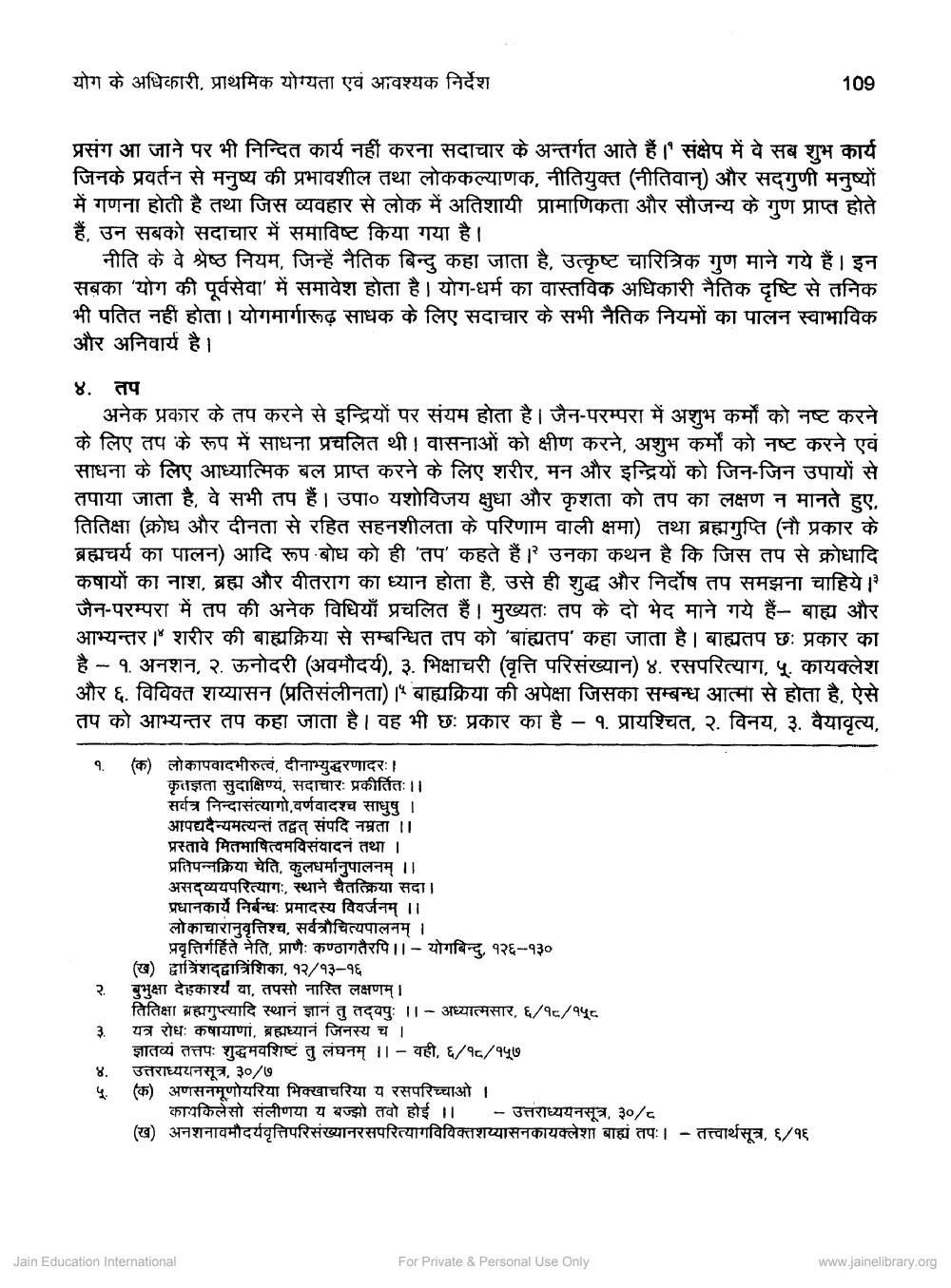________________
योग के अधिकारी, प्राथमिक योग्यता एवं आवश्यक निर्देश
109
प्रसंग आ जाने पर भी निन्दित कार्य नहीं करना सदाचार के अन्तर्गत आते हैं। संक्षेप में वे सब शुभ कार्य जिनके प्रवर्तन से मनुष्य की प्रभावशील तथा लोककल्याणक, नीतियुक्त (नीतिवान्) और सद्गुणी मनुष्यों में गणना होती है तथा जिस व्यवहार से लोक में अतिशायी प्रामाणिकता और सौजन्य के गुण प्राप्त होते हैं, उन सबको सदाचार में समाविष्ट किया गया है।
नीति के वे श्रेष्ठ नियम, जिन्हें नैतिक बिन्दु कहा जाता है, उत्कृष्ट चारित्रिक गुण माने गये हैं। इन सबका 'योग की पूर्वसेवा' में समावेश होता है। योग-धर्म का वास्तविक अधिकारी नैतिक दृष्टि से तनिक भी पतित नहीं होता। योगमार्गारूढ़ साधक के लिए सदाचार के सभी नैतिक नियमों का पालन स्वाभाविक और अनिवार्य है।
४. तप
अनेक प्रकार के तप करने से इन्द्रियों पर संयम होता है। जैन-परम्परा में अशुभ कर्मों को नष्ट करने के लिए तप के रूप में साधना प्रचलित थी। वासनाओं को क्षीण करने, अशुभ कर्मों को नष्ट करने एवं साधना के लिए आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और इन्द्रियों को जिन-जिन उपायों से तपाया जाता है, वे सभी तप हैं। उपा० यशोविजय क्षुधा और कृशता को तप का लक्षण न मानते हुए, तितिक्षा (क्रोध और दीनता से रहित सहनशीलता के परिणाम वाली क्षमा) तथा ब्रह्मगुप्ति (नौ प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन) आदि रूप बोध को ही 'तप' कहते हैं। उनका कथन है कि जिस तप से क्रोधादि कषायों का नाश, ब्रह्म और वीतराग का ध्यान होता है, उसे ही शुद्ध और निर्दोष तप समझना चाहिये। जैन-परम्परा में तप की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। मुख्यतः तप के दो भेद माने गये हैं- बाह्य और आभ्यन्तर । शरीर की बाह्यक्रिया से सम्बन्धित तप को 'बाह्यतप' कहा जाता है। बाह्यतप छः प्रकार का है- १. अनशन, २. ऊनोदरी (अवमौदय), ३. भिक्षाचरी (वृत्ति परिसंख्यान) ४. रसपरित्याग, ५. कायक्लेश
क्त शय्यासन (प्रतिसलीनता)। बाह्यक्रिया की अपेक्षा जिसका सम्बन्ध आत्मा से होता है, ऐसे तप को आभ्यन्तर तप कहा जाता है। वह भी छः प्रकार का है - १. प्रायश्चित, २. विनय, ३. वैयावृत्य,
लोकापवादभीरुत्वं, दीनाभ्युद्धरणादरः । कृतज्ञता सुदाक्षिण्यं, सदाचारः प्रकीर्तितः।। सर्वत्र निन्दासंत्यागो.वर्णवादश्च साधुषु । आपद्यदैन्यमत्यन्तं तद्वत संपदि नम्रता ।। प्रस्तावे मितभाषित्वमविसंवादनं तथा । प्रतिपन्नक्रिया चेति, कुलधर्मानुपालनम् ।। असदव्ययपरित्यागः, स्थाने चैतक्रिया सदा। प्रधानकार्ये निर्बन्धः प्रमादस्य विवर्जनम् ।। लोकाचारानुवृत्तिश्च, सर्वत्रौचित्यपालनम् ।
प्रवृत्तिर्गर्हिते नेति, प्राणैः कण्ठागतैरपि।। - योगबिन्दु, १२६-१३० (ख) द्वात्रिंशद्वात्रिंशिका, १२/१३-१६ बुभुक्षा देहकाश्य वा, तपसो नास्ति लक्षणम्।
तितिक्षा ब्रह्मगुप्त्यादि स्थानं ज्ञानं तु तद्वपुः ।। - अध्यात्मसार, ६/१८/१५८ ३. यत्र रोधः कषायाणा, ब्रह्मध्यानं जिनस्य च ।
ज्ञातव्यं तत्तपः शुद्धमवशिष्टं तु लंघनम् ।। - वही, ६/१८/१५७ उत्तराध्ययनसूत्र, ३०/७ (क) अणसनमूणोयरिया भिक्खाचरिया य रसपरिच्चाओ ।
कायकिलेसो संलीणया य बज्झो तवो होई ।। - उत्तराध्ययनसूत्र, ३०/८ (ख) अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपः। - तत्त्वार्थसूत्र, ६/१६
om ॐ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org