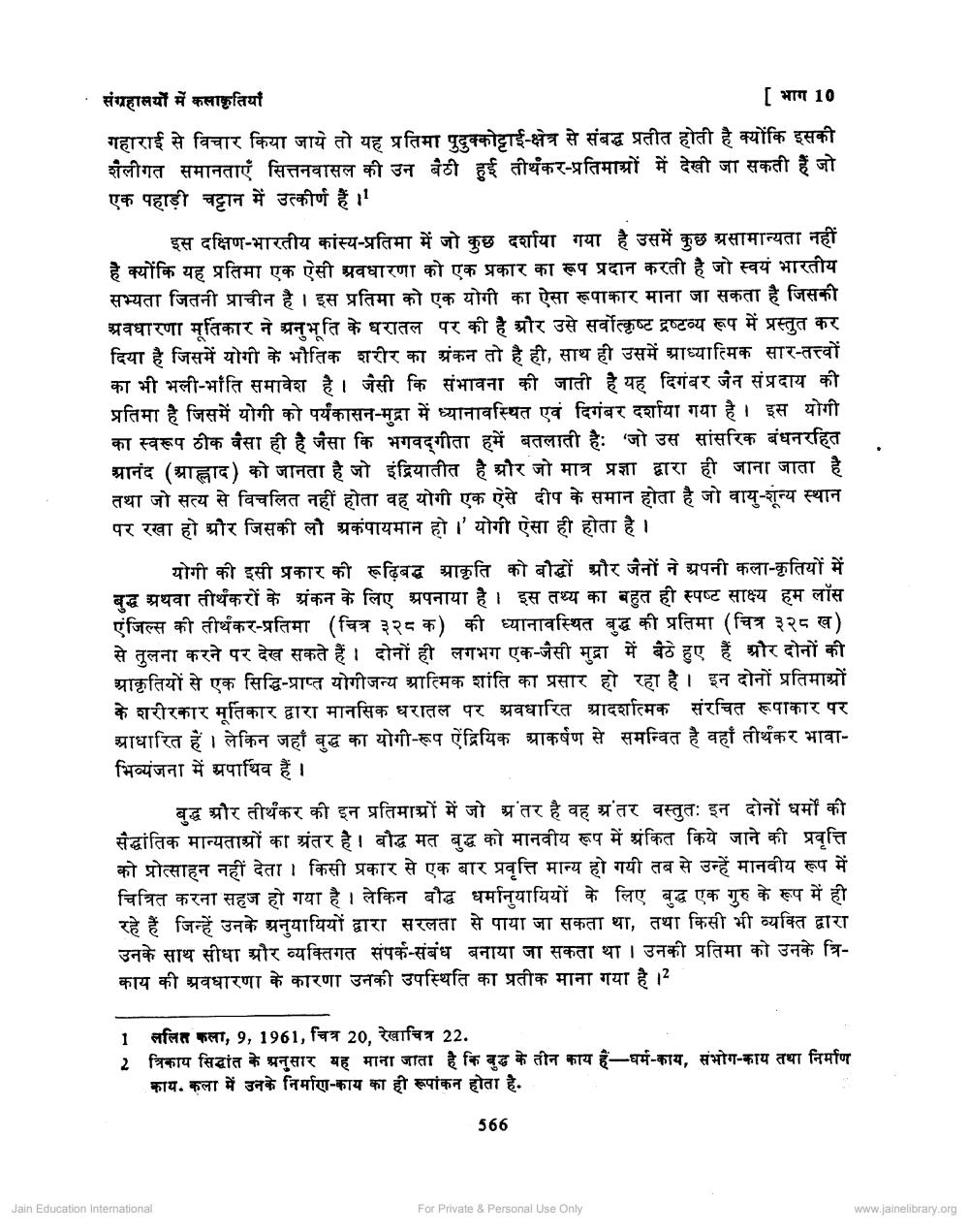________________
- संग्रहालयों में कलाकृतियाँ
[ भाग 10
गहाराई से विचार किया जाये तो यह प्रतिमा पुदुक्कोट्टाई-क्षेत्र से संबद्ध प्रतीत होती है क्योंकि इसकी शैलीगत समानताएं सित्तनवासल की उन बैठी हुई तीर्थंकर-प्रतिमाओं में देखी जा सकती हैं जो एक पहाड़ी चट्टान में उत्कीर्ण हैं।।
___इस दक्षिण-भारतीय कांस्य-प्रतिमा में जो कुछ दर्शाया गया है उसमें कुछ असामान्यता नहीं है क्योंकि यह प्रतिमा एक ऐसी अवधारणा को एक प्रकार का रूप प्रदान करती है जो स्वयं भारतीय सभ्यता जितनी प्राचीन है। इस प्रतिमा को एक योगी का ऐसा रूपाकार माना जा सकता है जिसकी अवधारणा मूर्तिकार ने अनुभूति के धरातल पर की है और उसे सर्वोत्कृष्ट द्रष्टव्य रूप में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें योगी के भौतिक शरीर का अंकन तो है ही, साथ ही उसमें आध्यात्मिक सार-तत्त्वों का भी भली-भांति समावेश है। जैसी कि संभावना की जाती है यह दिगंबर जैन संप्रदाय की प्रतिमा है जिसमें योगी को पर्यकासन-मुद्रा में ध्यानावस्थित एवं दिगंबर दर्शाया गया है। इस योगी का स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा कि भगवद्गीता हमें बतलाती है: 'जो उस सांसरिक बंधनरहित आनंद (आह्लाद) को जानता है जो इंद्रियातीत है और जो मात्र प्रज्ञा द्वारा ही जाना जाता है तथा जो सत्य से विचलित नहीं होता वह योगी एक ऐसे दीप के समान होता है जो वायु-शून्य स्थान पर रखा हो और जिसकी लौ अकंपायमान हो।' योगी ऐसा ही होता है।
___ योगी की इसी प्रकार की रूढिबद्ध आकृति को बौद्धों और जैनों ने अपनी कला-कृतियों में बुद्ध अथवा तीर्थंकरों के अंकन के लिए अपनाया है। इस तथ्य का बहुत ही स्पष्ट साक्ष्य हम लॉस एंजिल्स की तीर्थंकर-प्रतिमा (चित्र ३२८ क) की ध्यानावस्थित बुद्ध की प्रतिमा (चित्र ३२८ ख) से तुलना करने पर देख सकते हैं। दोनों ही लगभग एक-जैसी मुद्रा में बैठे हुए हैं और दोनों की प्राकृतियों से एक सिद्धि-प्राप्त योगीजन्य आत्मिक शांति का प्रसार हो रहा है। इन दोनों प्रतिमाओं के शरीरकार मूर्तिकार द्वारा मानसिक धरातल पर अवधारित आदर्शात्मक संरचित रूपाकार पर आधारित हैं। लेकिन जहाँ बद्ध का योगी-रूप ऐंद्रियिक आकर्षण से समन्वित है वहाँ तीर्थकर भावाभिव्यंजना में अपार्थिव हैं।
बुद्ध और तीर्थंकर की इन प्रतिमानों में जो अतर है वह अंतर वस्तुत: इन दोनों धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं का अंतर है। बौद्ध मत बुद्ध को मानवीय रूप में अंकित किये जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देता। किसी प्रकार से एक बार प्रवृत्ति मान्य हो गयी तब से उन्हें मानवीय रूप में चित्रित करना सहज हो गया है। लेकिन बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए बुद्ध एक गुरु के रूप में ही रहे हैं जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा सरलता से पाया जा सकता था, तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके साथ सीधा और व्यक्तिगत संपर्क-संबंध बनाया जा सकता था। उनकी प्रतिमा को उनके त्रिकाय की अवधारणा के कारणा उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना गया है।
1 ललित कला, 9, 1961, चित्र 20, रेखाचित्र 22. 2 त्रिकाय सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि बुद्ध के तीन काय है-धर्म-काय, संभोग-काय तथा निर्माण
काय. कला में उनके निर्माण-काय का ही रूपांकन होता है.
566
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org