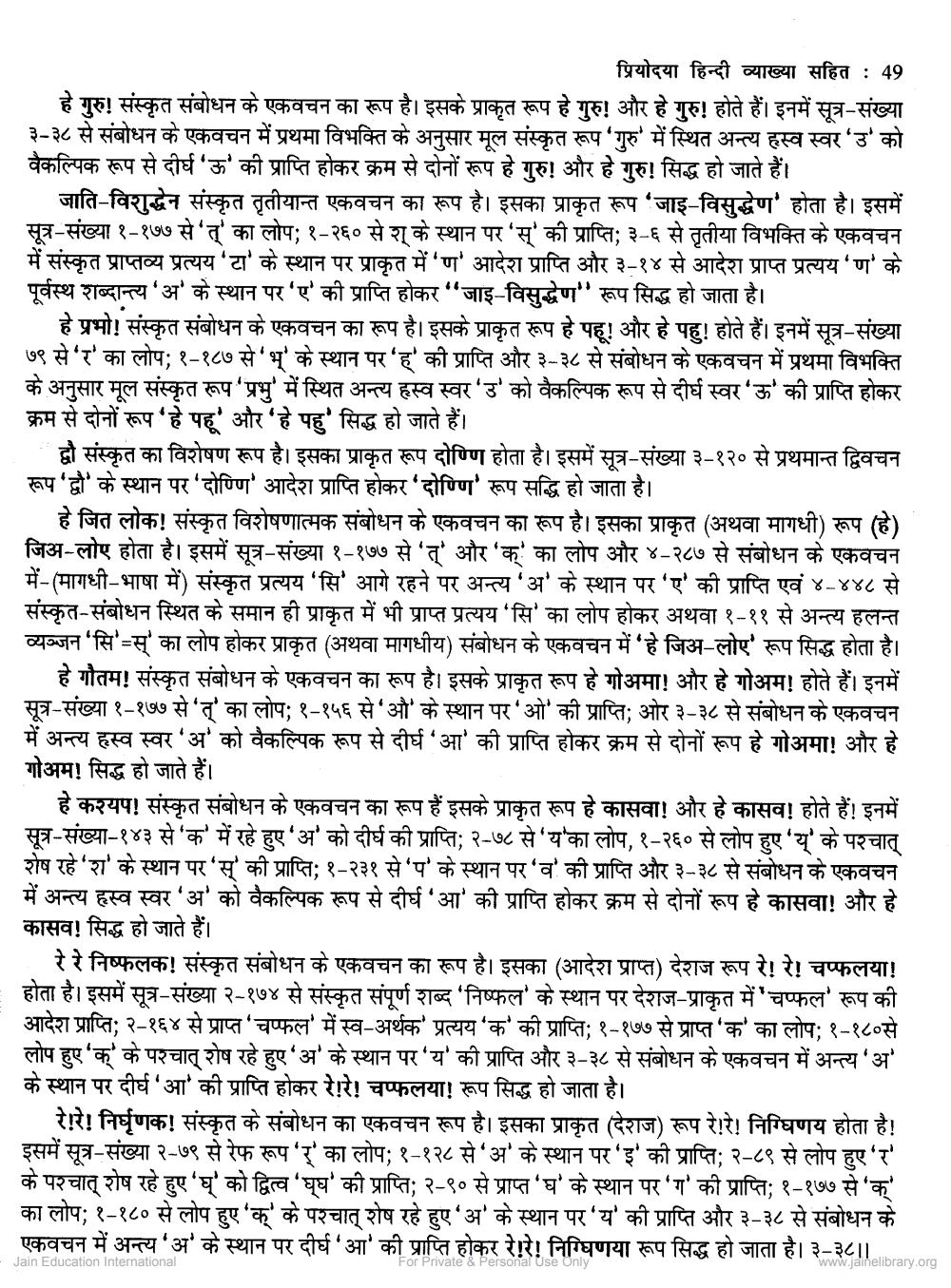________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 49
गुरु! संस्कृत संबोधन के एकवचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप हे गुरु! और हे गुरु! होते हैं। इनमें सूत्र - संख्या ३ - ३८ से संबोधन के एकवचन में प्रथमा विभक्ति के अनुसार मूल संस्कृत रूप 'गुरु' में स्थित अन्त्य ह्रस्व स्वर 'उ' को वैकल्पिक रूप से दीर्घ 'ऊ' की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप हे गुरु! और हे गुरु! सिद्ध हो जाते हैं।
जाति- विशुद्धेन संस्कृत तृतीयान्त एकवचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'जाइ - विसुद्धेण' होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १७७ से 'त्' का लोप; १ - २६० से श् के स्थान पर 'स्' की प्राप्ति; ३ - ६ से तृतीया विभक्ति के एकवचन में संस्कृत प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' आदेश प्राप्ति और ३-१४ से आदेश प्राप्त प्रत्यय 'ण' के पूर्वस्थ शब्दान्त्य 'अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति होकर "जाइ-विसुद्वेण " रूप सिद्ध हो जाता है।
प्रभो! संस्कृत संबोधन के एकवचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप हे पहू! और हे पहु! होते हैं। इनमें सूत्र - संख्या ७९ से 'र' का लोप; १ - १८७ से 'भू' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति और ३-३८ से संबोधन के एकवचन में प्रथमा विभक्ति के अनुसार मूल संस्कृत रूप 'प्रभु' में स्थित अन्त्य ह्रस्व स्वर 'उ' को वैकल्पिक रूप से दीर्घ स्वर 'ऊ' की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप 'हे पहू' और 'हे पहु' सिद्ध हो जाते हैं।
प्रथमान्त द्विवचन
हे जित लोक! संस्कृत विशेषणात्मक संबोधन के एकवचन का रूप है। इसका प्राकृत (अथवा मागधी) रूप (हे ) जिअ - लोए होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १७७ से 'त्' और 'क्' का लोप और ४ - २८७ से संबोधन के एकवचन
- (मागधी - भाषा में) संस्कृत प्रत्यय 'सि' आगे रहने पर अन्त्य 'अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति एवं ४-४४८ से संस्कृत- संबोधन स्थित समान ही प्राकृत में भी प्राप्त प्रत्यय 'सि' का लोप होकर अथवा १ - ११ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 'सि'=स्' का लोप होकर प्राकृत (अथवा मागधीय) संबोधन के एकवचन में 'हे जिअ - लोए' रूप सिद्ध होता है।
द्वौ संस्कृत का विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप दोण्णि होता है। इसमें सूत्र - संख्या ३ - १२० रूप 'द्वौ' के स्थान पर 'दोण्णि' आदेश प्राप्ति होकर 'दोण्णि' रूप सद्धि हो जाता है।
हे गौतम! संस्कृत संबोधन के एकवचन का रूप है। इसके प्राकृत रूप हे गोअमा ! और हे गोअम! होते हैं। इनमें सूत्र - संख्या १ - १७७ से 'त्' का लोप; १ - १५६ से 'औ' के स्थान पर 'ओ' की प्राप्ति ओर ३ - ३८ से संबोधन के एकवचन में अन्त्य ह्रस्व स्वर 'अ' को वैकल्पिक रूप से दीर्घ 'आ' की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप हे गोअमा ! और हे गोअम! सिद्ध हो जाते हैं।
कश्यप ! संस्कृत संबोधन के एकवचन का रूप हैं इसके प्राकृत रूप हे कासवा ! और हे कासव ! होते हैं ! इनमें सूत्र - संख्या - १४३ से 'क' में रहे हुए 'अ' को दीर्घ की प्राप्ति; २- ७८ से 'य'का लोप, १ - २६० से लोप हुए 'य्' के पश्चात् शेष रहे 'श' के स्थान पर 'स्' की प्राप्ति; १ - २३१ से 'प' के स्थान पर 'व' की प्राप्ति और ३-३८ से संबोधन के एकवचन में अन्त्य ह्रस्व स्वर 'अ' को वैकल्पिक रूप से दीर्घ 'आ' की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप हे कासवा ! और हे कासव ! सिद्ध हो जाते हैं।
रे रे निष्फलक ! संस्कृत संबोधन के एकवचन का रूप है। इसका (आदेश प्राप्त) देशज रूप रे! रे ! चप्फलया ! होता है। इसमें सूत्र - संख्या २ - १७४ से संस्कृत संपूर्ण शब्द 'निष्फल' के स्थान पर देशज - प्राकृत में ' चप्फल' रूप की आदेश प्राप्ति २ - १६४ से प्राप्त 'चप्फल' में स्व-अर्थक' प्रत्यय 'क' की प्राप्ति; १ - १७७ से प्राप्त 'क' का लोप; १ - १८० से लोप हुए 'क्' के पश्चात् शेष रहे हुए 'अ' के स्थान पर 'य' की प्राप्ति और ३-३८ से संबोधन के एकवचन में अन्त्य 'अ' के स्थान पर दीर्घ 'आ' की प्राप्ति होकर रे! रे ! चप्फलया! रूप सिद्ध हो जाता है।
रे! रे! निर्घृणक ! संस्कृत के संबोधन का एकवचन रूप है। इसका प्राकृत (देशज) रूप रे! रे ! निग्घिणय होता है ! इसमें सूत्र - संख्या २-७९ से रेफ रूप 'र्' का लोप; १ - १२८ से 'अ' के स्थान पर 'इ' की प्राप्ति; २-८९ से लोप हुए 'र' के पश्चात् शेष रहे हुए 'घ्' को द्वित्व 'घ्घ' की प्राप्ति; २ - ९० से प्राप्त 'घ' के स्थान पर 'ग' की प्राप्ति; १ - १७७ से 'क्' का लोप; १ - १८० से लोप हुए 'कू' के पश्चात् शेष रहे हुए 'अ' के स्थान पर 'य' की प्राप्ति और ३-३८ से संबोधन के एकवचन में अन्त्य 'अ' के स्थान पर दीर्घ 'आ' की प्राप्ति होकर रे! रे ! निग्घिणया रूप सिद्ध हो जाता है । ३-३८ ।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jaihelibrary.org