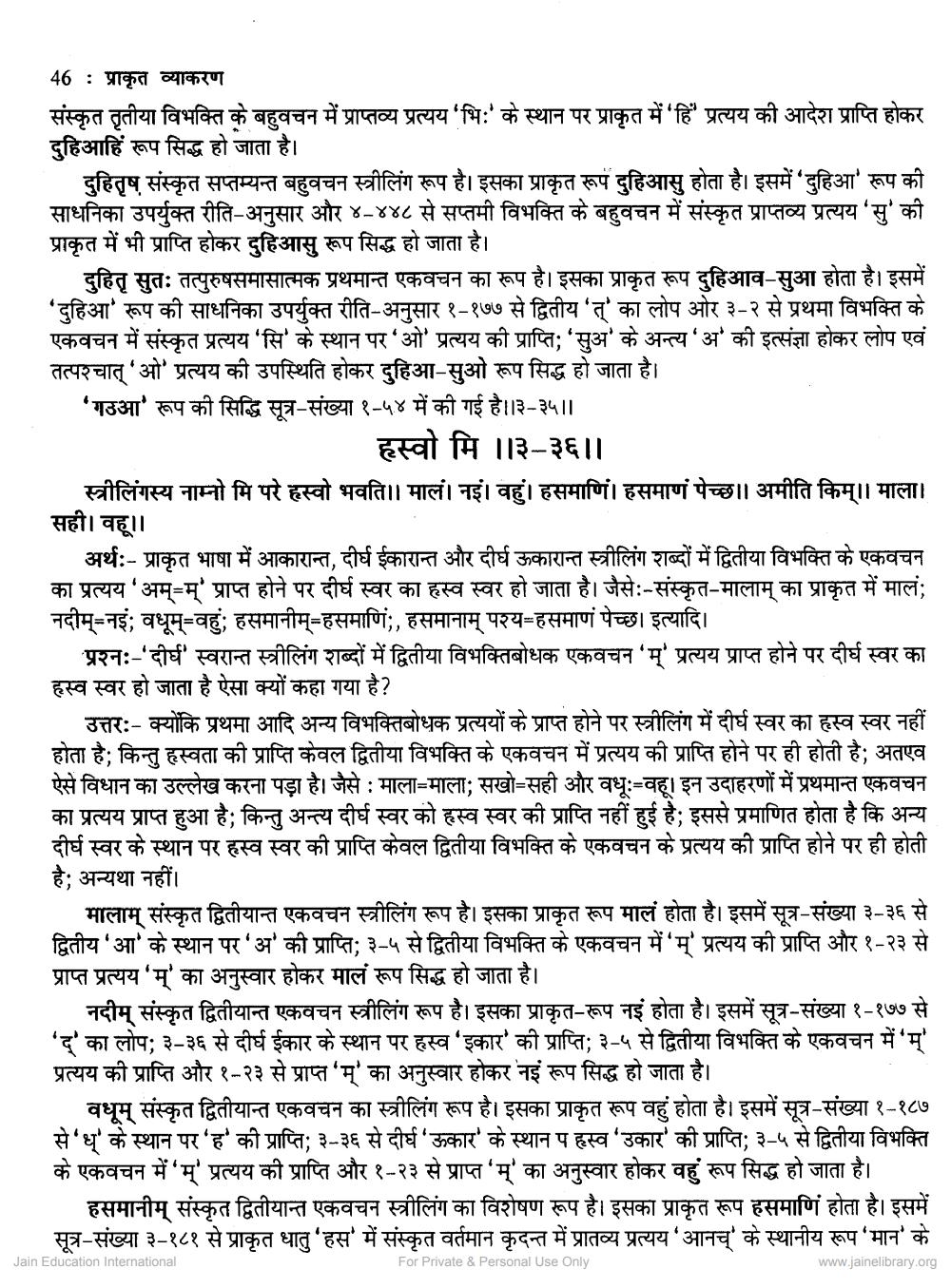________________
46 : प्राकृत व्याकरण
संस्कृत तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'भिः' के स्थान पर प्राकृत में 'हिं' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति होकर दुहिहिं रूप सिद्ध हो जाता है।
दुहितृष संस्कृत सप्तम्यन्त बहुवचन स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप दुहिआसु होता है। इसमें 'दुहिआ' रूप की साधनिका उपर्युक्त रीति- अनुसार और ४-४४८ से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में संस्कृत प्राप्तव्य प्रत्यय 'सु' की प्राकृत में भी प्राप्ति होकर दुहिआसु रूप सिद्ध हो जाता है।
दुहितृ सुतः तत्पुरुषसमासात्मक प्रथमान्त एकवचन का रूप है। इसका प्राकृत रूप दुहिआव-सुआ होता है। इसमें 'दुहिआ' रूप की साधनिका उपर्युक्त रीति अनुसार १ - १७७ से द्वितीय 'त्' का लोप ओर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'सि' के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति; 'सुअ' के अन्त्य 'अ' की इत्संज्ञा होकर लोप एवं तत्पश्चात् 'ओ' प्रत्यय की उपस्थिति होकर दुहिआ-सुओ रूप सिद्ध हो जाता है।
'गउआ' रूप की सिद्धि सूत्र - संख्या १-५४ में की गई है । । ३ - ३५ ।।
ह्रस्वो मि ।।३-३६॥
स्त्रीलिंगस्य नाम्नोमि परे ह्रस्वो भवति ।। मालं । नई। वहुं। हसमाणिं। हसमागं पेच्छ । अमीति किम् ।। माला । सही । वहू ॥
अर्थः- प्राकृत भाषा में आकारान्त, दीर्घ ईकारान्त और दीर्घ ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में द्वितीया विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय ‘अम्=म् ं प्राप्त होने पर दीर्घ स्वर का हस्व स्वर हो जाता है। जैसे:-संस्कृत-मालाम् का प्राकृत में मालं; नदीम्=नइं; वधूम्=वहुं; हसमानीम् - हसमाणि;, हसमानाम् पश्य = हसमाणं पेच्छ । इत्यादि।
'प्रश्नः-'दीर्घ' स्वरान्त स्त्रीलिंग शब्दों में द्वितीया विभक्तिबोधक एकवचन 'म्' प्रत्यय प्राप्त होने पर दीर्घ स्वर का हस्व स्वर हो जाता है ऐसा क्यों कहा गया है?
उत्तर:- क्योंकि प्रथमा आदि अन्य विभक्तिबोधक प्रत्ययों के प्राप्त होने पर स्त्रीलिंग में दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर नहीं होता है; किन्तु ह्रस्वता की प्राप्ति केवल द्वितीया विभक्ति के एकवचन में प्रत्यय की प्राप्ति होने पर ही होती है; अतएव ऐसे विधान का उल्लेख करना पड़ा है। जैसे : माला-माला; सखो - सही और वधूः = वहू । इन उदाहरणों में प्रथमान्त एकवचन का प्रत्यय प्राप्त हुआ है; किन्तु अन्त्य दीर्घ स्वर को हस्व स्वर की प्राप्ति नहीं हुई है; इससे प्रमाणित होता है कि अन्य दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर की प्राप्ति केवल द्वितीया विभक्ति के एकवचन के प्रत्यय की प्राप्ति होने पर ही होती है; अन्यथा नहीं।
माला संस्कृत द्वितीयान्त एकवचन स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप मालं होता है। इसमें सूत्र - संख्या ३ - ३६ से द्वितीय 'आ' के स्थान पर 'अ' की प्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एकवचन में 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म्' का अनुस्वार होकर मालं रूप सिद्ध हो जाता है।
नदीम् संस्कृत द्वितीयान्त एकवचन स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप नई होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १७७ से 'द्' का लोप; ३-३६ से दीर्घ ईकार के स्थान पर ह्रस्व 'इकार' की प्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एकवचन में 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १ - २३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर नई रूप सिद्ध हो जाता है।
धूम् संस्कृत द्वितीयान्त एकवचन का स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप वहुं होता है। इसमें सूत्र - संख्या १ - १८७ से 'धू' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; ३ - ३६ से दीर्घ 'ऊकार' के स्थान प ह्रस्व 'उकार' की प्राप्ति; ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एकवचन में 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १ - २३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर वहुं रूप सिद्ध हो जाता है।
समानीम् संस्कृत द्वितीयान्त एकवचन स्त्रीलिंग का विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप हसमाणिं होता है। इसमें सूत्र - संख्या ३ - १८१ से प्राकृत धातु 'हस' में संस्कृत वर्तमान कृदन्त में प्रातव्य प्रत्यय 'आनच्' के स्थानीय रूप 'मान' के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org