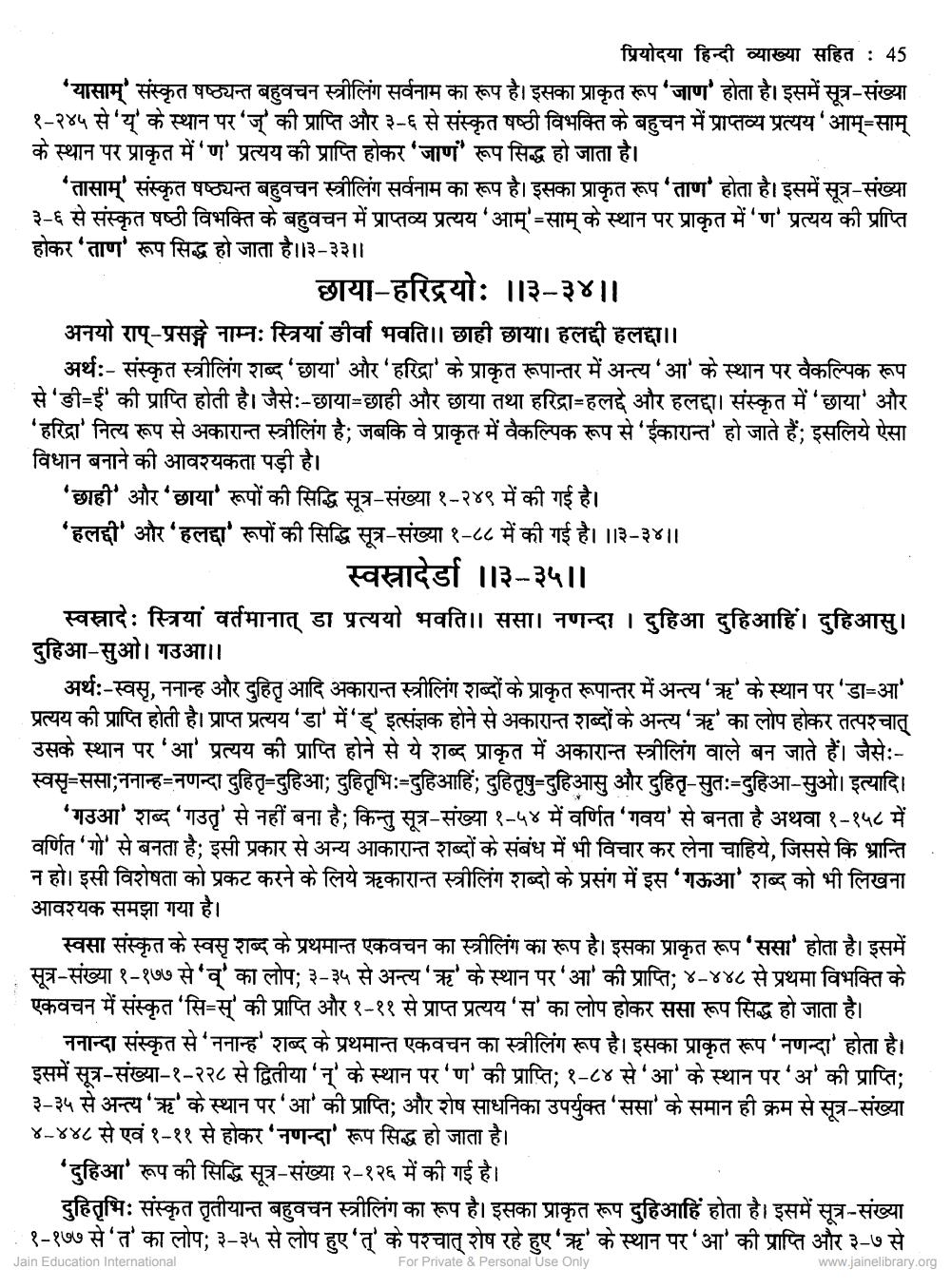________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 45 'यासाम्' संस्कृत षष्ठ्यन्त बहुवचन स्त्रीलिंग सर्वनाम का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'जाण' होता है। इसमें सूत्र - संख्या १-२४५ से 'य्' के स्थान पर 'ज्' की प्राप्ति और ३-६ से संस्कृत षष्ठी विभक्ति के बहुचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'आम्= साम् के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'जाणं' रूप सिद्ध हो जाता है।
'तासाम्' संस्कृत षष्ठ्यन्त बहुवचन स्त्रीलिंग सर्वनाम का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'ताण' होता है। इसमें सूत्र - संख्या ३-६ से संस्कृत षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'आम्' =साम् के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'ताण' रूप सिद्ध हो जाता है ।। ३-३३॥
छाया - हरिद्रयोः ।।३-३४।।
अनयो राप्-प्रसङ्गे नाम्नः स्त्रियां ङीर्वा भवति ।। छाही छाया । हलद्दी हलद्दा ||
अर्थः- संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द 'छाया' और 'हरिद्रा' के प्राकृत रूपान्तर में अन्त्य 'आ' के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'डी =ई' की प्राप्ति होती है। जैसे:- छाया-छाही और छाया तथा हरिद्रा - हलदे और हलद्दा । संस्कृत में 'छाया' और 'हरिद्रा' नित्य रूप से अकारान्त स्त्रीलिंग है; जबकि वे प्राकृत में वैकल्पिक रूप से 'ईकारान्त' हो जाते हैं; इसलिये ऐसा विधान बनाने की आवश्यकता पड़ी है।
'छाही' और 'छाया' रूपों की सिद्धि सूत्र - संख्या १ - २४९ में की गई है।
'हलद्दी' और 'हलद्दा' रूपों की सिद्धि सूत्र - संख्या १-८८ में की गई है। ।। ३-३४।।
स्वस्रादेर्डा ।।३ - ३५।।
स्वस्रादेः स्त्रियां वर्तमानात् डा प्रत्ययो भवति ।। ससा । नणन्दा । दुहिआ दुहिआहिं । दुहिआसु । दुआ-सुओ । गउआ । ।
अर्थः- स्वसृ, ननान्ह और दुहितृ आदि अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के प्राकृत रूपान्तर में अन्त्य 'ऋ' के स्थान पर 'डा=आ' प्रत्यय की प्राप्ति होती है। प्राप्त प्रत्यय 'डा' में 'ड्' इत्संज्ञक होने से अकारान्त शब्दों के अन्त्य 'ऋ' का लोप होकर तत्पश्चात् उसके स्थान पर 'आ' प्रत्यय की प्राप्ति होने से ये शब्द प्राकृत में अकारान्त स्त्रीलिंग वाले बन जाते हैं। जैसे:स्वसृ=ससा;ननान्ह=नणन्दा दुहितृ-दुहिआ; दुहितृभिः = दुहिआहिं; दुहितृषु-दुहिआसु और दुहितृ-सुतः - दुहिआ -सुओ । इत्यादि ।
'गउआ' शब्द 'गउतृ' से नहीं बना है; किन्तु सूत्र - संख्या १-५४ में वर्णित 'गवय' से बनता है अथवा १ - १५८ में वर्णित 'गो' से बनता है; इसी प्रकार से अन्य आकारान्त शब्दों के संबंध में भी विचार कर लेना चाहिये, जिससे कि भ्रान्ति न हो। इसी विशेषता को प्रकट करने के लिये ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दो के प्रसंग में इस 'गऊआ' शब्द को भी लिखना आवश्यक समझा गया है।
स्वसा संस्कृत के स्वसृ शब्द के प्रथमान्त एकवचन का स्त्रीलिंग का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'ससा' होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-१७७ से 'व्' का लोप; ३ - ३५ से अन्त्य 'ऋ' के स्थान पर 'आ' की प्राप्ति; ४-४४८ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में संस्कृत 'सि=स्' की प्राप्ति और १ - ११ से प्राप्त प्रत्यय 'स' का लोप होकर ससा रूप सिद्ध हो जाता है।
ननान्दा संस्कृत से 'ननान्ह' शब्द के प्रथमान्त एकवचन का स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप 'नणन्दा' होता है। इसमें सूत्र- संख्या - १ - २२८ से द्वितीया 'न्' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; १-८४ से 'आ' के स्थान पर 'अ' की प्राप्ति; ३ - ३५ से अन्त्य 'ऋ' के स्थान पर 'आ' की प्राप्ति; और शेष साधनिका उपर्युक्त 'ससा' के समान ही क्रम से सूत्र - संख्या ४ - ४४८ से एवं १ - ११ से होकर 'नणन्दा' रूप सिद्ध हो जाता है।
'दुहिआ' रूप की सिद्धि सूत्र - संख्या २ - १२६ में की गई है।
दुहितृभिः संस्कृत तृतीयान्त बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप है। इसका प्राकृत रूप दुहिआहिं होता है। इसमें सूत्र - संख्या १-१७७ से ‘त' का लोप; ३ - ३५ से लोप हुए 'त्' के पश्चात् शेष रहे हुए 'ऋ' के स्थान पर 'आ' की प्राप्ति और ३-७ से
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org