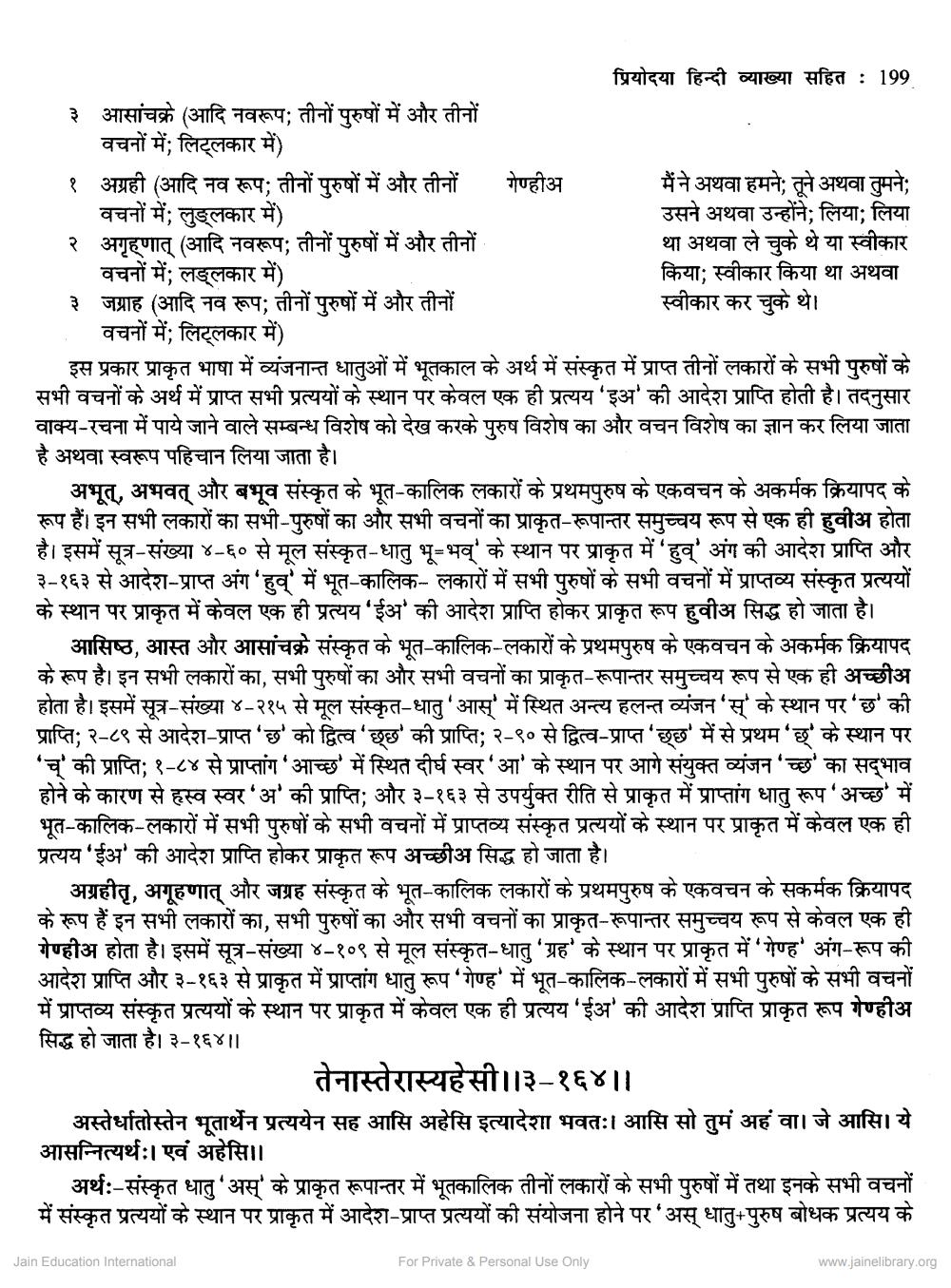________________
३ आसांचक्रे (आदि नवरूप; तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में; लिट्लकार में)
१ अग्रही (आदि नव रूप; तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में; लुङ्लकार में)
२ अगृह्णात् (आदि नवरूप; तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में; लङ्लकार में)
३ जग्राह (आदि नव रूप; तीनों पुरुषों में और तीनों
वचनों में; लिट्लकार में)
गेहीअ
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 199
इस प्रकार प्राकृत भाषा में व्यंजनान्त धातुओं में भूतकाल के अर्थ में संस्कृत में प्राप्त तीनों लकारों के सभी पुरुषों के सभी वचनों के अर्थ में प्राप्त सभी प्रत्ययों के स्थान पर केवल एक ही प्रत्यय 'इअ' की आदेश प्राप्ति होती है। तदनुसार वाक्य-रचना में पाये जाने वाले सम्बन्ध विशेष को देख करके पुरुष विशेष का और वचन विशेष का ज्ञान कर लिया जाता है अथवा स्वरूप पहिचान लिया जाता है।
मैंने अथवा हमने; तूने अथवा तुमने; उसने अथवा उन्होंने; लिया; लिया था अथवा ले चुके थे या स्वीकार किया; स्वीकार किया था अथवा स्वीकार कर चुके थे।
अभूत्, अभवत् और बभूव संस्कृत के भूत-कालिक लकारों के प्रथमपुरुष के एकवचन के अकर्मक क्रियापद के रूप हैं। इन सभी लकारों का सभी-पुरुषों का और सभी वचनों का प्राकृत रूपान्तर समुच्चय रूप से एक ही हुवीअ होता है। इसमें सूत्र - संख्या ४-६० से मूल संस्कृत धातु भू= भव्' के स्थान पर प्राकृत में 'हुव्' अंग की आदेश प्राप्ति और ३-१६३ से आदेश-प्राप्त अंग 'हुव्' में भूत-कालिक - लकारों में सभी पुरुषों के सभी वचनों में प्राप्तव्य संस्कृत प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में केवल एक ही प्रत्यय 'ईअ' की आदेश प्राप्ति होकर प्राकृत रूप हुवीअ सिद्ध हो जाता है।
आसिष्ठ, आस्त और आसांचक्रे संस्कृत के भूत-कालिक-लकारों के प्रथमपुरुष के एकवचन के अकर्मक क्रियापद के रूप है। इन सभी लकारों का, सभी पुरुषों का और सभी वचनों का प्राकृत - रूपान्तर समुच्चय रूप से एक ही अच्छीअ होता है। इसमें सूत्र- संख्या ४- २१५ से मूल संस्कृत - धातु 'आस्' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यंजन 'स्' के स्थान पर 'छ' की प्राप्ति; २-८९ से आदेश प्राप्त 'छ' को द्वित्व 'छ्छ' की प्राप्ति; २-९० से द्वित्व प्राप्त 'छ्छ' में से प्रथम 'छ्' के स्थान पर 'च्' की प्राप्ति; १ - ८४ से प्राप्तांग 'आच्छ' में स्थित दीर्घ स्वर 'आ' के स्थान पर आगे संयुक्त व्यंजन 'च्छ' का सद्भाव होने के कारण से हस्व स्वर 'अ' की प्राप्ति; और ३-१६३ से उपर्युक्त रीति से प्राकृत में प्राप्तांग धातु रूप ' अच्छ' में भूत-कालिक - लकारों में सभी पुरुषों के सभी वचनों में प्राप्तव्य संस्कृत प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में केवल एक ही 'प्रत्यय 'ईअ' की आदेश प्राप्ति होकर प्राकृत रूप अच्छीअ सिद्ध हो जाता है।
ग्रह, अहणात् और जग्रह संस्कृत के भूत-कालिक लकारों के प्रथमपुरुष के एकवचन के सकर्मक क्रियापद के रूप हैं इन सभी कारों का, सभी पुरुषों का और सभी वचनों का प्राकृत रूपान्तर समुच्चय रूप से केवल एक ही गेही होता है। इसमें सूत्र - संख्या ४- १०९ से मूल संस्कृत - धातु 'ग्रह' के स्थान पर प्राकृत में 'गेण्ह' अंग-रूप की आदेश प्राप्ति और ३- १६३ से प्राकृत में प्राप्तांग धातु रूप 'गेण्ह' में भूत-कालिक-लकारों में सभी पुरुषों के सभी वचनों में प्राप्तव्य संस्कृत प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में केवल एक ही प्रत्यय 'ईअ' की आदेश प्राप्ति प्राकृत रूप गेण्हीअ सिद्ध हो जाता है । ३-१६४।।
Jain Education International
तेनास्तेरास्यहेसी ।।३-१६४।।
अस्तेर्धातोस्तेन भूतार्थेन प्रत्ययेन सह आसि अहेसि इत्यादेशा भवतः । आसि सो तुमं अहं वा । आसि। ये आसन्नित्यर्थः । एवं अहेसि ।।
अर्थः-संस्कृत धातु 'अस्' के प्राकृत रूपान्तर में भूतकालिक तीनों लकारों के सभी पुरुषों में तथा इनके सभी वचनों में संस्कृत प्रत्ययों के स्थान पर प्राकृत में आदेश प्राप्त प्रत्ययों की संयोजना होने पर 'अस् धातु+पुरुष बोधक प्रत्यय के
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org