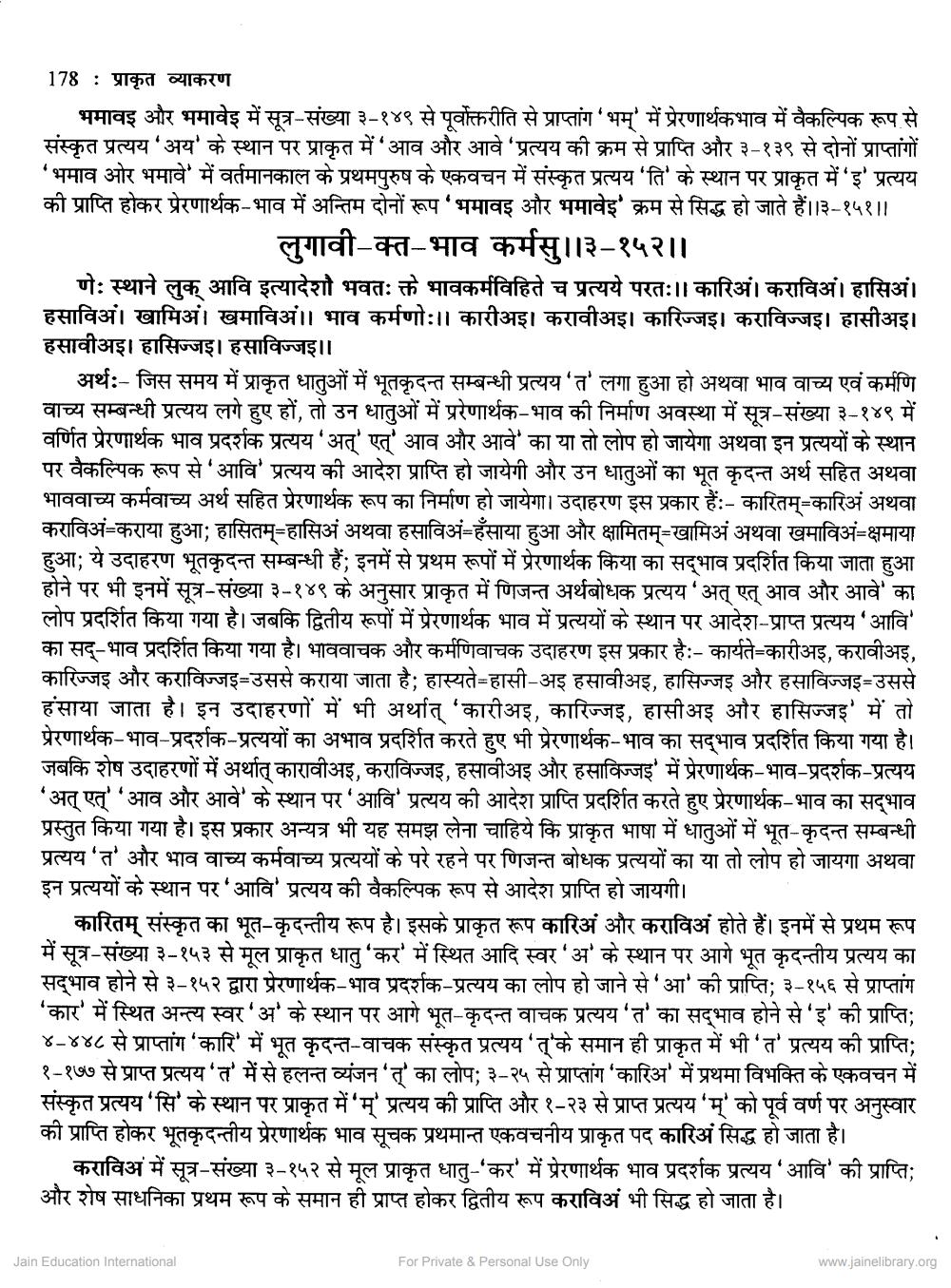________________
178 : प्राकृत व्याकरण ___भमावइ और भमावेइ में सूत्र-संख्या ३-१४९ से पूर्वोक्तरीति से प्राप्तांग 'भम्' में प्रेरणार्थकभाव में वैकल्पिक रूप से संस्कृत प्रत्यय 'अय' के स्थान पर प्राकृत में 'आव और आवे 'प्रत्यय की क्रम से प्राप्ति और ३-१३९ से दोनों प्राप्तांगों 'भमाव ओर भमावे' में वर्तमानकाल के प्रथमपुरुष के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रेरणार्थक-भाव में अन्तिम दोनों रूप 'भमावइ और भमावेइ' क्रम से सिद्ध हो जाते हैं।।३-१५१।।
लुगावी-क्त-भाव कर्मसु।।३-१५२।। णेः स्थाने लुक् आवि इत्यादेशो भवतः क्ते भावकर्मविहिते च प्रत्यये परतः।। कारिओ करावि हासि। हसाविआ खामि। खमावि।। भाव कर्मणोः।। कारीअइ। करावीअइ। कारिज्जइ। कराविज्जइ। हासीअइ। हसावीअइ। हासिज्जइ। हसाविज्जइ।। ___ अर्थः- जिस समय में प्राकृत धातुओं में भूतकृदन्त सम्बन्धी प्रत्यय 'त' लगा हुआ हो अथवा भाव वाच्य एवं कर्मणि वाच्य सम्बन्धी प्रत्यय लगे हुए हों, तो उन धातुओं में प्ररेणार्थक-भाव की निर्माण अवस्था में सूत्र-संख्या ३-१४९ में वर्णित प्रेरणार्थक भाव प्रदर्शक प्रत्यय 'अत्' एत्' आव और आवे' का या तो लोप हो जायेगा अथवा इन प्रत्ययों के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'आवि' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति हो जायेगी और उन धातुओं का भूत कृदन्त अर्थ सहित अथवा भाववाच्य कर्मवाच्य अर्थ सहित प्रेरणार्थक रूप का निर्माण हो जायेगा। उदाहरण इस प्रकार हैं:- कारितम् कारिअं अथवा कराविकराया हुआ; हासितम्-हासिअं अथवा हसाविअं-हँसाया हुआ और क्षामितम् खामिअं अथवा खमाविअंक्षमाया हुआ; ये उदाहरण भूतकृदन्त सम्बन्धी हैं; इनमें से प्रथम रूपों में प्रेरणार्थक किया का सद्भाव प्रदर्शित किया जाता हुआ होने पर भी इनमें सूत्र-संख्या ३-१४९ के अनुसार प्राकृत में णिजन्त अर्थबोधक प्रत्यय 'अत् एत् आव और आवे' का लोप प्रदर्शित किया गया है। जबकि द्वितीय रूपों में प्रेरणार्थक भाव में प्रत्ययों के स्थान पर आदेश-प्राप्त प्रत्यय 'आवि' का सद्-भाव प्रदर्शित किया गया है। भाववाचक और कर्मणिवाचक उदाहरण इस प्रकार है:- कार्यकारीअइ, करावीअइ, कारिज्जइ और कराविज्जइ-उससे कराया जाता है; हास्यते-हासी-अइ हसावीअइ, हासिज्जइ और हसाविज्जइ उससे हंसाया जाता है। इन उदाहरणों में भी अर्थात् 'कारीअइ, कारिज्जइ, हासीअइ और हासिज्जइ' में तो प्रेरणार्थक-भाव-प्रदर्शक-प्रत्ययों का अभाव प्रदर्शित करते हुए भी प्रेरणार्थक-भाव का सद्भाव प्रदर्शित किया गया है। जबकि शेष उदाहरणों में अर्थात् कारावीअइ, कराविज्जइ, हसावीअइ और हसाविज्जई' में प्रेरणार्थक-भाव-प्रदर्शक-प्रत्यय 'अत् एत्' 'आव और आवे' के स्थान पर 'आवि' प्रत्यय की आदेश प्राप्ति प्रदर्शित करते हुए प्रेरणार्थक-भाव का सद्भाव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अन्यत्र भी यह समझ लेना चाहिये कि प्राकृत भाषा में धातुओं में भूत-कृदन्त सम्बन्धी प्रत्यय 'त' और भाव वाच्य कर्मवाच्य प्रत्ययों के परे रहने पर णिजन्त बोधक प्रत्ययों का या तो ले जायगा अथवा इन प्रत्ययों के स्थान पर 'आवि' प्रत्यय की वैकल्पिक रूप से आदेश प्राप्ति हो जायगी।
कारितम संस्कत का भत-कदन्तीय रूप है। इसके प्राकत रूप कारिअं और कराविअं होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या ३-१५३ से मूल प्राकृत धातु 'कर' में स्थित आदि स्वर 'अ' के स्थान पर आगे भूत कृदन्तीय प्रत्यय का सद्भाव होने से ३-१५२ द्वारा प्रेरणार्थक-भाव प्रदर्शक-प्रत्यय का लोप हो जाने से 'आ' की प्राप्ति; ३-१५६ से प्राप्तांग 'कार' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर आगे भूत-कृदन्त वाचक प्रत्यय 'त' का सद्भाव होने से 'इ' की प्राप्ति; ४-४४८ से प्राप्तांग 'कारि' में भूत कृदन्त-वाचक संस्कृत प्रत्यय 'त्'के समान ही प्राकृत में भी 'त' प्रत्यय की प्राप्ति; १-१७७ से प्राप्त प्रत्यय 'त' में से हलन्त व्यंजन 'त्' का लोप; ३-२५ से प्राप्तांग 'कारिअ' में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'सि' के स्थान पर प्राकृत में 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त प्रत्यय 'म्' को पूर्व वर्ण पर अनुस्वार की प्राप्ति होकर भूतकृदन्तीय प्रेरणार्थक भाव सूचक प्रथमान्त एकवचनीय प्राकृत पद कारिअंसिद्ध हो जाता है। ___ कराविअं में सूत्र-संख्या ३-१५२ से मूल प्राकृत धातु-'कर' में प्रेरणार्थक भाव प्रदर्शक प्रत्यय 'आवि' की प्राप्ति; और शेष साधनिका प्रथम रूप के समान ही प्राप्त होकर द्वितीय रूप कराविअं भी सिद्ध हो जाता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org