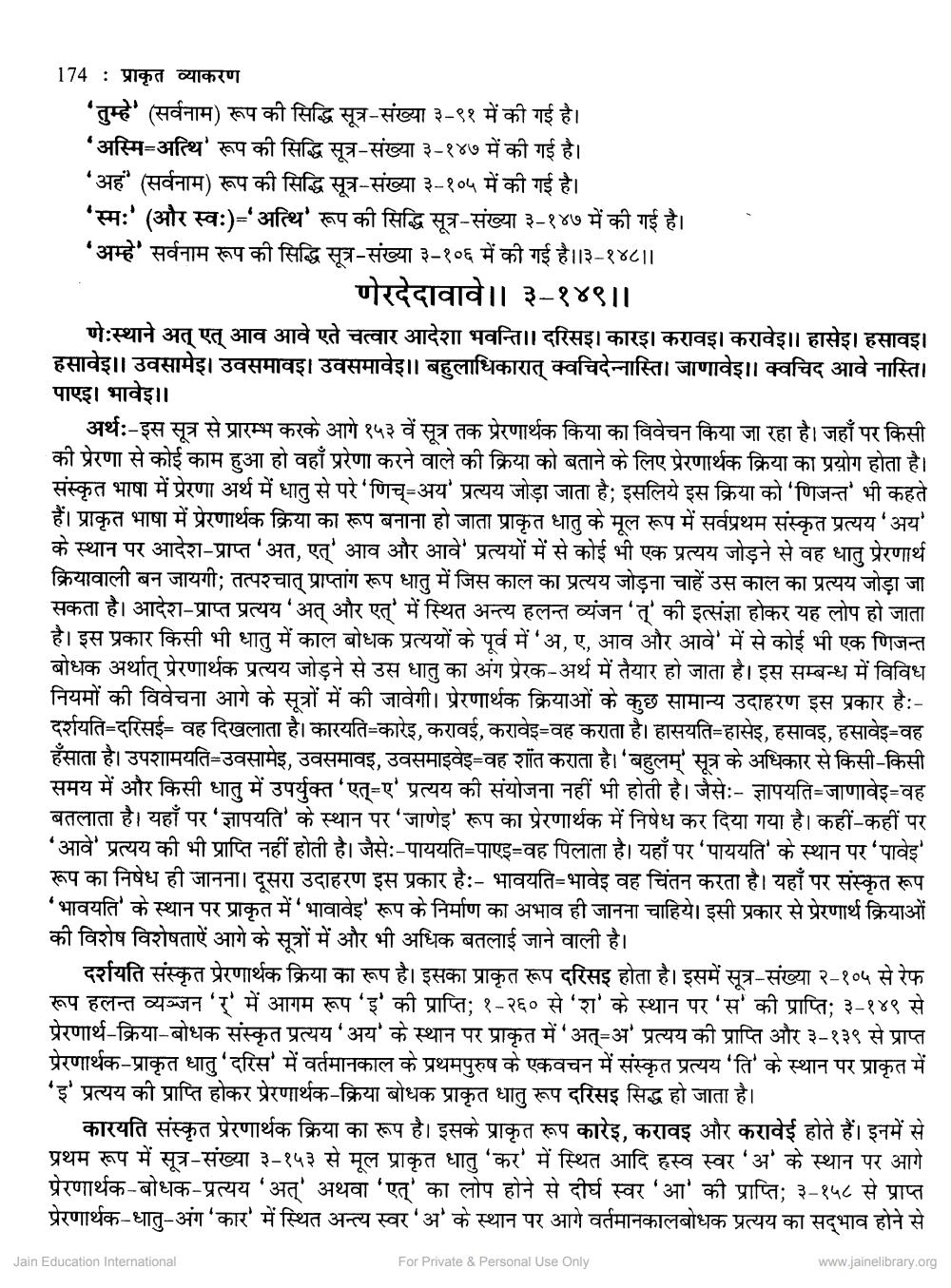________________
174 : प्राकृत व्याकरण
'तुम्हे' (सर्वनाम) रूप की सिद्धि सूत्र - संख्या ३ - ९१ में की गई है। 'अस्मि - अत्थि' रूप की सिद्धि सूत्र - संख्या ३ -१४७ में की गई है। 'अहं' (सर्वनाम) रूप की सिद्धि सूत्र - संख्या ३- १०५ में की गई है। 'स्मः' ( और स्वः) = ' अत्थि' रूप की सिद्धि सूत्र - संख्या ३ -१४७ में की गई है। 'अम्हे' सर्वनाम रूप की सिद्धि सूत्र - संख्या ३- १०६ में की गई है । । ३ - १४८ ।।
णेरदेदावावे।। ३-१४९।।
स्थाने अत् एत् आव आवे एते चत्वार आदेशा भवन्ति ।। दरिसइ । कार । करावइ । करावे ।। हासे । हसावइ । हसावेइ।। उवसामेइ। उवसमावइ । उवसमावेइ ।। बहुलाधिकारात् क्वचिदेन्नास्ति । जाणावेइ ॥ क्वचिद आवे नास्ति । पाएइ । भावेइ ||
अर्थः- इस सूत्र से प्रारम्भ करके आगे १५३ वें सूत्र तक प्रेरणार्थक किया का विवेचन किया जा रहा है। जहाँ पर किसी प्रेरणा से कोई काम हुआ हो वहाँ प्ररेणा करने वाले की क्रिया को बताने के लिए प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में प्रेरणा अर्थ में धातु से परे 'णिच्=अय' प्रत्यय जोड़ा जाता है; इसलिये इस क्रिया को 'णिजन्त' भी कहते हैं। । प्राकृत भाषा में प्रेरणार्थक क्रिया का रूप बनाना हो जाता प्राकृत धातु के मूल रूप में सर्वप्रथम संस्कृत प्रत्यय 'अय' के स्थान पर आदेश - प्राप्त 'अत, एत्' आव और आवे' प्रत्ययों में से कोई भी एक प्रत्यय जोड़ने से वह धातु प्रेरणार्थ क्रियावाली बन जायगी; तत्पश्चात् प्राप्तांग रूप धातु में जिस काल का प्रत्यय जोड़ना चाहें उस काल का प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। आदेश प्राप्त प्रत्यय ' अत् और एत्' में स्थित अन्त्य हलन्त व्यंजन 'तू' की इत्संज्ञा होकर यह लोप हो जाता है। इस प्रकार किसी भी धातु में काल बोधक प्रत्ययों के पूर्व में 'अ, ए, आव और आवे' में से कोई भी एक णिजन्त बोधक अर्थात् प्रेरणार्थक प्रत्यय जोड़ने से उस धातु का अंग प्रेरक अर्थ में तैयार हो जाता है। इस सम्बन्ध में विविध नियमों की विवेचना आगे के सूत्रों में की जावेगी । प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार है:दर्शयति-दरिसई = वह दिखलाता है। कारयति-कारेइ, करावई, करावेइ = वह कराता है । हासयति हासेइ, हसावइ, हसावेइ = वह हँसाता है। उपशामयति-उवसामेइ, उवसमावइ, उवसमाइवेइ = वह शांत कराता है। 'बहुलम्' सूत्र के अधिकार से किसी-किसी समय में और किसी धातु में उपर्युक्त ' एत्-ए' प्रत्यय की संयोजना नहीं भी होती है। जैसे:- ज्ञापयति-जाणावेइ-वह बतलाता है। यहाँ पर 'ज्ञापयति' के स्थान पर 'जाणेइ' रूप का प्रेरणार्थक में निषेध कर दिया गया है। कहीं-कहीं पर ' आवे' प्रत्यय की भी प्राप्ति नहीं होती है। जैसे :- पाययति = पाएइ = वह पिलाता है। यहाँ पर 'पाययति' के स्थान पर 'पावेइ' रूप का निषेध ही जानना। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है:- भावयति = भावेइ वह चिंतन करता है। यहाँ पर संस्कृत रूप
4
'भावयति' के स्थान पर प्राकृत में 'भावावेइ' रूप के निर्माण का अभाव ही जानना चाहिये। इसी प्रकार से प्रेरणार्थ क्रियाओं की विशेष विशेषताऐं आगे के सूत्रों में और भी अधिक बतलाई जाने वाली है।
दर्शयति संस्कृत प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। इसका प्राकृत रूप दरिसइ होता है। इसमें सूत्र - संख्या २ - १०५ से रेफ रूप हलन्त व्यञ्जन 'र्' में आगम रूप 'इ' की प्राप्ति; १ - २६० से 'श' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति; ३-१४९ से प्रेरणार्थ- क्रिया-बोधक संस्कृत प्रत्यय 'अय' के स्थान पर प्राकृत में 'अत्-अ' प्रत्यय की प्राप्ति और ३- १३९ से प्राप्त प्रेरणार्थक- प्राकृत धातु 'दरिस' में वर्तमानकाल के प्रथमपुरुष के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रेरणार्थक क्रिया बोधक प्राकृत धातु रूप दरिसइ सिद्ध हो जाता है।
कारयति संस्कृत प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। इसके प्राकृत रूप कारेइ, करावइ और करावेई होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र - संख्या ३ - १५३ से मूल प्राकृत धातु 'कर' में स्थित आदि ह्रस्व स्वर 'अ' के स्थान पर आगे प्रेरणार्थक- बोधक-प्रत्यय 'अत्' अथवा 'एत्' का लोप होने से दीर्घ स्वर 'आ' की प्राप्ति; ३ - १५८ से प्राप्त प्रेरणार्थक- धातु-अंग 'कार' में स्थित अन्त्य स्वर 'अ' के स्थान पर आगे वर्तमानकालबोधक प्रत्यय का सद्भाव होने से
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International