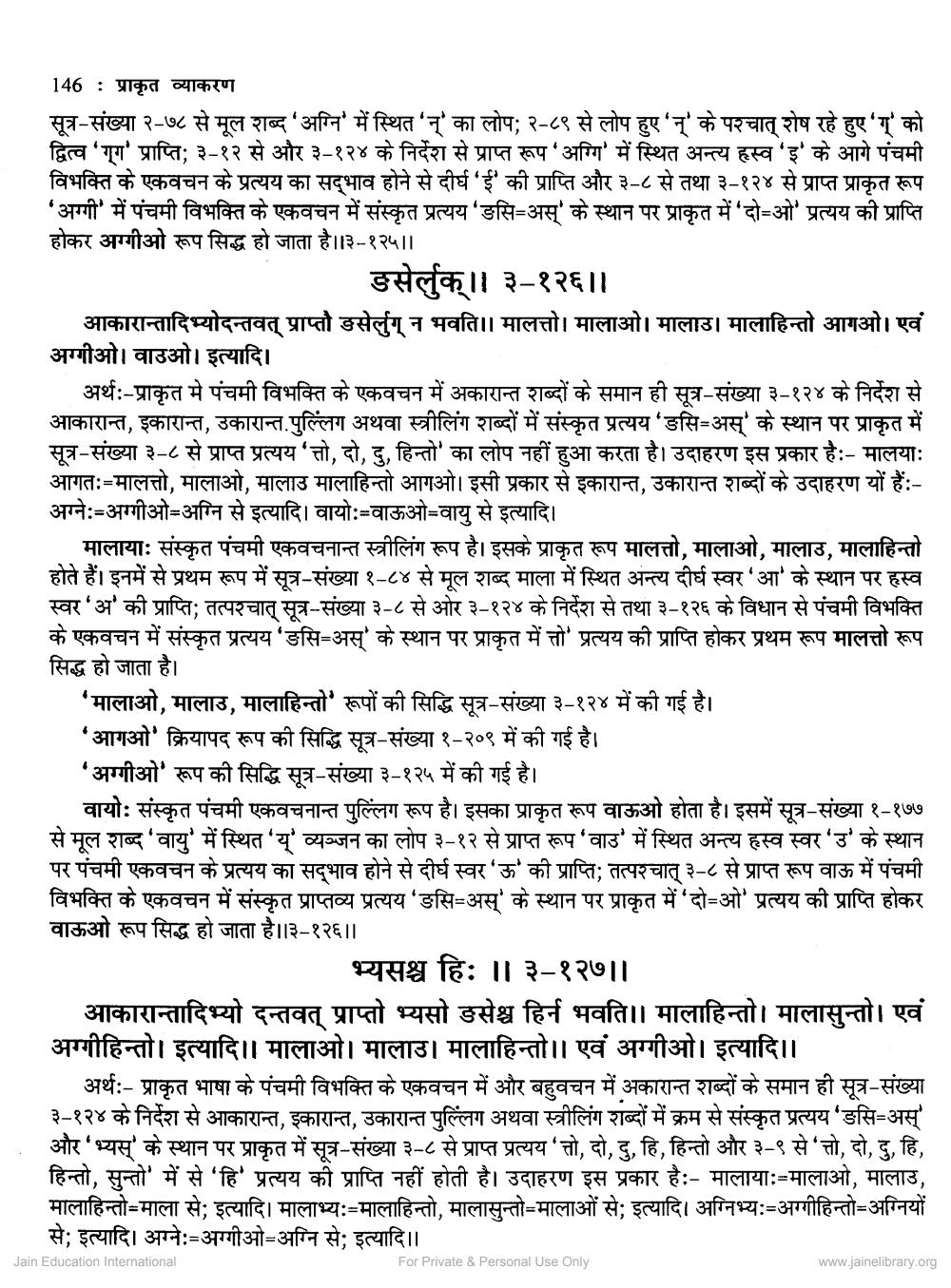________________
146 : प्राकृत व्याकरण सूत्र-संख्या २-७८ से मूल शब्द 'अग्नि' में स्थित 'न्' का लोप; २-८९ से लोप हुए 'न्' के पश्चात् शेष रहे हुए 'ग्' को द्वित्व 'ग्ग' प्राप्ति; ३-१२ से और ३-१२४ के निर्देश से प्राप्त रूप 'अग्गि' में स्थित अन्त्य हृस्व 'इ' के आगे पंचमी विभक्ति के एकवचन के प्रत्यय का सद्भाव होने से दीर्घ 'ई' की प्राप्ति और ३-८ से तथा ३-१२४ से प्राप्त प्राकृत रूप 'अग्गी में पंचमी विभक्ति के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय ‘ङसि-अस्' के स्थान पर प्राकृत में 'दो-ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अग्गीओ रूप सिद्ध हो जाता है।।३-१२५।।
ङसेलक्॥ ३-१२६॥ आकारान्तादिभ्योदन्तवत् प्राप्तौ उसे ग् न भवति।। मालत्तो। मालाओ। मालाउ। मालाहिन्तो आगओ। एवं अग्गीओ। वाउओ। इत्यादि।
अर्थः-प्राकृत मे पंचमी विभक्ति के एकवचन में अकारान्त शब्दों के समान ही सूत्र-संख्या ३-१२४ के निर्देश से आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त.पुल्लिग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों में संस्कृत प्रत्यय 'ङसि-अस् के स्थान पर प्राकृत में सूत्र-संख्या ३-८ से प्राप्त प्रत्यय 'त्तो, दो, दु, हिन्तो' का लोप नहीं हुआ करता है। उदाहरण इस प्रकार है:- मालयाः आगतः मालत्तो, मालाओ, मालाउ मालाहिन्तो आगओ। इसी प्रकार से इकारान्त, उकारान्त शब्दों के उदाहरण यों हैं:अग्ने:-अग्गीओ=अग्नि से इत्यादि। वायोः वाऊओ-वायु से इत्यादि।
मालायाः संस्कृत पंचमी एकवचनान्त स्त्रीलिंग रूप है। इसके प्राकृत रूप मालत्तो, मालाओ, मालाउ, मालाहिन्तो होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र-संख्या १-८४ से मूल शब्द माला में स्थित अन्त्य दीर्घ स्वर 'आ' के स्थान पर हस्व स्वर 'अ की प्राप्ति; तत्पश्चात् सूत्र-संख्या ३-८ से ओर ३-१२४ के निर्देश से तथा ३-१२६ के विधान से पंचमी विभक्ति के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'ङसि-अस्' के स्थान पर प्राकृत में त्तो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप मालत्तो रूप सिद्ध हो जाता है।
'मालाओ, मालाउ, मालाहिन्तो' रूपों की सिद्धि सूत्र-संख्या ३–१२४ में की गई है। 'आगओ' क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या १-२०९ में की गई है। 'अग्गीओ' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या ३-१२५ में की गई है।
वायोः संस्कृत पंचमी एकवचनान्त पुल्लिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप वाऊओ होता है। इसमें सूत्र-संख्या १-१७७ से मूल शब्द 'वायु में स्थित 'य' व्यञ्जन का लोप ३-१२ से प्राप्त रूप 'वाउ' में स्थित अन्त्य हस्व स्वर 'उ' के स्थान पर पंचमी एकवचन के प्रत्यय का सद्भाव होने से दीर्घ स्वर 'ऊ की प्राप्ति; तत्पश्चात् ३-८ से प्राप्त रूप वाऊ में पंचमी विभक्ति के एकवचन में संस्कृत प्राप्तव्य प्रत्यय 'ङसि-अस्' के स्थान पर प्राकृत में 'दो-ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर वाऊओ रूप सिद्ध हो जाता है।।३-१२६।।
भ्यसश्च हिः ॥३-१२७।। आकारान्तादिभ्यो दन्तवत् प्राप्तो भ्यसो उसेश्च हिर्न भवति।। मालाहिन्तो। मालासुन्तो। एवं अग्गीहिन्तो। इत्यादि।। मालाओ। मालाउ। मालाहिन्तो।। एवं अग्गीओ। इत्यादि।।
अर्थः- प्राकृत भाषा के पंचमी विभक्ति के एकवचन में और बहवचन में अकारान्त शब्दों के समान ही सूत्र-संख्या ३-१२४ के निर्देश से आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों में क्रम से संस्कृत प्रत्यय 'ङसि अस्'
और 'भ्यस्' के स्थान पर प्राकृत में सूत्र-संख्या ३-८ से प्राप्त प्रत्यय 'त्तो, दो, दु, हि, हिन्तो और ३-९ से 'त्तो, दो, दु, हि, हिन्तो, सुन्तो' में से 'हि' प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होती है। उदाहरण इस प्रकार है:- मालायाः मालाओ, मालाउ, मालाहिन्तो माला से; इत्यादि। मालाभ्यः मालाहिन्तो, मालासुन्तो-मालाओं से; इत्यादि। अग्निभ्यः अग्गीहिन्तो अग्नियों
से; इत्यादि। अग्ने: अग्गीओ अग्नि से; इत्यादि।। Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org