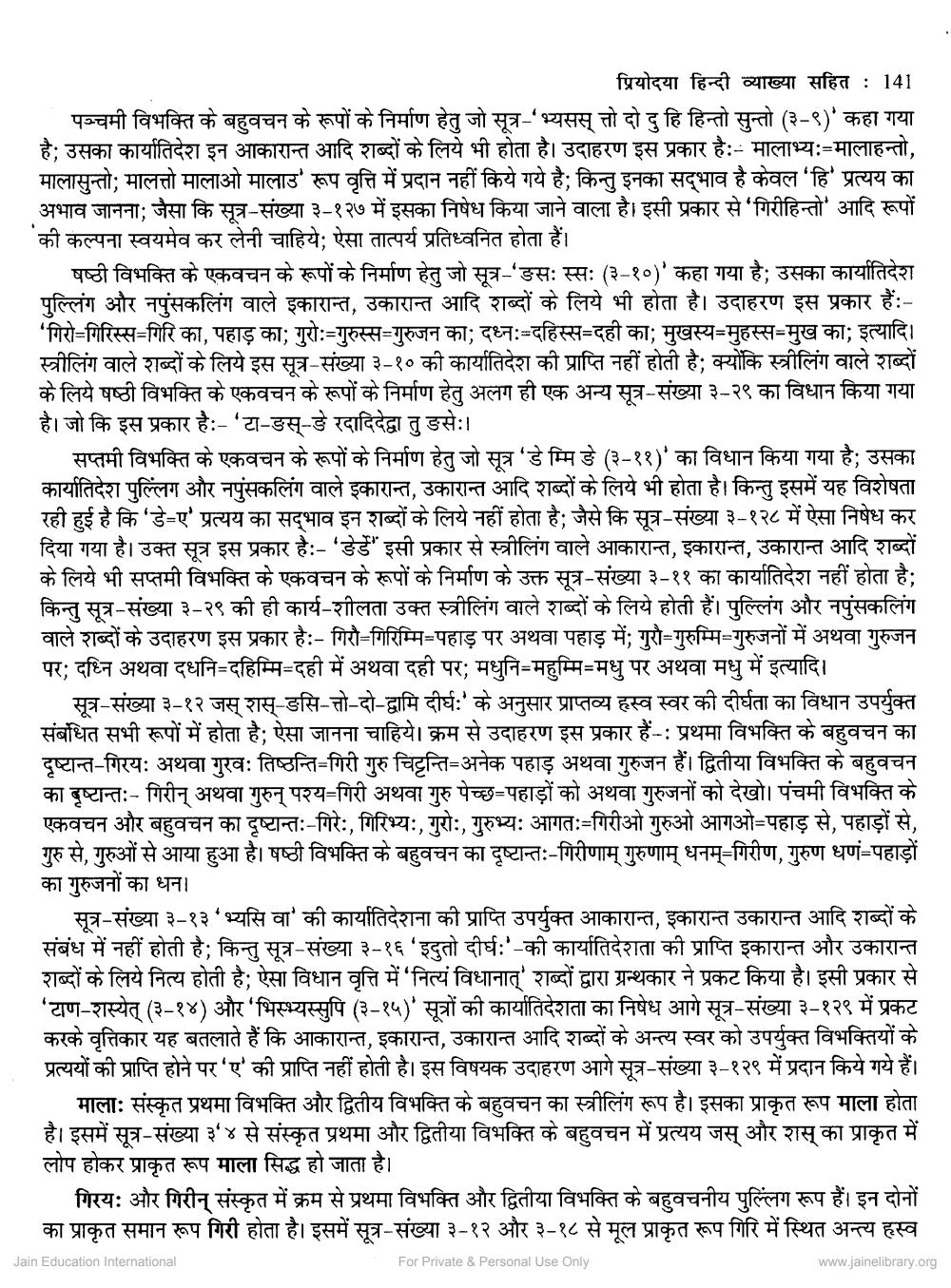________________
प्रियोदया हिन्दी व्याख्या सहित : 141 पञ्चमी विभक्ति के बहुवचन के रूपों के निर्माण हेतु जो सूत्र-'भ्यसस् त्तो दो दु हि हिन्तो सुन्तो (३-९) कहा गया है; उसका कार्यातिदेश इन आकारान्त आदि शब्दों के लिये भी होता है। उदाहरण इस प्रकार है:- मालाभ्यः-मालाहन्तो, मालासुन्तो; मालत्तो मालाओ मालाउ रूप वृत्ति में प्रदान नहीं किये गये है; किन्तु इनका सद्भाव है केवल 'हि' प्रत्यय का अभाव जानना; जैसा कि सूत्र-संख्या ३-१२७ में इसका निषेध किया जाने वाला है। इसी प्रकार से 'गिरीहिन्तो' आदि रूपों की कल्पना स्वयमेव कर लेनी चाहिये; ऐसा तात्पर्य प्रतिध्वनित होता हैं।
षष्ठी विभक्ति के एकवचन के रूपों के निर्माण हेतु जो सूत्र-'ङसः स्सः (३-१०) कहा गया है; उसका कार्यातिदेश पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले इकारान्त, उकारान्त आदि शब्दों के लिये भी होता है। उदाहरण इस प्रकार हैं:'गिरो-गिरिस्स-गिरि का, पहाड़ का; गुरोः गुरुस्स-गुरुजन का; दधनः-दहिस्स-दही का; मुखस्य-मुहस्स-मुख का; इत्यादि। स्त्रीलिंग वाले शब्दों के लिये इस सूत्र-संख्या ३-१० की कार्यातिदेश की प्राप्ति नहीं होती है; क्योंकि स्त्रीलिंग वाले शब्दों के लिये षष्ठी विभक्ति के एकवचन के रूपों के निर्माण हेतु अलग ही एक अन्य सूत्र-संख्या ३-२९ का विधान किया गया है। जो कि इस प्रकार है:- 'टा-ङस्-डे रदादिदेद्वा तु ङसेः।
सप्तमी विभक्ति के एकवचन के रूपों के निर्माण हेतु जो सूत्र 'डे म्मि डे (३-११) का विधान किया गया है; उसका कार्यातिदेश पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले इकारान्त, उकारान्त आदि शब्दों के लिये भी होता है। किन्तु इसमें यह विशेषता रही हुई है कि 'डे-ए' प्रत्यय का सद्भाव इन शब्दों के लिये नहीं होता है; जैसे कि सूत्र-संख्या ३-१२८ में ऐसा निषेध कर दिया गया है। उक्त सूत्र इस प्रकार है:- 'डे." इसी प्रकार से स्त्रीलिंग वाले आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त आदि शब्दों के लिये भी सप्तमी विभक्ति के एकवचन के रूपों के निर्माण के उक्त सूत्र-संख्या ३-११ का कार्यातिदेश नहीं होता है; किन्तु सूत्र-संख्या ३-२९ की ही कार्य-शीलता उक्त स्त्रीलिंग वाले शब्दों के लिये होती हैं। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले शब्दों के उदाहरण इस प्रकार है:- गिरी-गिरिम्मि-पहाड़ पर अथवा पहाड़ में; गुरौ-गुरुम्मि गुरुजनों में अथवा गुरुजन पर; दधिन अथवा दधनि-दहिम्मि-दही में अथवा दही पर; मधुनि-महुम्मि-मधु पर अथवा मधु में इत्यादि।
सूत्र-संख्या ३-१२ जस् शस्-ङसि-तो-दो-द्वामि दीर्घः' के अनुसार प्राप्तव्य हस्व स्वर की दीर्घता का विधान उपर्युक्त संबंधित सभी रूपों में होता है; ऐसा जानना चाहिये। क्रम से उदाहरण इस प्रकार हैं--: प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का दृष्टान्त-गिरयः अथवा गुरवः तिष्ठन्ति गिरी गुरु चिट्टन्ति अनेक पहाड़ अथवा गुरुजन हैं। द्वितीया विभक्ति के बहुवचन का दृष्टान्तः- गिरीन् अथवा गुरुन् पश्य=गिरी अथवा गुरु पेच्छ-पहाड़ों को अथवा गुरुजनों को देखो। पंचमी विभक्ति के एकवचन और बहुवचन का दृष्टान्तः-गिरेः, गिरिभ्यः, गुरोः, गुरुभ्यः आगतः गिरीओ गुरुओ आगओ-पहाड़ से, पहाड़ों से, गुरु से, गुरुओं से आया हुआ है। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का दृष्टान्तः-गिरीणाम् गुरुणाम् धनम् गिरीण, गुरुण धणं-पहाड़ों का गुरुजनों का धन। __सूत्र-संख्या ३-१३ भ्यसि वा' की कार्यातिदेशना की प्राप्ति उपर्युक्त आकारान्त, इकारान्त उकारान्त आदि शब्दों के संबंध में नहीं होती है; किन्तु सूत्र-संख्या ३-१६ 'इदुतो दीर्घः'-की कार्यातिदेशता की प्राप्ति इकारान्त और उकारान्त शब्दों के लिये नित्य होती है; ऐसा विधान वृत्ति में 'नित्यं विधानात्' शब्दों द्वारा ग्रन्थकार ने प्रकट किया है। इसी प्रकार से 'टाण-शस्येत् (३-१४) और 'भिस्भ्यस्सुपि (३-१५) सूत्रों की कार्यातिदेशता का निषेध आगे सूत्र-संख्या ३-१२९ में प्रकट करके वृत्तिकार यह बतलाते हैं कि आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त आदि शब्दों के अन्त्य स्वर को उपर्युक्त विभक्तियों के प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर 'ए' की प्राप्ति नहीं होती है। इस विषयक उदाहरण आगे सूत्र-संख्या ३-१२९ में प्रदान किये गये हैं। ____ मालाः संस्कृत प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का स्त्रीलिंग रूप है। इसका प्राकृत रूप माला होता है। इसमें सूत्र-संख्या ३४ से संस्कृत प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय जस् और शस् का प्राकृत में लोप होकर प्राकृत रूप माला सिद्ध हो जाता है।
गिरयः और गिरीन् संस्कृत में क्रम से प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति के बहुवचनीय पुल्लिंग रूप हैं। इन दोनों का प्राकृत समान रूप गिरी होता है। इसमें सूत्र-संख्या ३-१२ और ३-१८ से मूल प्राकृत रूप गिरि में स्थित अन्त्य हस्व
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org