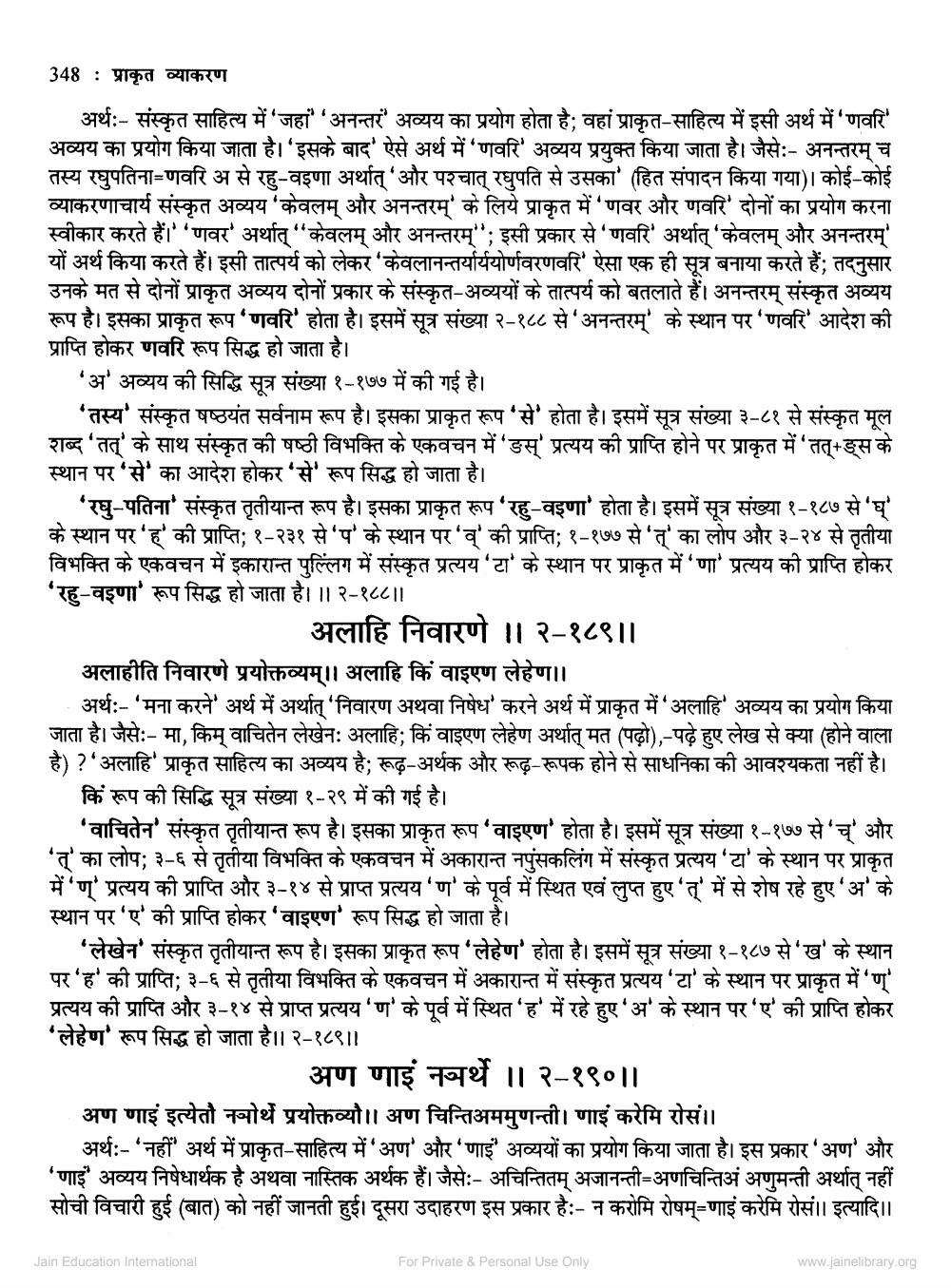________________
348 : प्राकृत व्याकरण
अर्थः- संस्कृत साहित्य में जहां 'अनन्तरं अव्यय का प्रयोग होता है; वहां प्राकृत-साहित्य में इसी अर्थ में 'णवरि' अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऐसे अर्थ में 'णवरि' अव्यय प्रयुक्त किया जाता है। जैसेः- अनन्तरम् च तस्य रघुपतिना=णवरि अ से रहु-वइणा अर्थात् 'और पश्चात् रघुपति से उसका' (हित संपादन किया गया)। कोई-कोई व्याकरणाचार्य संस्कृत अव्यय 'केवलम् और अनन्तरम्' के लिये प्राकृत में णवर और णवरि' दोनों का प्रयोग करना स्वीकार करते हैं। 'णवर' अर्थात् "केवलम् और अनन्तरम्'; इसी प्रकार से 'णवरि' अर्थात् 'केवलम् और अनन्तरम्' यों अर्थ किया करते हैं। इसी तात्पर्य को लेकर केवलानन्तर्यार्ययोर्णवरणवरि' ऐसा एक ही सूत्र बनाया करते हैं; तदनुसार उनके मत से दोनों प्राकृत अव्यय दोनों प्रकार के संस्कृत-अव्ययों के तात्पर्य को बतलाते हैं। अनन्तरम् संस्कृत अव्यय रूप है। इसका प्राकृत रूप णवरि' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-१८८ से 'अनन्तरम्' के स्थान पर 'णवरि' आदेश की प्राप्ति होकर णवरि रूप सिद्ध हो जाता है।
'अ' अव्यय की सिद्धि सूत्र संख्या १-१७७ में की गई है।
"तस्य' संस्कृत षष्ठयंत सर्वनाम रूप है। इसका प्राकृत रूप से होता है। इसमें सूत्र संख्या ३-८१ से संस्कृत मूल शब्द 'तत्' के साथ संस्कृत की षष्ठी विभक्ति के एकवचन में 'ङस्' प्रत्यय की प्राप्ति होने पर प्राकृत में 'तत्+ङ्स के स्थान पर 'से' का आदेश होकर 'से' रूप सिद्ध हो जाता है।
'रघु-पतिना' संस्कृत तृतीयान्त रूप है। इसका प्राकृत रूप 'रहु-वइणा' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१८७ से 'घ' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; १-२३१ से 'प' के स्थान पर 'व' की प्राप्ति; १-१७७ से 'त्' का लोप और ३-२४ से तृतीया विभक्ति के एकवचन में इकारान्त पुल्लिंग में संस्कृत प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत में 'णा' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'रहु-वइणा' रूप सिद्ध हो जाता है। ।। २-१८८।।
अलाहि निवारणे ।। २-१८९।। अलाहीति निवारणे प्रयोक्तव्यम्।। अलाहि किं वाइएण लेहेण।।
अर्थः- 'मना करने अर्थ में अर्थात् 'निवारण अथवा निषेध करने अर्थ में प्राकृत में 'अलाहि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे:- मा, किम् वाचितेन लेखेनः अलाहि; किं वाइएण लेहेण अर्थात् मत (पढ़ो),-पढ़े हुए लेख से क्या (होने वाला है)? 'अलाहि' प्राकृत साहित्य का अव्यय है; रूढ़-अर्थक और रूढ़-रूपक होने से साधनिका की आवश्यकता नहीं है।
किं रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-२९ में की गई है।
'वाचितेन' संस्कृत तृतीयान्त रूप है। इसका प्राकृत रूप 'वाइएण' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१७७ से 'च्' और 'त्' का लोप; ३-६ से तृतीया विभक्ति के एकवचन में अकारान्त नपुंसकलिंग में संस्कृत प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१४ से प्राप्त प्रत्यय 'ण' के पूर्व में स्थित एवं लुप्त हुए 'त्' में से शेष रहे हुए 'अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति होकर 'वाइएण' रूप सिद्ध हो जाता है।
'लेखेन' संस्कृत तृतीयान्त रूप है। इसका प्राकृत रूप 'लेहेण होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१८७ से 'ख' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; ३-६ से तृतीया विभक्ति के एकवचन में अकारान्त में संस्कृत प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१४ से प्राप्त प्रत्यय 'ण' के पूर्व में स्थित 'ह' में रहे हुए 'अ' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति होकर 'लेहेण रूप सिद्ध हो जाता है।। २-१८९॥
अण णाई नबर्थे ।। २-१९०॥ अण णाई इत्येतो नबोर्थ प्रयोक्तव्यौ।। अण चिन्तिअममुणन्ती। णाई करेमि रोसं।।
अर्थः- 'नहीं' अर्थ में प्राकृत-साहित्य में अण' और 'णाई अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 'अण' और 'णाई अव्यय निषेधार्थक है अथवा नास्तिक अर्थक हैं। जैसे:- अचिन्तितम् अजानन्ती अणचिन्तिअं अणुमन्ती अर्थात् नहीं सोची विचारी हुई (बात) को नहीं जानती हुई। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है:- न करोमि रोषम्=णाई करेमि रोसं।। इत्यादि।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org