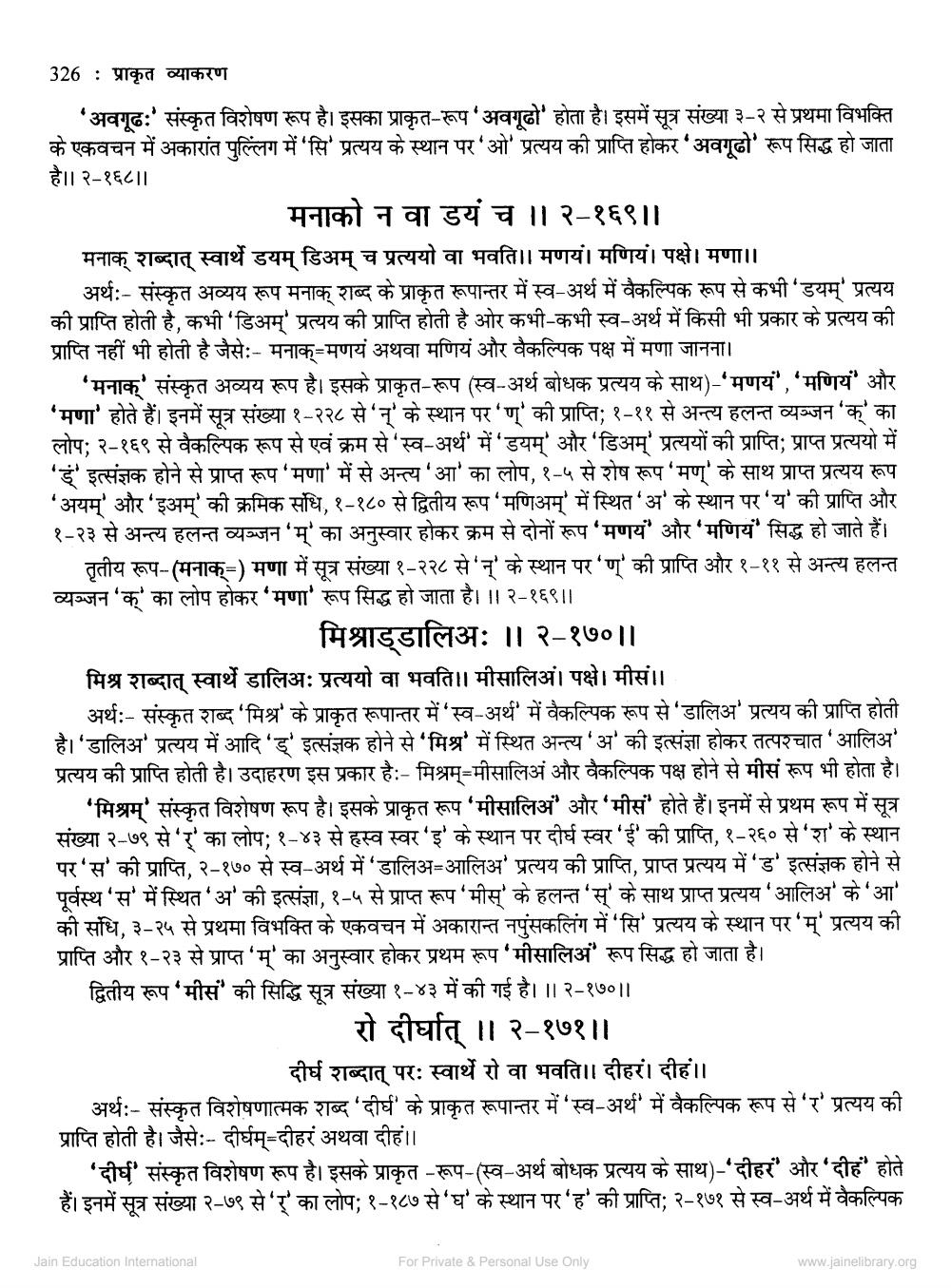________________
326 : प्राकृत व्याकरण
'अवगूढः' संस्कृत विशेषण रूप है। इसका प्राकृत-रूप 'अवगूढो' होता है। इसमें सूत्र संख्या ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारांत पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'अवगूढो रूप सिद्ध हो जाता है।। २-१६८।।
मनाको न वा डयं च ।। २-१६९।। मनाक् शब्दात् स्वार्थे डयम् डिअम् च प्रत्ययो वा भवति।। मणयं। मणिय। पक्षे। मणा।।
अर्थः- संस्कृत अव्यय रूप मनाक् शब्द के प्राकृत रूपान्तर में स्व-अर्थ में वैकल्पिक रूप से कभी 'डयम्' प्रत्यय की प्राप्ति होती है, कभी 'डिअम्' प्रत्यय की प्राप्ति होती है ओर कभी-कभी स्व-अर्थ में किसी भी प्रकार के प्रत्यय की प्राप्ति नहीं भी होती है जैसेः- मनाक्-मणयं अथवा मणियं और वैकल्पिक पक्ष में मणा जानना।
'मनाक्' संस्कृत अव्यय रूप है। इसके प्राकृत-रूप (स्व-अर्थ बोधक प्रत्यय के साथ)-'मणयं', 'मणियं' और 'मणा' होते हैं। इनमें सूत्र संख्या १-२२८ से 'न्' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति; १-११ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 'क्' का लोप; २-१६९ से वैकल्पिक रूप से एवं क्रम से 'स्व-अर्थ' में 'डयम्' और 'डिअम्' प्रत्ययों की प्राप्ति; प्राप्त प्रत्ययो में 'ड्' इत्संज्ञक होने से प्राप्त रूप 'मणा' में से अन्त्य 'आ' का लोप, १-५ से शेष रूप 'मण' के साथ प्राप्त प्रत्यय रूप 'अयम्' और 'इअम्' की क्रमिक संधि, १-१८० से द्वितीय रूप 'मणिअम्' में स्थित 'अ' के स्थान पर 'य' की प्राप्ति और १-२३ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 'म्' का अनुस्वार होकर क्रम से दोनों रूप 'मणयं' और 'मणियं सिद्ध हो जाते हैं।
तृतीय रूप-(मनाक्=) मणा में सूत्र संख्या १-२२८ से 'न्' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति और १-११ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 'क्' का लोप होकर 'मणा' रूप सिद्ध हो जाता है। ।। २-१६९।।
मिश्राड्डालिअः ॥२-१७०॥ मिश्र शब्दात् स्वार्थे डालिअः प्रत्ययो वा भवति।। मीसालि पक्षे। मीसं।।
अर्थः- संस्कृत शब्द 'मिश्र के प्राकृत रूपान्तर में 'स्व-अर्थ' में वैकल्पिक रूप से 'डालिअ' प्रत्यय की प्राप्ति होती है। 'डालिअ प्रत्यय में आदि 'ड्' इत्संज्ञक होने से 'मिश्र में स्थित अन्त्य 'अ' की इत्संज्ञा होकर तत्पश्चात 'आलिअ' प्रत्यय की प्राप्ति होती है। उदाहरण इस प्रकार है:- मिश्रम्=मीसालिअं और वैकल्पिक पक्ष होने से मीसं रूप भी होता है। _ 'मिश्रम् संस्कृत विशेषण रूप है। इसके प्राकृत रूप 'मीसालि और 'मीसं' होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र संख्या २-७९ से 'र' का लोप; १-४३ से हस्व स्वर 'इ' के स्थान पर दीर्घ स्वर 'ई' की प्राप्ति, १-२६० से 'श' के स्थान पर 'स' की प्राप्ति, २-१७० से स्व-अर्थ में 'डालिअ-आलिअ' प्रत्यय की प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय में 'ड' इत्संज्ञक होने से पूर्वस्थ 'स' में स्थित 'अ' की इत्संज्ञा, १-५ से प्राप्त रूप 'मीस्' के हलन्त 'स्' के साथ प्राप्त प्रत्यय 'आलिअ के 'आ' की संधि, ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त नपुंसकलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर प्रथम रूप 'मीसालिअं रूप सिद्ध हो जाता है। द्वितीय रूप 'मीसं' की सिद्धि सूत्र संख्या १-४३ में की गई है। ।। २-१७०॥
रो दीर्घात् ।। २-१७१॥
दीर्घ शब्दात् परः स्वार्थे रो वा भवति।। दीहरं। दीह।। अर्थः- संस्कृत विशेषणात्मक शब्द 'दीर्घ' के प्राकृत रूपान्तर में स्व-अर्थ' में वैकल्पिक रूप से 'र' प्रत्यय की प्राप्ति होती है। जैसे:- दीर्घम्=दीहरं अथवा दीहं।।
'दीर्घ संस्कृत विशेषण रूप है। इसके प्राकृत -रूप-(स्व-अर्थ बोधक प्रत्यय के साथ)-'दीहर' और 'दीह' होते हैं। इनमें सूत्र संख्या २-७९ से 'र' का लोप; १-१८७ से 'घ' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; २-१७१ से स्व-अर्थ में वैकल्पिक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org