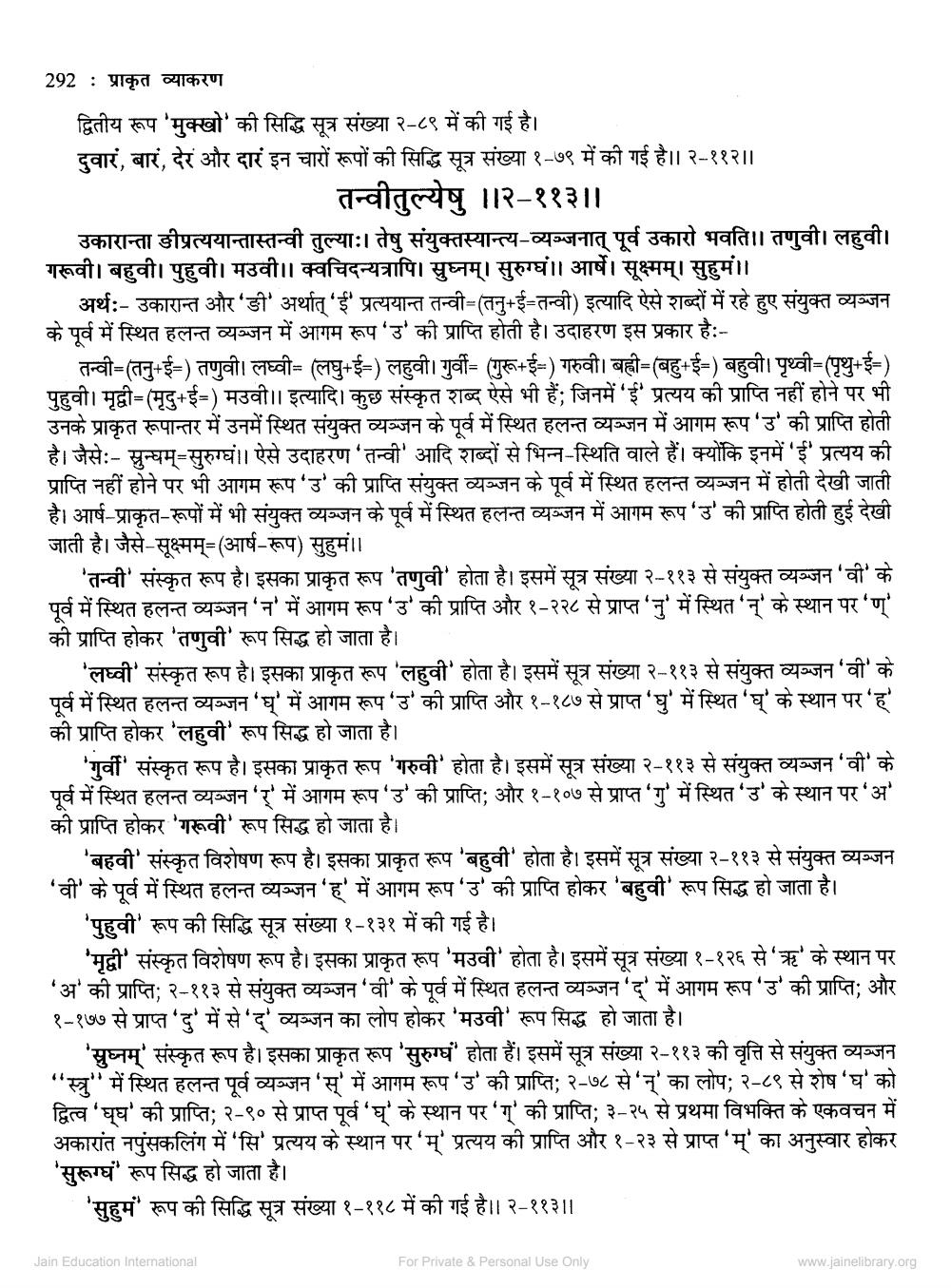________________
292 : प्राकृत व्याकरण
द्वितीय रूप 'मुक्खो ' की सिद्धि सूत्र संख्या २-८९ में की गई है। दुवारं, बारं, देर और दारं इन चारों रूपों की सिद्धि सूत्र संख्या १-७९ में की गई है।। २-११२।।
तन्वीतुल्येषु ॥२-११३।। उकारान्ता ङीप्रत्ययान्तास्तन्वी तुल्याः। तेषु संयुक्तस्यान्त्य-व्यञ्जनात् पूर्व उकारो भवति।। तणुवी। लहुवी। गरूवी। बहुवी। पुहुवी। मउवी।। क्वचिदन्यत्रापि। सुघ्नम्। सुरुग्घं।। आर्षे। सूक्ष्मम्। सुहुम।।
अर्थः- उकारान्त और 'डी' अर्थात् 'ई' प्रत्ययान्त तन्वी (तनु+ई-तन्वी) इत्यादि ऐसे शब्दों में रहे हुए संयुक्त व्यञ्जन के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति होती है। उदाहरण इस प्रकार है:___ तन्वी=(तनु-ई-) तणुवी। लघ्वी= (लघु+ई=) लहुवी। गुर्वी= (गुरू+ई-) गरुवी। बह्वी=(बहु-ई=) बहुवी। पृथ्वी-(पृथु-ई-) पुहुवी। मृद्वी= (मृदु+ई-) मउवी।। इत्यादि। कुछ संस्कृत शब्द ऐसे भी हैं; जिनमें 'ई' प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होने पर भी उनके प्राकृत रूपान्तर में उनमें स्थित संयुक्त व्यञ्जन के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति होती है। जैसे:- सुन्धम् सुरुग्घ।। ऐसे उदाहरण 'तन्वी' आदि शब्दों से भिन्न-स्थिति वाले हैं। क्योंकि इनमें 'ई' प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होने पर भी आगम रूप 'उ' की प्राप्ति संयुक्त व्यञ्जन के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन में होती देखी जाती है। आर्ष-प्राकृत-रूपों में भी संयुक्त व्यञ्जन के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। जैसे-सूक्ष्मम् (आर्ष-रूप) सुहुम।।
'तन्वी' संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'तणुवी' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-११३ से संयुक्त व्यञ्जन 'वी' के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन 'न' में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति और १-२२८ से प्राप्त 'नु' में स्थित 'न्' के स्थान पर 'ण' की प्राप्ति होकर 'तणुवी रूप सिद्ध हो जाता है।
'लघ्वी' संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'लहुवी' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-११३ से संयुक्त व्यञ्जन 'वी' के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन 'घ' में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति और १-१८७ से प्राप्त 'घु' में स्थित 'घ्' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति होकर 'लहुवी रूप सिद्ध हो जाता है।
'गुर्वी' संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'गरुवी होता है। इसमें सूत्र संख्या २-११३ से संयुक्त व्यञ्जन 'वी' के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन 'र' में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति; और १-१०७ से प्राप्त 'गु' में स्थित 'उ' के स्थान पर 'अ' की प्राप्ति होकर 'गरूवी रूप सिद्ध हो जाता है। __'बहवी' संस्कृत विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप 'बहुवी' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-११३ से संयुक्त व्यञ्जन 'वी' के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन 'ह' में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति होकर 'बहुवी रूप सिद्ध हो जाता है।
'पुहुवी' रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-१३१ में की गई है।
'मृद्वी' संस्कृत विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप 'मउवी' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१२६ से 'ऋ' के स्थान पर 'अ' की प्राप्ति; २-११३ से संयुक्त व्यञ्जन 'वी' के पूर्व में स्थित हलन्त व्यञ्जन 'द्' में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति; और १-१७७ से प्राप्त 'दु' में से 'द्' व्यञ्जन का लोप होकर 'मउवी' रूप सिद्ध हो जाता है।
'स्रुघ्नम् संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'सुरुग्घं होता हैं। इसमें सूत्र संख्या २-११३ की वृत्ति से संयुक्त व्यञ्जन "स्त्रु" में स्थित हलन्त पूर्व व्यञ्जन 'स्' में आगम रूप 'उ' की प्राप्ति; २-७८ से 'न्' का लोप; २-८९ से शेष 'घ' को द्वित्व 'घ' की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व 'घ' के स्थान पर 'ग्' की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारांत नपुंसकलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर 'सुरूग्घं रूप सिद्ध हो जाता है।
'सुहुमं रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-११८ में की गई है।। २-११३।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org