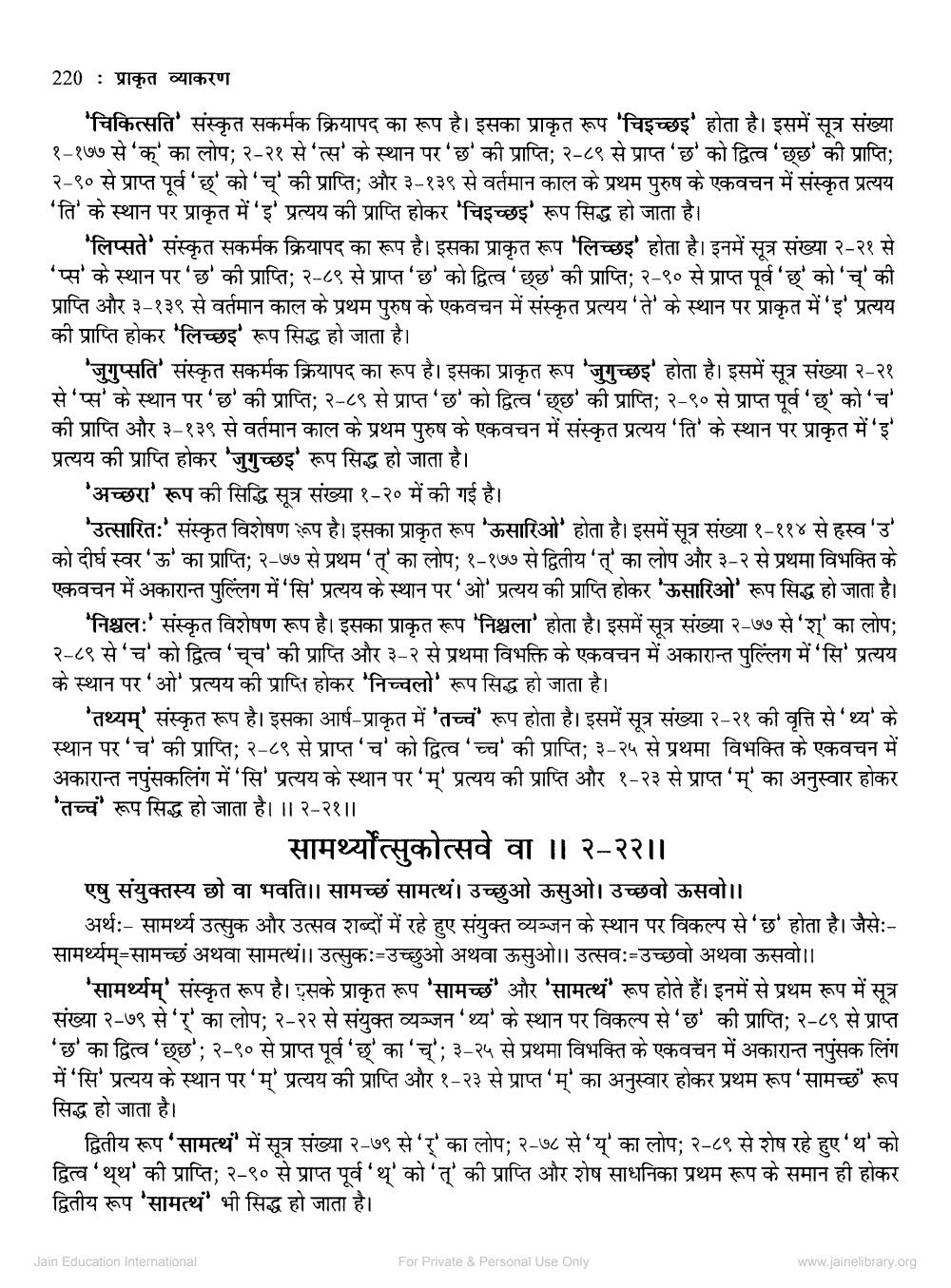________________
220 : प्राकृत व्याकरण ___"चिकित्सति' संस्कृत सकर्मक क्रियापद का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'चिइच्छइ' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-१७७ से 'क्' का लोप; २-२१ से 'त्स' के स्थान पर 'छ' की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त 'छ' को द्वित्व 'छ्छ' की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व 'छ्' को 'च' की प्राप्ति; और ३-१३९ से वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'चिइच्छइ' रूप सिद्ध हो जाता है।
"लिप्सते' संस्कृत सकर्मक क्रियापद का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'लिच्छई' होता है। इनमें सूत्र संख्या २-२१ से 'प्स' के स्थान पर 'छ' की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त 'छ' को द्वित्व'छ्छ' की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व 'छ्' को 'च' की प्राप्ति और ३-१३९ से वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'ते' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'लिच्छइ' रूप सिद्ध हो जाता है।। ___ 'जुगुप्सति' संस्कृत सकर्मक क्रियापद का रूप है। इसका प्राकृत रूप 'जुगुच्छई' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-२१ से 'प्स' के स्थान पर 'छ' की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त 'छ' को द्वित्व 'छ्छ' की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व 'छ्' को 'च' की प्राप्ति और ३–१३९ से वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एकवचन में संस्कृत प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत में 'इ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'जुगुच्छइ' रूप सिद्ध हो जाता है।
'अच्छरा' रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १-२० में की गई है।
'उत्सारितः संस्कृत विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप 'ऊसारिओ' होता है। इसमें सूत्र संख्या १-११४ से हस्व'उ' को दीर्घ स्वर 'ऊ' का प्राप्ति; २-७७ से प्रथम 'त्' का लोप; १-१७७ से द्वितीय 'त्' का लोप और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'ऊसारिओ' रूप सिद्ध हो जाता है।
"निश्चलः' संस्कृत विशेषण रूप है। इसका प्राकृत रूप 'निश्चला' होता है। इसमें सूत्र संख्या २-७७ से 'श्' का लोप; २-८९ से 'च' को द्वित्व 'च्च' की प्राप्ति और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'निच्चलो' रूप सिद्ध हो जाता है।
'तथ्यम्' संस्कृत रूप है। इसका आर्ष-प्राकृत में 'तच्च रूप होता है। इसमें सूत्र संख्या २-२१ की वृत्ति से 'थ्य के स्थान पर 'च' की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त 'च' को द्वित्व 'च्च' की प्राप्ति; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त नपुंसकलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर 'तच्चं रूप सिद्ध हो जाता है। ।। २-२१ ।।
सामर्थ्योत्सकोत्सवे वा ॥ २-२२।। एषु संयुक्तस्य छो वा भवति।। सामच्छं सामत्थं। उच्छुओ ऊसुओ। उच्छवो ऊसवो।
अर्थः- सामर्थ्य उत्सुक और उत्सव शब्दों में रहे हुए संयुक्त व्यञ्जन के स्थान पर विकल्प से 'छ' होता है। जैसे:सामर्थ्यम्=सामच्छं अथवा सामत्थ।। उत्सुकः-उच्छुओ अथवा ऊसुओ।। उत्सवः-उच्छवो अथवा ऊसवो।। _ 'सामर्थ्यम्' संस्कृत रूप है। इसके प्राकृत रूप 'सामच्छ' और 'सामत्थं रूप होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र संख्या २-७९ से 'र' का लोप; २-२२ से संयुक्त व्यञ्जन 'थ्य' के स्थान पर विकल्प से 'छ' की प्राप्ति; २-८९ से प्राप्त 'छ' का द्वित्व'छ्छ'; २-९० से प्राप्त पूर्व 'छ्' का 'च'; ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त नपुंसक लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १-२३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर प्रथम रूप 'सामच्छ' रूप सिद्ध हो जाता है।
द्वितीय रूप 'सामत्थं' में सूत्र संख्या २-७९ से 'र' का लोप; २-७८ से 'य' का लोप; २-८९ से शेष रहे हुए 'थ' को द्वित्व'थ्थ' की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व 'थ्' को 'त्' की प्राप्ति और शेष साधनिका प्रथम रूप के समान ही होकर द्वितीय रूप 'सामत्थं भी सिद्ध हो जाता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org