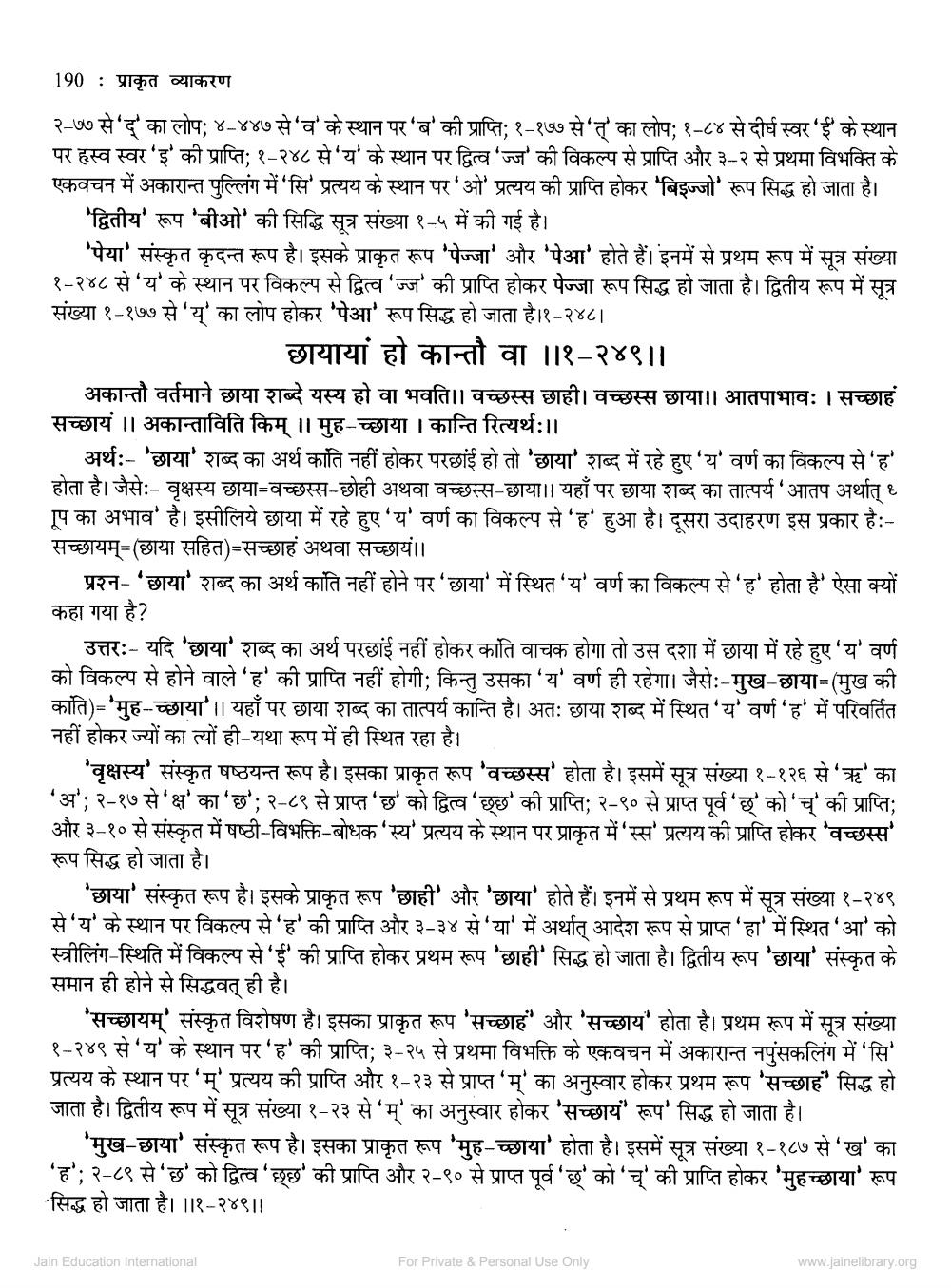________________
190 : प्राकृत व्याकरण
२-७७ से 'द्' का लोप; ४-४४७ से 'व' के स्थान पर 'ब' की प्राप्ति; १ - १७७ से 'त्' का लोप; १-८४ से दीर्घ स्वर 'ई' के स्थान पर हस्व स्वर 'इ' की प्राप्ति; १ - २४८ से 'य' के स्थान पर द्वित्व 'ज्ज' की विकल्प से प्राप्ति और ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त पुल्लिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'ओ' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'बिइज्जो' रूप सिद्ध हो जाता है।
'द्वितीय' रूप 'बीओ' की सिद्धि सूत्र संख्या १-५ में की गई है।
'पेया' संस्कृत कृदन्त रूप है। इसके प्राकृत रूप 'पेज्जा' और 'पेआ' होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र संख्या १ - २४८ से 'य' के स्थान पर विकल्प से द्वित्व 'ज्ज' की प्राप्ति होकर पेज्जा रूप सिद्ध हो जाता है। द्वितीय रूप में सूत्र संख्या १-१७७ से 'य्' का लोप होकर 'पेआ' रूप सिद्ध हो जाता है। १ - २४८ ।
छायायां हो कान्तौ वा ।।१-२४९।।
अकान्तौ वर्तमाने छाया शब्दे यस्य हो वा भवति ।। वच्छस्स छाही । वच्छस्स छाया ।। आतपाभावः । सच्छाहं सच्छायं । अकान्ताविति किम् ॥ मुह-च्छाया । कान्ति रित्यर्थः ।।
अर्थः- 'छाया' शब्द का अर्थ कांति नहीं होकर परछाई हो तो 'छाया' शब्द में रहे हुए 'य' वर्ण का विकल्प से 'ह' होता है। जैसे :- वृक्षस्य छाया=वच्छस्स छोही अथवा वच्छस्स छाया ।। यहाँ पर छाया शब्द का तात्पर्य 'आतप अर्थात् तूप का अभाव' है। इसीलिये छाया में रहे हुए 'य' वर्ण का विकल्प से 'ह' हुआ है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है:सच्छायम् = (छाया सहित ) = सच्छाहं अथवा सच्छायं ।।
प्रश्न- 'छाया' शब्द का अर्थ कांति नहीं होने पर 'छाया' में स्थित 'य' वर्ण का विकल्प से 'ह' होता है' ऐसा क्यों कहा गया है?
उत्तरः- यदि 'छाया' शब्द का अर्थ परछाई नहीं होकर कांति वाचक होगा तो उस दशा में छाया में रहे हुए 'य' वर्ण को विकल्प से होने वाले 'ह' की प्राप्ति नहीं होगी; किन्तु उसका 'य' वर्ण ही रहेगा। जैसे:- मुख - छाया = (मुख की कांति)='मुह--च्छाया'।। यहाँ पर छाया शब्द का तात्पर्य कान्ति है। अतः छाया शब्द में स्थित 'य' वर्ण 'ह' में परिवर्तित नहीं होकर ज्यों का त्यों ही यथा रूप में ही स्थित रहा है।
'वृक्षस्य' संस्कृत षष्ठयन्त रूप है। इसका प्राकृत रूप 'वच्छस्स' होता है। इसमें सूत्र संख्या १ - १२६ से 'ऋ' का 'अ'; २ - १७ से 'क्ष' का 'छ' ; २-८९ से प्राप्त 'छ' को द्वित्व 'छ्छ' की प्राप्ति; २-९० से प्राप्त पूर्व 'छ्' को 'च्' की प्राप्ति; और ३-१० से संस्कृत में षष्ठी विभक्ति-बोधक 'स्य' प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में 'स्स' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'वच्छस्स' रूप सिद्ध हो जाता है।
'छाया' संस्कृत रूप है। इसके प्राकृत रूप 'छाही' और 'छाया' होते हैं। इनमें से प्रथम रूप में सूत्र संख्या १ - २४९ से 'य' के स्थान पर विकल्प से 'ह' की प्राप्ति और ३ - ३४ से 'या' में अर्थात् आदेश रूप से प्राप्त 'हा' में स्थित 'आ' को स्त्रीलिंग-स्थिति में विकल्प से 'ई' की प्राप्ति होकर प्रथम रूप 'छाही' सिद्ध हो जाता है। द्वितीय रूप 'छाया' संस्कृत के समान ही होने से सिद्धवत् ही है।
'सच्छायम्' संस्कृत विशेषण है। इसका प्राकृत रूप 'सच्छाह' और 'सच्छाय' होता है। प्रथम रूप में सूत्र संख्या १ - २४९ से 'य' के स्थान पर 'ह' की प्राप्ति; ३ - २५ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अकारान्त नपुंसकलिंग में 'सि' प्रत्यय के स्थान पर 'म्' प्रत्यय की प्राप्ति और १ - २३ से प्राप्त 'म्' का अनुस्वार होकर प्रथम रूप 'सच्छाह' सिद्ध हो जाता है। द्वितीय रूप में सूत्र संख्या १ - २३ से 'म्' का अनुस्वार होकर 'सच्छायं रूप' सिद्ध हो जाता है।
'मुख - छाया' संस्कृत रूप है। इसका प्राकृत रूप 'मुह - च्छाया' होता है। इसमें सूत्र संख्या १ - १८७ से 'ख' का 'ह'; २-८९ से 'छ' को द्वित्व 'छ्छ' की प्राप्ति और २ - ९० से प्राप्त पूर्व 'छ्' को 'च्' की प्राप्ति होकर 'मुहच्छाया' रूप - सिद्ध हो जाता है। ।।१-२४९।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org