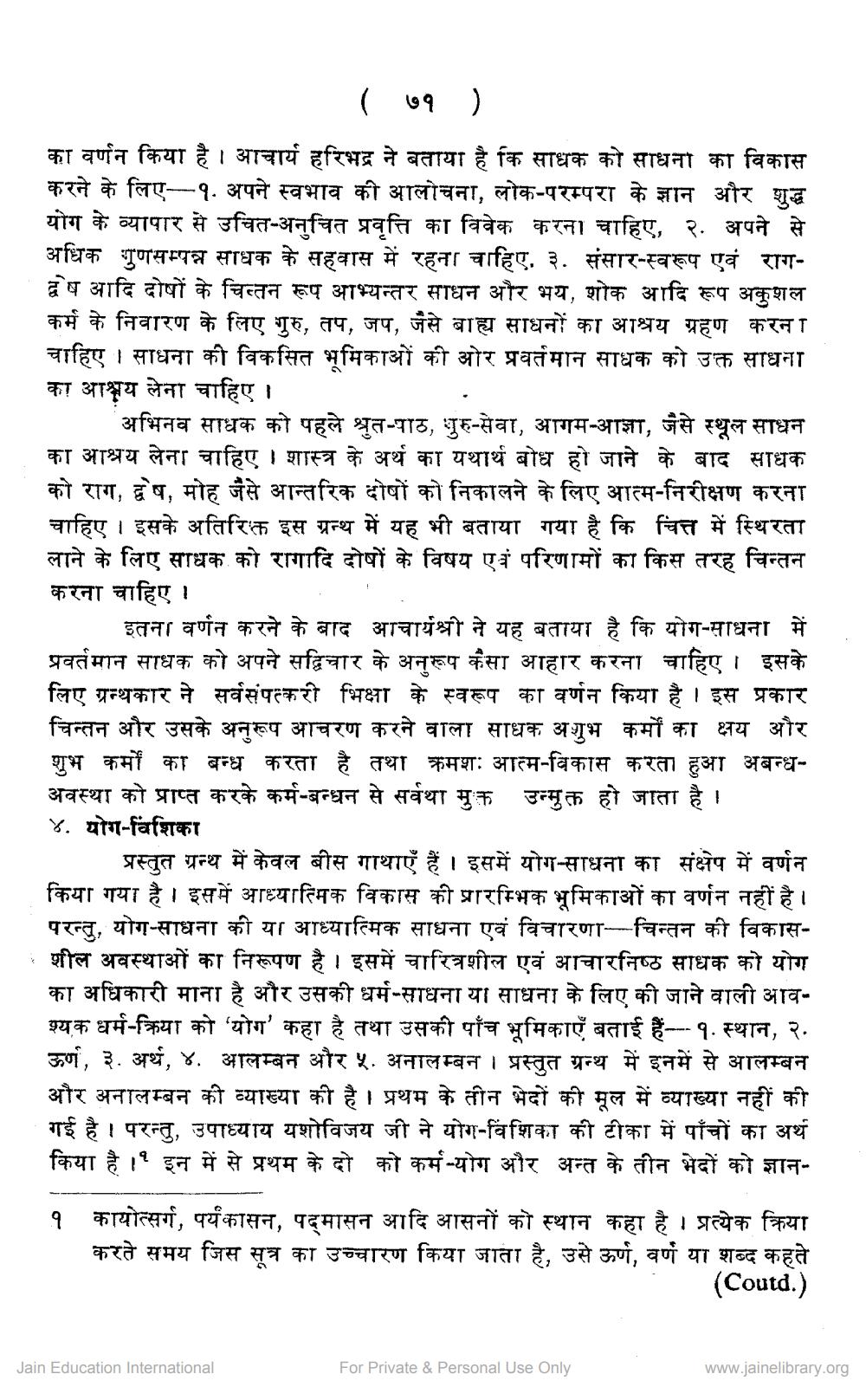________________
(
७१ )
का वर्णन किया है । आचार्य हरिभद्र ने बताया है कि साधक को साधना का विकास करने के लिए - १. अपने स्वभाव की आलोचना, लोक-परम्परा के ज्ञान और शुद्ध योग के व्यापार से उचित-अनुचित प्रवृत्ति का विवेक करना चाहिए, २. अपने से अधिक गुणसम्पन्न साधक के सहवास में रहना चाहिए. ३. संसार - स्वरूप एवं रागद्वेष आदि दोषों के चिन्तन रूप आभ्यन्तर साधन और भय, शोक आदि रूप अकुशल कर्म के निवारण के लिए गुरु, तप, जप, जैसे बाह्य साधनों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए | साधना की विकसित भूमिकाओं की ओर प्रवर्तमान साधक को उक्त साधना का आश्रय लेना चाहिए ।
● अभिनव साधक को पहले श्रुत-पाठ, गुरु-सेवा, आगम-आज्ञा, जैसे स्थूल साधन का आश्रय लेना चाहिए । शास्त्र के अर्थ का यथार्थ बोध हो जाने के बाद साधक को राग, द्वेष, मोह जैसे आन्तरिक दोषों को निकालने के लिए आत्म-निरीक्षण करना चाहिए | इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में यह भी बताया गया है कि चित्त में स्थिरता लाने के लिए साधक को रागादि दोषों के विषय एवं परिणामों का किस तरह चिन्तन करना चाहिए ।
इतना वर्णन करने के बाद आचार्यश्री ने यह बताया है कि योग-साधना में प्रवर्तमान साधक को अपने सद्विचार के अनुरूप कैसा आहार करना चाहिए । इसके लिए ग्रन्थकार ने सर्वसंपत्करी भिक्षा के स्वरूप का वर्णन किया है । इस प्रकार चिन्तन और उसके अनुरूप आचरण करने वाला साधक अशुभ कर्मों का क्षय और शुभ कर्मों का बन्ध करता है तथा क्रमशः आत्म-विकास करता हुआ अबन्धअवस्था को प्राप्त करके कर्म - बन्धन से सर्वथा मुक्त उन्मुक्त हो जाता है । ४. योग-विंशिका
प्रस्तुत ग्रन्थ में केवल बीस गाथाएँ हैं । इसमें योग-साधना का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसमें आध्यात्मिक विकास की प्रारम्भिक भूमिकाओं का वर्णन नहीं है । परन्तु, योग-साधना की या आध्यात्मिक साधना एवं विचारणा - चिन्तन की विकासशील अवस्थाओं का निरूपण है । इसमें चारित्रशील एवं आचारनिष्ठ साधक को योग ET अधिकारी माना है और उसकी धर्म-साधना या साधना के लिए की जाने वाली आवश्यक धर्म -क्रिया को 'योग' कहा है तथा उसकी पाँच भूमिकाएँ बताई हैं --- १. स्थान, २. ऊर्ण, ३. अर्थ, ४. आलम्बन और ५. अनालम्बन । प्रस्तुत ग्रन्थ में इनमें से आलम्बन और अनालम्बन की व्याख्या की है । प्रथम के तीन भेदों की मूल में व्याख्या नहीं की गई है । परन्तु, उपाध्याय यशोविजय जी ने योग-विंशिका की टीका में पाँचों का अर्थ किया है। इन में से प्रथम के दो को कर्म-योग और अन्त के तीन भेदों को ज्ञान
१ कायोत्सर्ग, पर्यंकासन, पद्मासन आदि आसनों को स्थान कहा है । प्रत्येक क्रिया करते समय जिस सूत्र का उच्चारण किया जाता है, उसे ऊर्ण, वर्ण या शब्द कहते
( Coutd.)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org