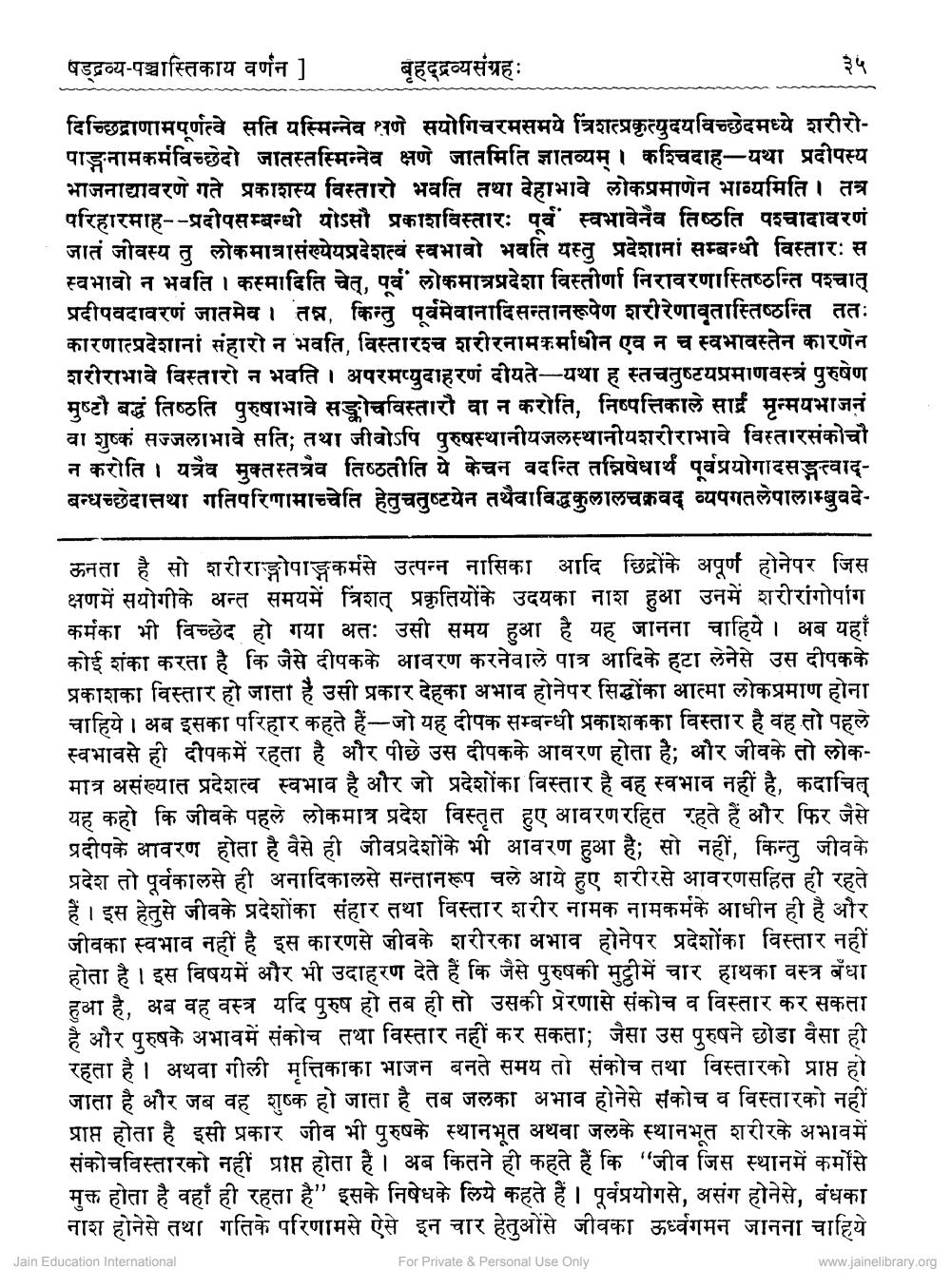________________
षड्द्रव्य-पञ्चास्तिकाय वर्णन ]
बृहद्रव्यसंग्रहः
३५
दिच्छिद्राणामपूर्णत्वे सति यस्मिन्नेव क्षणे सयोगिचरमसमये त्रिंशत्प्रकृत्युदयविच्छेदमध्ये शरीरोपाङ्गनामकर्मविच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव क्षणे जातमिति ज्ञातव्यम् । कश्चिदाह-यथा प्रदीपस्य भाजनाद्यावरणे गते प्रकाशस्य विस्तारो भवति तथा देहाभावे लोकप्रमाणेन भाव्यमिति । तत्र परिहारमाह--प्रदीपसम्बन्धी योऽसौ प्रकाशविस्तारः पूर्व स्वभावेनैव तिष्ठति पश्चादावरणं जातं जीवस्य तु लोकमात्रासंख्येयप्रदेशत्वं स्वभावो भवति यस्तु प्रदेशानां सम्बन्धी विस्तारः स स्वभावो न भवति । कस्मादिति चेत्, पूर्व लोकमात्रप्रदेशा विस्तीर्णा निरावरणास्तिष्ठन्ति पश्चात् प्रदीपवदावरणं जातमेव । तन्न, किन्तु पूर्वमेवानादिसन्तानरूपेण शरीरेणावृतास्तिष्ठन्ति ततः कारणात्प्रदेशानां संहारो न भवति, विस्तारश्च शरीरनामकर्माधीन एव न च स्वभावस्तेन कारणेन शरीराभावे विस्तारो न भवति । अपरमप्युदाहरणं दीयते-यथा ह स्तचतुष्टयप्रमाणवस्त्रं पुरुषेण मुष्टौ बद्धं तिष्ठति पुरुषाभावे सङ्कोचविस्तारौ वा न करोति, निष्पत्तिकाले साई मृन्मयभाजनं वा शुष्कं सज्जलाभावे सति; तथा जीवोऽपि पुरुषस्थानीयजलस्थानीयशरीराभावे विस्तारसंकोचौ न करोति । यत्रैव मुक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति ये केचन वदन्ति तनिषेधार्थ पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्बन्धच्छेदात्तथा गतिपरिणामाच्चेति हेतुचतुष्टयेन तथैवाविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालाम्बुवदे
ऊनता है सो शरीराङ्गोपाङ्गकर्मसे उत्पन्न नासिका आदि छिद्रोंके अपूर्ण होनेपर जिस क्षणमें सयोगीके अन्त समयमें त्रिंशत् प्रकृतियोंके उदयका नाश हुआ उनमें शरीरांगोपांग कर्मका भी विच्छेद हो गया अतः उसी समय हुआ है यह जानना चाहिये। अब यहाँ कोई शंका करता है कि जैसे दीपकके आवरण करनेवाले पात्र आदिके हटा लेनेसे उस दीपकके प्रकाशका विस्तार हो जाता है उसी प्रकार देहका अभाव होनेपर सिद्धोंका आत्मा लोकप्रमाण होना चाहिये। अब इसका परिहार कहते हैं-जो यह दीपक सम्बन्धी प्रकाशकका विस्तार है वह तो पहले स्वभावसे ही दीपकमें रहता है और पीछे उस दीपकके आवरण होता है; और जीवके तो लोकमात्र असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है और जो प्रदेशोंका विस्तार है वह स्वभाव नहीं है, कदाचित् यह कहो कि जीवके पहले लोकमात्र प्रदेश विस्तृत हुए आवरणरहित रहते हैं और फिर जैसे प्रदीपके आवरण होता है वैसे ही जीवप्रदेशोंके भी आवरण हुआ है; सो नहीं, किन्तु जीवके प्रदेश तो पूर्वकालसे ही अनादिकालसे सन्तानरूप चले आये हुए शरीरसे आवरणसहित ही रहते हैं। इस हेतसे जीवके प्रदेशोंका संहार तथा विस्तार शरीर नामक नामकर्मके आधीन ही है और जीवका स्वभाव नहीं है इस कारणसे जीवके शरीरका अभाव होनेपर प्रदेशोंका विस्तार नहीं होता है । इस विषयमें और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे पुरुषकी मुट्ठीमें चार हाथका वस्त्र बँधा हुआ है, अब वह वस्त्र यदि पुरुष हो तब ही तो उसकी प्रेरणासे संकोच व विस्तार कर सकता है और पुरुषके अभावमें संकोच तथा विस्तार नहीं कर सकता; जैसा उस पुरुषने छोडा वैसा ही रहता है। अथवा गीली मृत्तिकाका भाजन बनते समय तो संकोच तथा विस्तारको प्राप्त हो जाता है और जब वह शुष्क हो जाता है तब जलका अभाव होनेसे संकोच व विस्तारको नहीं प्राप्त होता है इसी प्रकार जीव भी पुरुषके स्थानभूत अथवा जलके स्थानभूत शरीरके अभाव में संकोचविस्तारको नहीं प्राप्त होता है। अब कितने ही कहते हैं कि “जीव जिस स्थानमें कर्मोसे मुक्त होता है वहाँ ही रहता है" इसके निषेधके लिये कहते हैं। पूर्वप्रयोगसे, असंग होनेसे, बंधका नाश होनेसे तथा गतिके परिणामसे ऐसे इन चार हेतुओंसे जीवका ऊर्ध्वगमन जानना चाहिये
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org