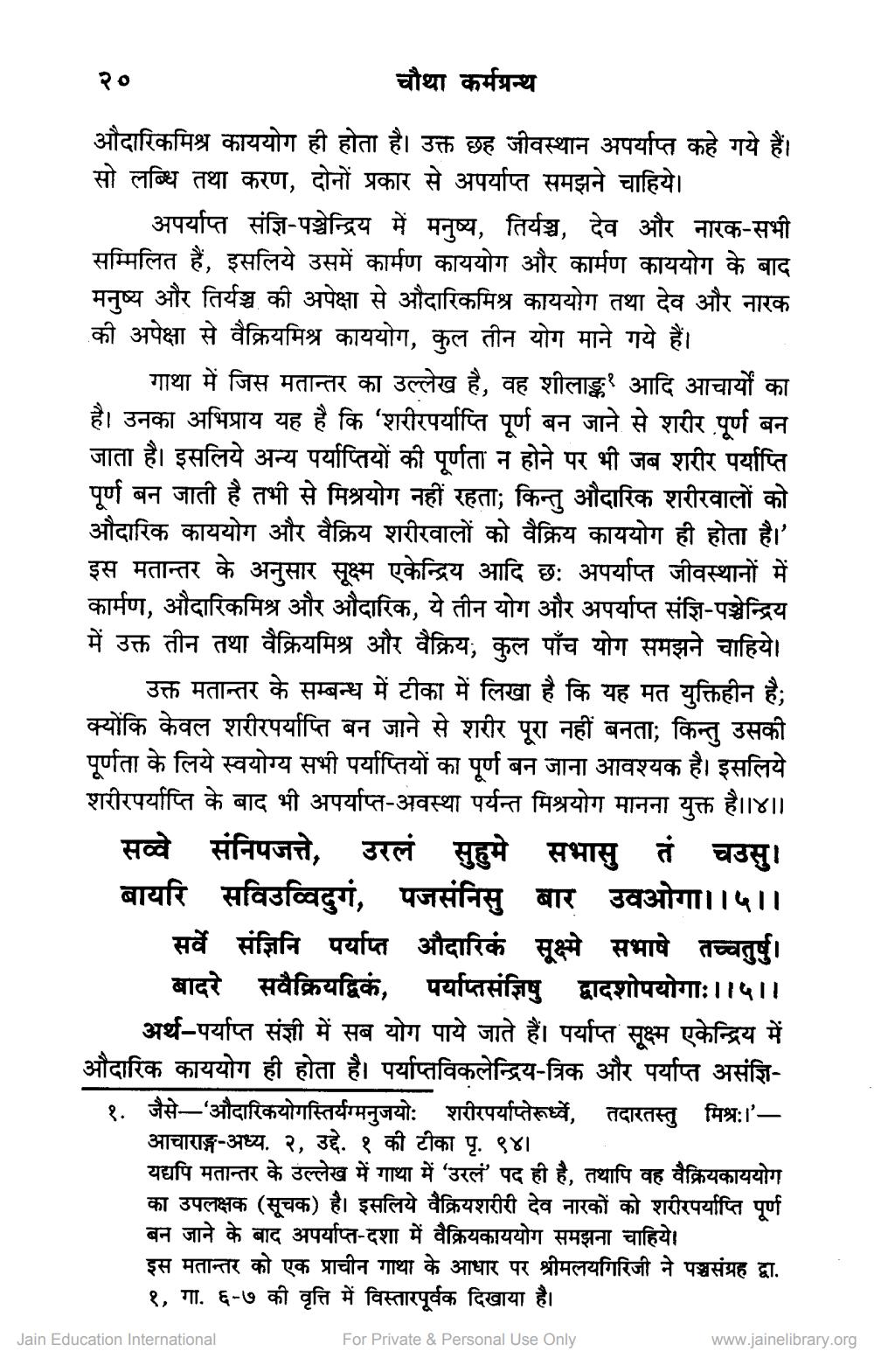________________
चौथा कर्मग्रन्थ
औदारिकमिश्र काययोग ही होता है। उक्त छह जीवस्थान अपर्याप्त कहे गये हैं। सो लब्धि तथा करण, दोनों प्रकार से अपर्याप्त समझने चाहिये ।
२०
अपर्याप्त संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय में मनुष्य, तिर्यञ्च देव और नारक - सभी सम्मिलित हैं, इसलिये उसमें कार्मण काययोग और कार्मण काययोग के बाद मनुष्य और तिर्यञ्च की अपेक्षा से औदारिकमिश्र काययोग तथा देव और नारक की अपेक्षा से वैक्रियमिश्र काययोग, कुल तीन योग माने गये हैं।
गाथा में जिस मतान्तर का उल्लेख है, वह शीलाङ्क आदि आचार्यों का है । उनका अभिप्राय यह है कि 'शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन जाने से शरीर पूर्ण बन जाता है। इसलिये अन्य पर्याप्तियों की पूर्णता न होने पर भी जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण बन जाती है तभी से मिश्रयोग नहीं रहता; किन्तु औदारिक शरीरवालों को औदारिक काययोग और वैक्रिय शरीरवालों को वैक्रिय काययोग ही होता है।' इस मतान्तर के अनुसार सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि छः अपर्याप्त जीवस्थानों में कार्मण, औदारिकमिश्र और औदारिक, ये तीन योग और अपर्याप्त संज्ञि - पञ्चेन्द्रिय में उक्त तीन तथा वैक्रियमिश्र और वैक्रिय, कुल पाँच योग समझने चाहिये ।
उक्त मतान्तर के सम्बन्ध में टीका में लिखा है कि यह मत युक्तिहीन है; क्योंकि केवल शरीरपर्याप्ति बन जाने से शरीर पूरा नहीं बनता; किन्तु उसकी पूर्णता के लिये स्वयोग्य सभी पर्याप्तियों का पूर्ण बन जाना आवश्यक है। इसलिये शरीरपर्याप्ति के बाद भी अपर्याप्त अवस्था पर्यन्त मिश्रयोग मानना युक्त है ॥ ४ ॥ सव्वे संनिपजत्ते, उरलं सुहुमे सभासु तं चउसु । बायरि सविउव्विदुगं, पजसंनिसु बार
उवओगा । । ५ । ।
सभाषे तच्चतुर्षु ।
सर्वे संज्ञिनि पर्याप्त औदारिकं सूक्ष्मे बादरे सवैक्रियद्विकं पर्याप्तसंज्ञिषु द्वादशोपयोगाः । । ५ । । अर्थ - पर्याप्त संज्ञी में सब योग पाये जाते हैं। पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय में औदारिक काययोग ही होता है। पर्याप्तविकलेन्द्रिय-त्रिक और पर्याप्त असंज्ञि
,
१. जैसे— 'औदारिकयोगस्तिर्यग्मनुजयोः शरीरपर्याप्तेरूर्ध्वे तदारतस्तु मिश्रः । ' - आचाराङ्ग-अध्य. २, उद्दे. १ की टीका पृ. ९४।
यद्यपि मतान्तर के उल्लेख में गाथा में 'उरलं' पद ही है, तथापि वह वैक्रियकाययोग का उपलक्षक (सूचक) है। इसलिये वैक्रियशरीरी देव नारकों को शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन जाने के बाद अपर्याप्त दशा में वैक्रियकाययोग समझना चाहिये । इस मतान्तर को एक प्राचीन गाथा के आधार पर श्रीमलयगिरिजी ने पञ्चसंग्रह द्वा. १, गा. ६-७ की वृत्ति में विस्तारपूर्वक दिखाया है।
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org