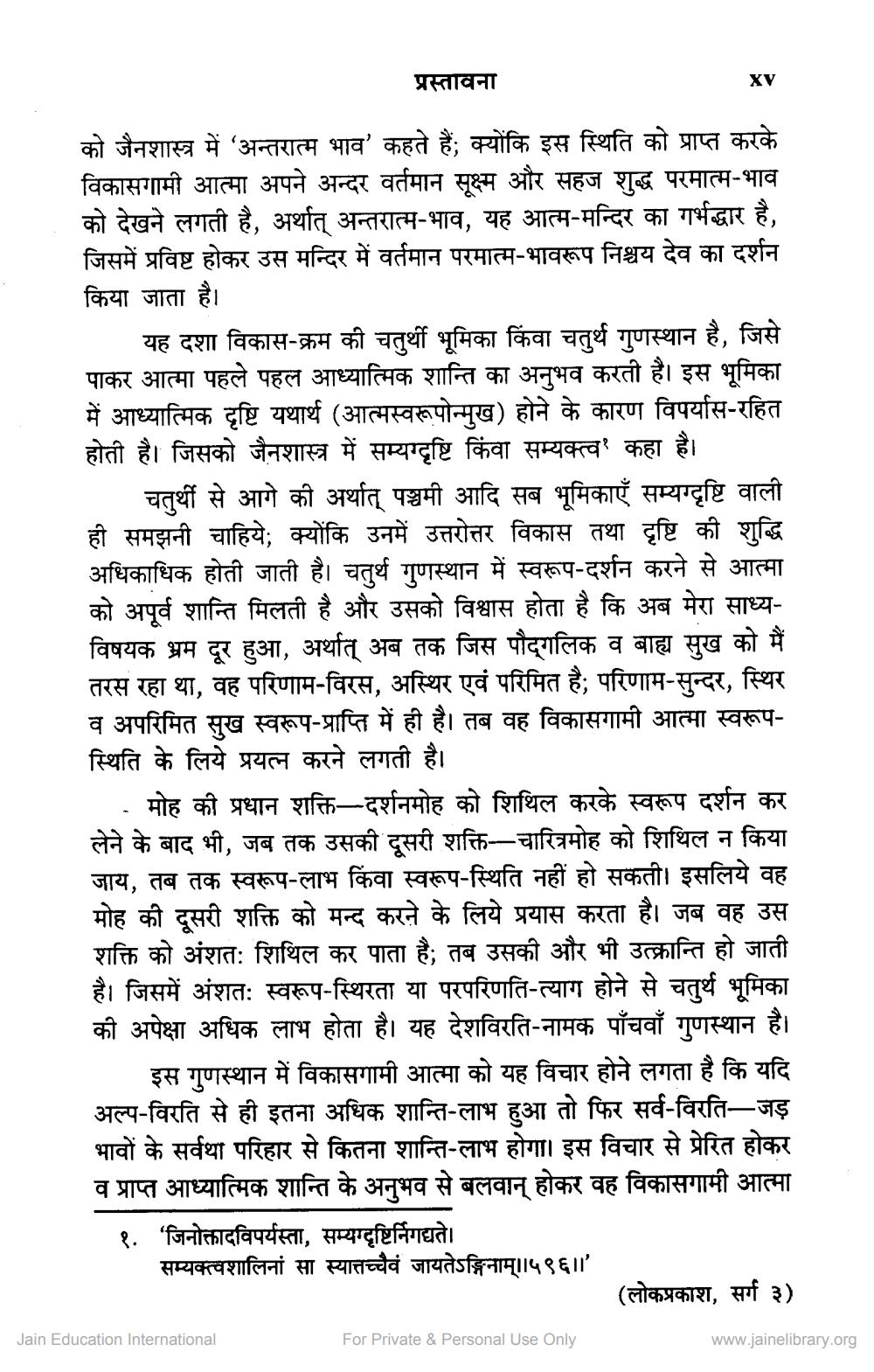________________
प्रस्तावना
को जैनशास्त्र में 'अन्तरात्म भाव' कहते हैं; क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करके विकासगामी आत्मा अपने अन्दर वर्तमान सूक्ष्म और सहज शुद्ध परमात्म-भाव को देखने लगती है, अर्थात् अन्तरात्म-भाव, यह आत्म- मन्दिर का गर्भद्धार है, जिसमें प्रविष्ट होकर उस मन्दिर में वर्तमान परमात्म-भावरूप निश्चय देव का दर्शन किया जाता है।
यह दशा विकास-क्रम की चतुर्थी भूमिका किंवा चतुर्थ गुणस्थान है, जिसे पाकर आत्मा पहले पहल आध्यात्मिक शान्ति का अनुभव करती है। इस भूमिका में आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ (आत्मस्वरूपोन्मुख ) होने के कारण विपर्यास-रहित होती है। जिसको जैनशास्त्र में सम्यग्दृष्टि किंवा सम्यक्त्व' कहा है।
चतुर्थी से आगे की अर्थात् पञ्चमी आदि सब भूमिकाएँ सम्यग्दृष्टि वाली ही समझनी चाहिये; क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास तथा दृष्टि की शुद्धि अधिकाधिक होती जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूप-दर्शन करने से आत्मा को अपूर्व शान्ति मिलती है और उसको विश्वास होता है कि अब मेरा साध्यविषयक भ्रम दूर हुआ, अर्थात् अब तक जिस पौद्गलिक व बाह्य सुख को मैं तरस रहा था, वह परिणाम - विरस, अस्थिर एवं परिमित है; परिणाम- सुन्दर, स्थिर व अपरिमित सुख स्वरूप - प्राप्ति में ही है। तब वह विकासगामी आत्मा स्वरूपस्थिति के लिये प्रयत्न करने लगती है।
XV
मोह की प्रधान शक्ति - दर्शनमोह को शिथिल करके स्वरूप दर्शन कर लेने के बाद भी, जब तक उसकी दूसरी शक्ति- चारित्रमोह को शिथिल न किया जाय, तब तक स्वरूप लाभ किंवा स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। इसलिये वह मोह की दूसरी शक्ति को मन्द करने के लिये प्रयास करता है। जब वह उस शक्ति को अंशत: शिथिल कर पाता है; तब उसकी और भी उत्क्रान्ति हो जाती है। जिसमें अंशतः स्वरूप- स्थिरता या परपरिणति त्याग होने से चतुर्थ भूमिका की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। यह देशविरति - नामक पाँचवाँ गुणस्थान है।
इस गुणस्थान में विकासगामी आत्मा को यह विचार होने लगता है कि यदि अल्प-विरति से ही इतना अधिक शान्ति-लाभ हुआ तो फिर सर्व - विरति — जड़ भावों के सर्वथा परिहार से कितना शान्ति लाभ होगा। इस विचार से प्रेरित होकर व प्राप्त आध्यात्मिक शान्ति के अनुभव से बलवान् होकर वह विकासगामी आत्मा
१. 'जिनोक्तादविपर्यस्ता, सम्यग्दृष्टिर्निगद्यते ।
सम्यक्त्वशालिनां सा स्यात्तच्चैवं जायतेऽङ्गिनाम्॥ ५९६ ॥'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
( लोकप्रकाश, सर्ग ३)
www.jainelibrary.org