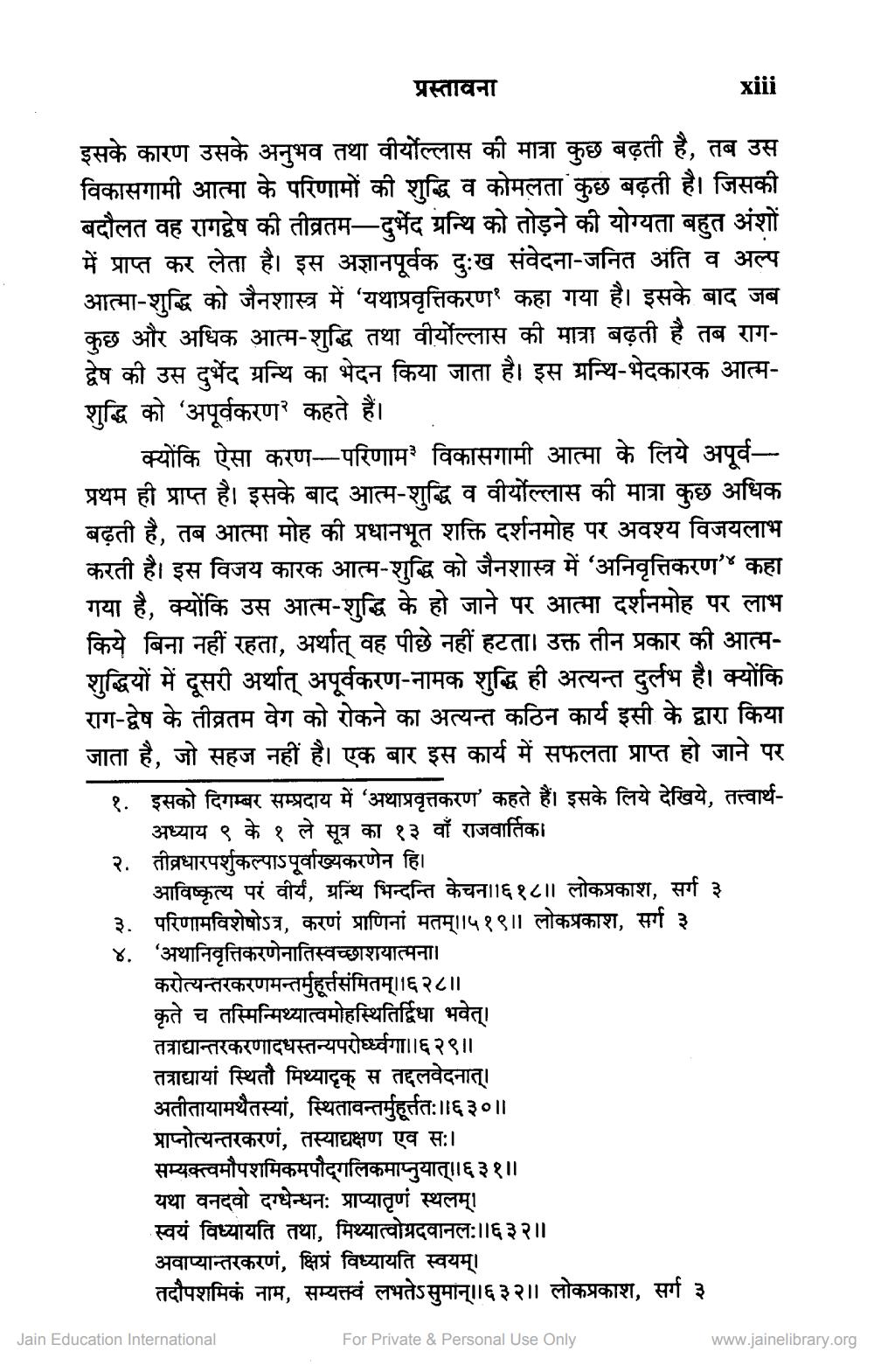________________
प्रस्तावना
इसके कारण उसके अनुभव तथा वीर्योल्लास की मात्रा कुछ बढ़ती है, तब उस विकासगामी आत्मा के परिणामों की शुद्धि व कोमलता कुछ बढ़ती है । जिसकी बदौलत वह रागद्वेष की तीव्रतम - दुर्भेद ग्रन्थि को तोड़ने की योग्यता बहुत अंशों में प्राप्त कर लेता है। इस अज्ञानपूर्वक दुःख संवेदना - जनित अंति व अल्प आत्मा शुद्धि को जैनशास्त्र में 'यथाप्रवृत्तिकरण' कहा गया है। इसके बाद जब कुछ और अधिक आत्म-शुद्धि तथा वीर्योल्लास की मात्रा बढ़ती है तब रागद्वेष की उस दुर्भेद ग्रन्थि का भेदन किया जाता है। इस ग्रन्थि-भेदकारक आत्मशुद्धि को 'अपूर्वकरण' कहते हैं।
xiii
क्योंकि ऐसा करण - परिणाम विकासगामी आत्मा के लिये अपूर्वप्रथम ही प्राप्त है। इसके बाद आत्म शुद्धि व वीर्योल्लास की मात्रा कुछ अधिक बढ़ती है, तब आत्मा मोह की प्रधानभूत शक्ति दर्शनमोह पर अवश्य विजयलाभ करती है। इस विजय कारक आत्म शुद्धि को जैनशास्त्र में 'अनिवृत्तिकरण' कहा गया है, क्योंकि उस आत्म शुद्धि के हो जाने पर आत्मा दर्शनमोह पर लाभ किये बिना नहीं रहता, अर्थात् वह पीछे नहीं हटता । उक्त तीन प्रकार की आत्मशुद्धियों में दूसरी अर्थात् अपूर्वकरण-नामक शुद्धि ही अत्यन्त दुर्लभ है। क्योंकि राग-द्वेष के तीव्रतम वेग को रोकने का अत्यन्त कठिन कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, जो सहज नहीं है। एक बार इस कार्य में सफलता प्राप्त हो जाने पर
Jain Education International
१. इसको दिगम्बर सम्प्रदाय में 'अथाप्रवृत्तकरण' कहते हैं। इसके लिये देखिये, तत्त्वार्थअध्याय ९ के १ ले सूत्र का १३ वाँ राजवार्तिक ।
२. तीव्रधारपर्शुकल्पाऽपूर्वाख्यकरणेन हि ।
आविष्कृत्य परं वीर्य, ग्रन्थि भिन्दन्ति केचन ।। ६१८ ॥ लोकप्रकाश, सर्ग ३ ३. परिणामविशेषोऽत्र, करणं प्राणिनां मतम् ॥ ५१९ || लोकप्रकाश, सर्ग ३ ४. 'अथानिवृत्तिकरणेनातिस्वच्छाशयात्मना।
करोत्यन्तरकरणमन्तर्मुहूर्तसंमितम्॥६२८ ॥ कृते च तस्मिन्मिथ्यात्वमोहस्थितिर्द्विधा भवेत्। तत्राद्यान्तरकरणादधस्तन्यपरोर्ध्वगा॥ ६२९ ॥ तत्राद्यायां स्थितौ मिथ्यादृक् स तद्दलवेदनात् । अतीतायामथैतस्यां स्थितावन्तर्मुहूर्ततः॥६३०॥ प्राप्नोत्यन्तरकरणं, तस्याद्यक्षण एव सः । सम्यक्त्वमौपशमिकमपौद्गलिकमाप्नुयात्॥ ६३१॥ यथा वनदवो दग्धेन्धनः प्राप्यातृणं स्थलम् । स्वयं विध्यायति तथा, मिथ्यात्वोग्रदवानलः ॥६३२॥ अवाप्यान्तरकरणं, क्षिप्रं विध्यायति स्वयम् । तदौपशमिकं नाम,
सम्यक्त्तत्वं लभतेऽसुमान्॥ ६३२ || लोकप्रकाश, सर्ग ३
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org