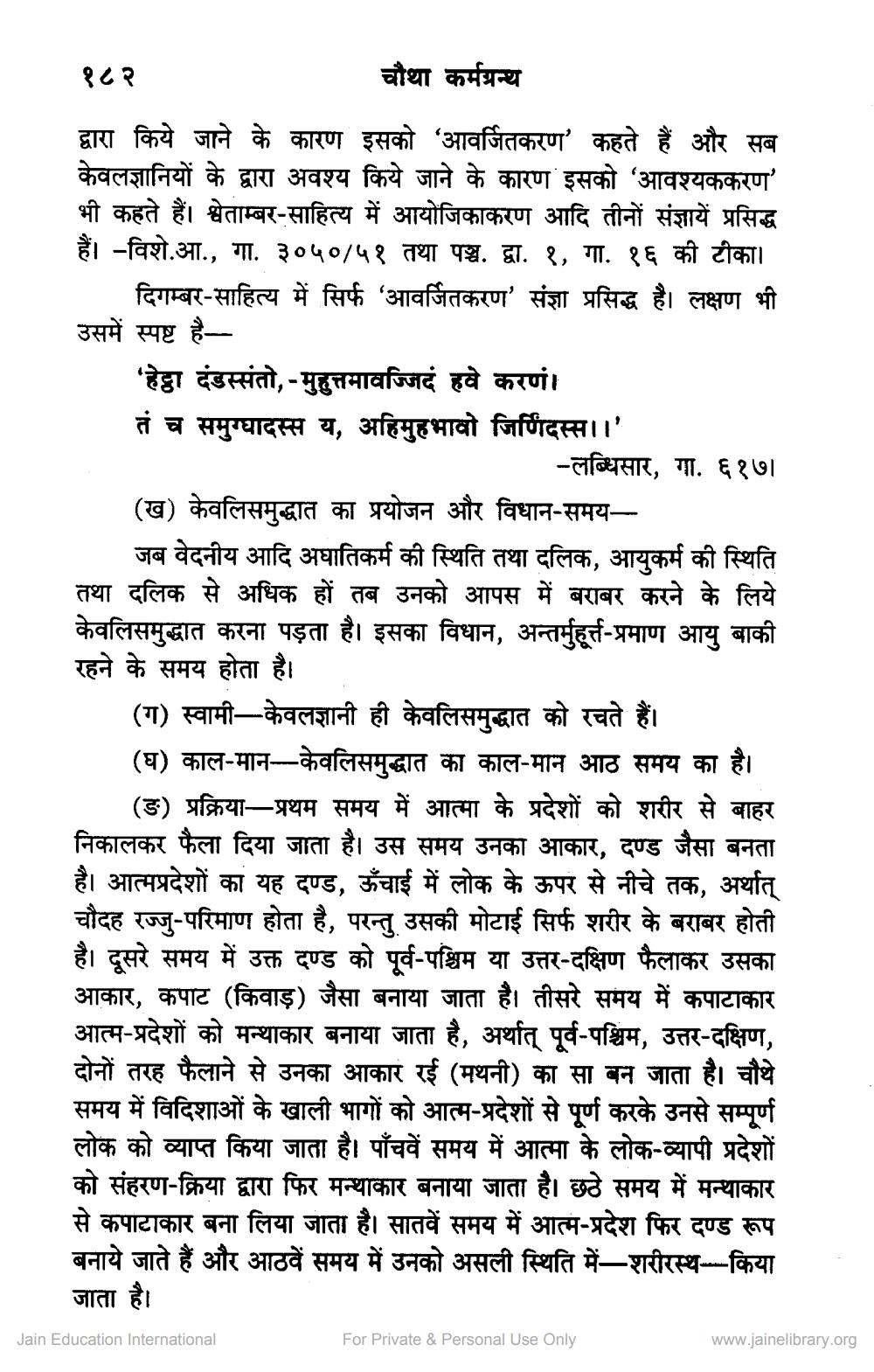________________
१८२
चौथा कर्मग्रन्थ द्वारा किये जाने के कारण इसको 'आवर्जितकरण' कहते हैं और सब केवलज्ञानियों के द्वारा अवश्य किये जाने के कारण इसको 'आवश्यककरण' भी कहते हैं। श्वेताम्बर-साहित्य में आयोजिकाकरण आदि तीनों संज्ञायें प्रसिद्ध हैं। -विशे.आ., गा. ३०५०/५१ तथा पञ्च. द्वा. १, गा. १६ की टीका।
दिगम्बर-साहित्य में सिर्फ 'आवर्जितकरण' संज्ञा प्रसिद्ध है। लक्षण भी उसमें स्पष्ट है
'हेट्ठा दंडस्संतो,- मुहुत्तमावज्जिदं हवे करणं। तं च समुग्धादस्स य, अहिमुहभावो जिणिदस्स।।'
-लब्धिसार, गा. ६१७। (ख) केवलिसमुद्धात का प्रयोजन और विधान-समय
जब वेदनीय आदि अघातिकर्म की स्थिति तथा दलिक, आयुकर्म की स्थिति तथा दलिक से अधिक हों तब उनको आपस में बराबर करने के लिये केवलिसमुद्धात करना पड़ता है। इसका विधान, अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण आयु बाकी रहने के समय होता है।
(ग) स्वामी–केवलज्ञानी ही केवलिसमुद्धात को रचते हैं। (घ) काल-मान-केवलिसमुद्धात का काल-मान आठ समय का है।
(ङ) प्रक्रिया-प्रथम समय में आत्मा के प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालकर फैला दिया जाता है। उस समय उनका आकार, दण्ड जैसा बनता है। आत्मप्रदेशों का यह दण्ड, ऊँचाई में लोक के ऊपर से नीचे तक, अर्थात् चौदह रज्जु-परिमाण होता है, परन्तु उसकी मोटाई सिर्फ शरीर के बराबर होती है। दूसरे समय में उक्त दण्ड को पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण फैलाकर उसका आकार, कपाट (किवाड़) जैसा बनाया जाता है। तीसरे समय में कपाटाकार आत्म-प्रदेशों को मन्थाकार बनाया जाता है, अर्थात् पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, दोनों तरह फैलाने से उनका आकार रई (मथनी) का सा बन जाता है। चौथे समय में विदिशाओं के खाली भागों को आत्म-प्रदेशों से पूर्ण करके उनसे सम्पूर्ण लोक को व्याप्त किया जाता है। पाँचवें समय में आत्मा के लोक-व्यापी प्रदेशों को संहरण-क्रिया द्वारा फिर मन्थाकार बनाया जाता है। छठे समय में मन्थाकार से कपाटाकार बना लिया जाता है। सातवें समय में आत्म-प्रदेश फिर दण्ड रूप बनाये जाते हैं और आठवें समय में उनको असली स्थिति में शरीरस्थ-किया जाता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org