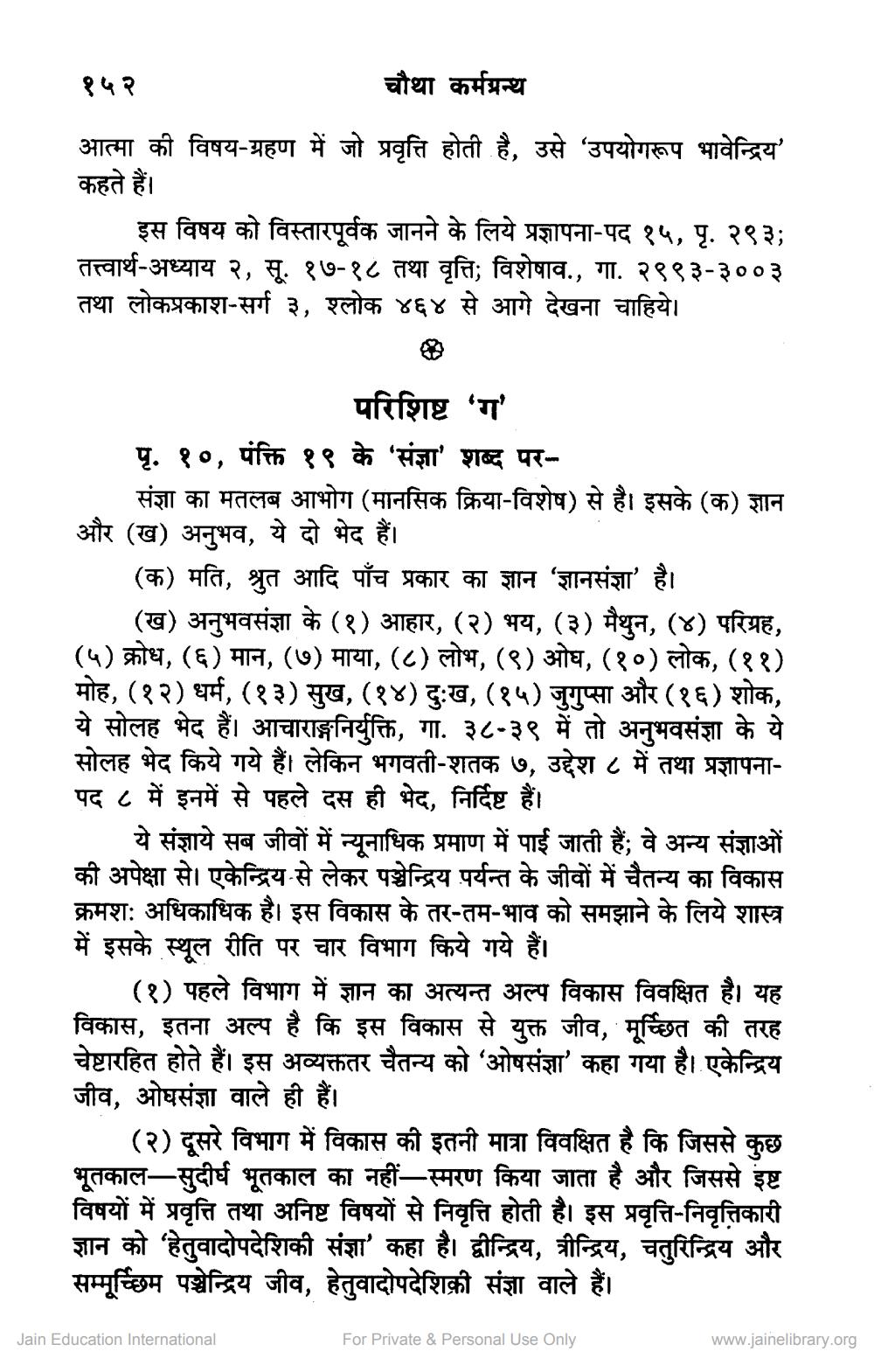________________
१५२
चौथा कर्मग्रन्थ
आत्मा की विषय-ग्रहण में जो प्रवृत्ति होती है, उसे 'उपयोगरूप भावेन्द्रिय' कहते हैं।
इस विषय को विस्तारपूर्वक जानने के लिये प्रज्ञापना-पद १५, पृ. २९३; तत्त्वार्थ-अध्याय २, सू. १७ - १८ तथा वृत्ति; विशेषाव., गा. २९९३-३००३ तथा लोकप्रकाश-सर्ग ३, श्लोक ४६४ से आगे देखना चाहिये।
परिशिष्ट 'ग'
पृ. १०, पंक्ति १९ के 'संज्ञा' शब्द पर
संज्ञा का मतलब आभोग (मानसिक क्रिया - विशेष ) से है। इसके (क) ज्ञान और (ख) अनुभव, ये दो भेद हैं।
(क) मति, श्रुत आदि पाँच प्रकार का ज्ञान 'ज्ञानसंज्ञा' है।
(ख) अनुभवसंज्ञा के (१) आहार, (२) भय, (३) मैथुन, (४) परिग्रह, (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया, (८) लोभ, (९) ओघ, (१०) लोक, (११) मोह, (१२) धर्म, (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) जुगुप्सा और (१६) शोक, ये सोलह भेद हैं। आचाराङ्गनिर्युक्ति, गा. ३८-३९ में तो अनुभवसंज्ञा के ये सोलह भेद किये गये हैं। लेकिन भगवती - शतक ७, उद्देश ८ में तथा प्रज्ञापनापद ८ में इनमें से पहले दस ही भेद, निर्दिष्ट हैं।
ये संज्ञाये सब जीवों में न्यूनाधिक प्रमाण में पाई जाती हैं; वे अन्य संज्ञाओं की अपेक्षा से । एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त के जीवों में चैतन्य का विकास क्रमशः अधिकाधिक है। इस विकास के तर-तम-भाव को समझाने के लिये शास्त्र में इसके स्थूल रीति पर चार विभाग किये गये हैं ।
(१) पहले विभाग में ज्ञान का अत्यन्त अल्प विकास विवक्षित है। यह विकास, इतना अल्प है कि इस विकास से युक्त जीव, मूच्छित की तरह चेष्टारहित होते हैं। इस अव्यक्ततर चैतन्य को 'ओषसंज्ञा' कहा गया है। एकेन्द्रिय जीव, ओघसंज्ञा वाले ही हैं।
(२) दूसरे विभाग में विकास की इतनी मात्रा विवक्षित है कि जिससे कुछ भूतकाल — सुदीर्घ भूतकाल का नहीं - स्मरण किया जाता है और जिससे इष्ट विषयों में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट विषयों से निवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति - निवृत्तिकारी ज्ञान को 'हेतुवादोपदेशिकी संज्ञा' कहा है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और सम्मूच्छिम पञ्चेन्द्रिय जीव, हेतुवादोपदेशिक्री संज्ञा वाले हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org