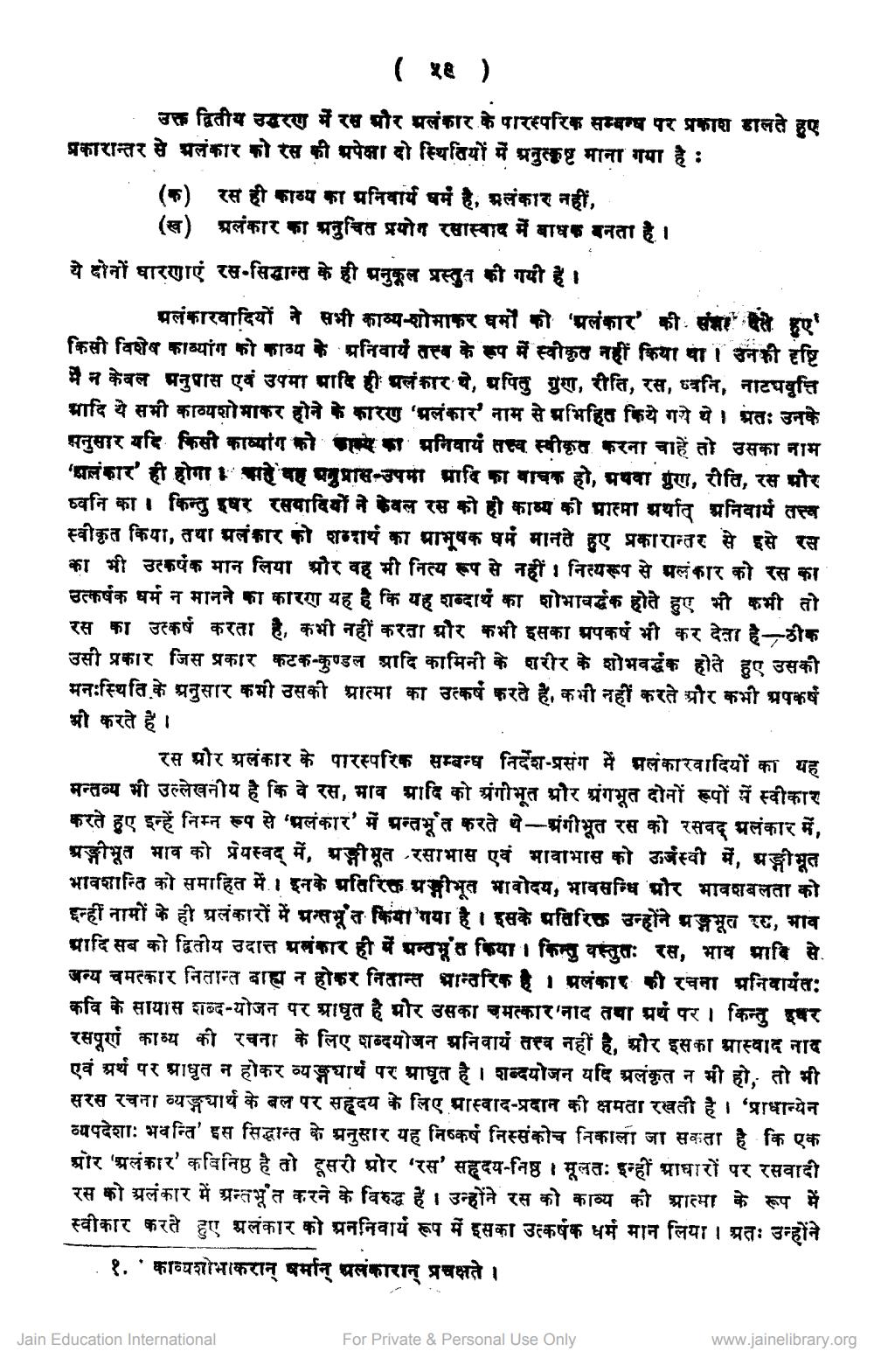________________
उक्त द्वितीय उखरण में रस मोर प्रलंकार के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए प्रकारान्तर से अलंकार को रस की अपेक्षा दो स्थितियों में अनुकृष्ट माना गया है :
(क) रस ही काव्य का अनिवार्य धर्म है, अलंकार नहीं,
(ख) अलंकार का अनुचित प्रयोग रसास्वाद में बाधक बनता है। ये दोनों धारणाएं रस-सिद्धान्त के ही अनुकूल प्रस्तुत की गयी है।
प्रलंकारवादियों ने सभी काव्य-शोभाकर धर्मों को 'अलंकार' की संभाते हुए किसी विशेष काव्यांग को काव्य के अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकृत नहीं किया था। उनकी दृष्टि में न केवल अनुपास एवं उपमा मादि ही अलंकार थे, अपितु गुण, रीति, रस, ध्वनि, नाटयवृत्ति भादि ये सभी मी काव्यशोमाकर होने के कारण 'अलंकार' नाम से अभिहित किये गये थे। प्रतः उनके मनुसार यदि किसी काव्यांग को काम का मनिवार्य तत्व स्वीकृत करना चाहें तो उसका नाम 'अलंकार' ही होगा। चाहे वह मनुप्रास-उपमा प्रादि का वाचक हो, अथवा गुण, रीति, रस पौर ध्वनि का। किन्तु इधर रसवादियों ने केवल रस को ही काव्य की प्रास्मा अर्थात् अनिवार्य तत्व स्वीकृत किया, तथा भलंकार को शनार्थ का प्राभूषक धर्म मानते हुए प्रकारान्तर से इसे रस का भी उत्कर्षक मान लिया और वह भी नित्य रूप से नहीं। नित्यरूप से प्रलंकार को रस का उत्कर्षक धर्म न मानने का कारण यह है कि यह शब्दार्थ का शोभावर्द्धक होते हुए भी कभी तो रस का उत्कर्ष करता है, कभी नहीं करता और कभी इसका अपकर्ष भी कर देता है-ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कटक-कुण्डल प्रादि कामिनी के शरीर के शोभवर्द्धक होते हुए उसकी मनःस्थिति के अनुसार कभी उसकी प्रात्मा का उत्कर्ष करते हैं, कभी नहीं करते और कभी अपकर्ष भी करते हैं।
रस और अलंकार के पारस्परिक सम्बन्ध निर्देश-प्रसंग में भलंकारवादियों का यह मन्तव्य भी उल्लेखनीय है कि वे रस, भाव प्रादि को अंगीभूत और अंगभूत दोनों रूपों में स्वीकार करते हुए इन्हें निम्न रूप से 'प्रलंकार' में अन्तर्भूत करते थे-अंगीभूत रस को रसवद् अलंकार में, अङ्गीभूत भाव को प्रेयस्वद् में, मनीभूत रसाभास एवं भावाभास को उर्जस्वी में, मनीभूत भावशान्ति को समाहित में। इनके अतिरिक्त मलीभूत भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता को इन्हीं नामों के ही प्रलंकारों में भरसभूत किया गया है । इसके अतिरिक उन्होंने मङ्गभूत रस, भाव मादि सब को द्वितीय उदात्त प्रलंकार ही में अन्तत किया। किन्तु वस्तुतः रस, भाव मादि से. अन्य चमत्कार नितान्त बाह्य न होकर नितान्त भान्तरिक है । प्रलंकार की रचना अनिवार्यतः कवि के सायास शब्द-योजन पर प्राघृत है मौर उसका चमत्कार 'नाद तथा प्रथं पर । किन्तु इधर रसपूर्ण काव्य की रचना के लिए शब्दयोजन अनिवार्य तत्व नहीं है, और इसका मास्वाद नाद एवं अर्थ पर प्राधृत न होकर व्यङ्गधार्थ पर माघृत है । शब्दयोजन यदि अलंकृत न भी हो, तो भी सरस रचना व्यङ्गयार्थ के बल पर सहृदय के लिए मास्वाद-प्रदान की क्षमता रखती है । 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति' इस सिद्धान्त के अनुसार यह निष्कर्ष निस्संकोच निकाला जा सकता है कि एक और 'अलंकार' कविनिष्ठ है तो दूसरी ओर 'रस' सहृदय-निष्ठ । मूलतः इन्हीं आधारों पर रसवादी रस को अलंकार में अन्तर्भूत करने के विरुद्ध हैं । उन्होंने रस को काव्य को प्रात्मा के रूप में स्वीकार करते हुए अलंकार को अननिवार्य रूप में इसका उत्कर्षक धर्म मान लिया । अतः उन्होंने .. १. ' काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org