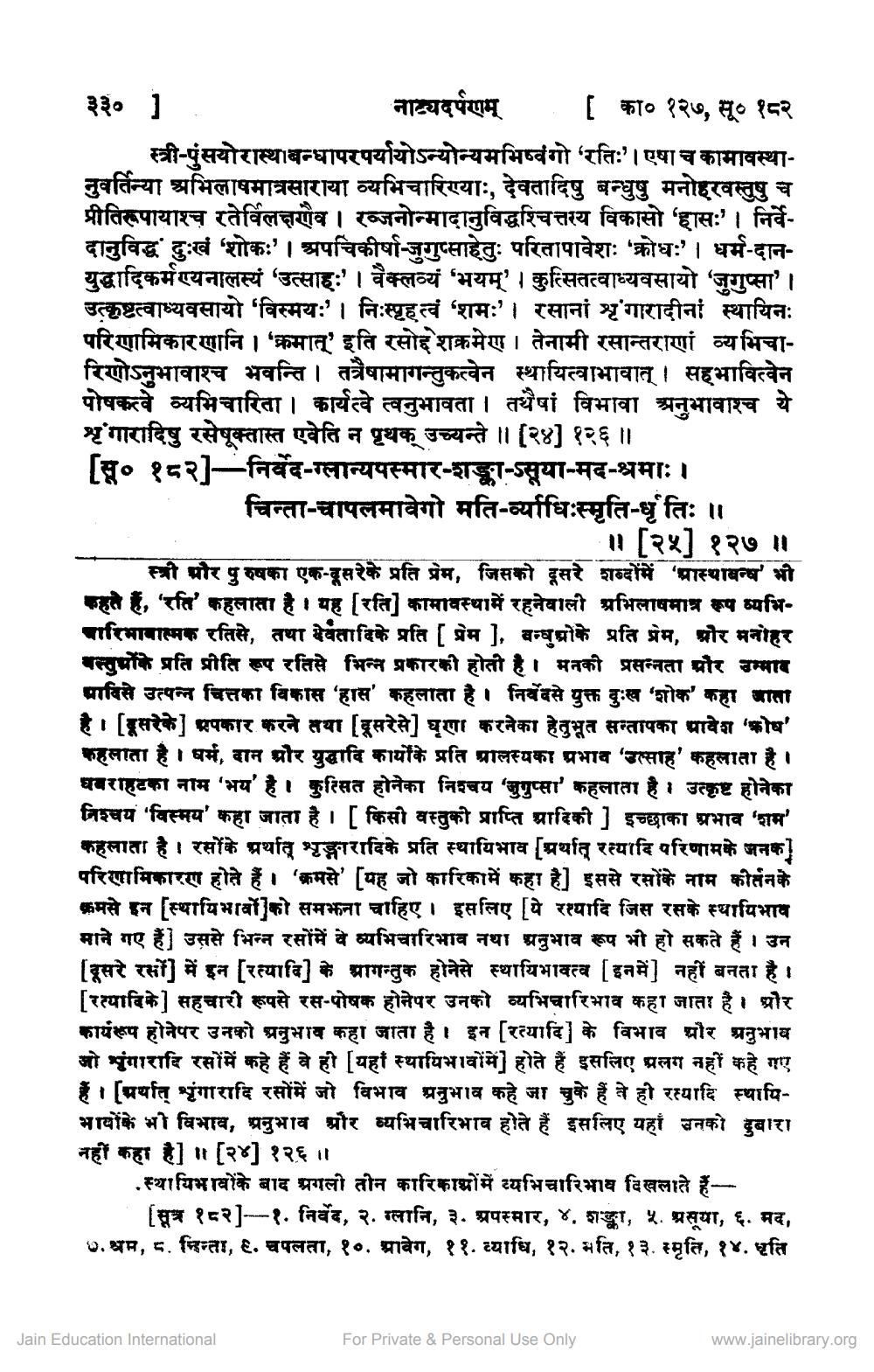________________
३३० ]
नाट्यदर्पणम्
[ का० १२७, सू० १८२
स्त्री-पुंसयोरास्था बन्धापरपर्यायोऽन्योन्यमभिष्वंगो ' रतिः' । एषा च कामावस्थानुवर्तिन्या अभिलाषमात्रसाराया व्यभिचारिण्याः, देवतादिषु बन्धुषु मनोहरवस्तुषु च प्रीतिरूपायाश्च रतेर्विलक्षणैव । रब्जनोन्मादानुविद्धश्चित्तस्य विकासो 'हास:' । निर्वे - दानुविद्ध ं दुःखं 'शोकः' । अपचिकीर्षा जुगुप्साहेतुः परितापावेशः 'क्रोधः' । धर्म-दानयुद्धादिकर्मण्यनालस्यं 'उत्साह:' । वैक्लव्यं 'भयम्' । कुत्सितत्वाध्यवसायो 'जुगुप्सा' । उत्कृष्टत्वाध्यवसायो 'विस्मयः' । निःस्पृहत्वं 'शमः ' । रसानां शृंगारादीनां स्थायिनः परिणामिकारणानि । 'क्रमात्' इति रसोद्द शक्रमेण । तेनामी रसान्तराणां व्यभिचारिणोऽनुभावाश्च भवन्ति । तत्रैषामागन्तुकत्वेन स्थायित्वाभावात् । सहभावित्वेन पोषकत्वे व्यभिचारिता । कार्यत्वे त्वनुभावता । तथैषां विभावा अनुभावाश्च ये गारादिषु रसेषूक्तास्त एवेति न पृथक् उच्यन्ते ।। [२४] १२६ ।। [सू० १८२ ] - निर्वेद-ग्लान्यपस्मार - शङ्का - ऽसूया-मद-श्रमाः । चिन्ता - चापलमावेगो मति-र्व्याधिःस्मृति- धृतिः ॥
।। [२५] १२७ ॥ शब्दोंमें 'प्रास्थाबन्ध' भी अभिलाषमात्र रूप व्यभि
स्त्री और पुरुषका एक-दूसरे के प्रति प्रेम, जिसको दूसरे कहते हैं, 'रति' कहलाता है । यह [रति] कामावस्था में रहनेवाली चारिभावात्मक रतिसे, तथा देवतादिके प्रति [ प्रेम ], बन्धुधोके प्रति प्रेम, और मनोहर वस्तुओंके प्रति प्रीति रूप रतिसे भिन्न प्रकारकी होती है । मनकी प्रसन्नता और उन्माद प्राविसे उत्पन्न चित्तका विकास 'हास' कहलाता है । निर्देबसे युक्त दुःख 'शोक' कहा जाता है । [दूसरेके ] एपकार करने तथा [दूसरेसे] घृणा करनेका हेतुभूत सन्तापका प्रावेश 'क्रोध' कहलाता है। धर्म, दान और युद्धादि कार्योंके प्रति प्रालस्यका प्रभाव 'उत्साह' कहलाता है । घबराहटका नाम 'भय' है । कुत्सित होनेका निश्चय 'जुगुप्सा' कहलाता है । उत्कृष्ट होनेका निश्चय 'विस्मय' कहा जाता है। [किसी वस्तुको प्राप्ति आदिकी ] इच्छाका प्रभाव 'शम' कहलाता है। रसोंके अर्थात् शृङ्गारादिके प्रति स्थायिभाव [श्रर्थात् रत्यादि परिणाम के जनक ] परिणामिकारण होते हैं। 'क्रमसे' [यह जो कारिकामें कहा है] इससे रसोंके नाम कीर्तनके क्रमसे इन [स्थायिभाव]को समझना चाहिए। इसलिए [ ये रत्यादि जिस रसके स्थायिभाव माने गए हैं] उससे भिन्न रसोंमें वे व्यभिचारिभाव नथा अनुभाव रूप भी हो सकते हैं। उन [दूसरे रसों] में इन [रत्यादि] के श्रागन्तुक होनेसे स्थायिभावत्व [ इनमें ] नहीं बनता है । [रत्यादिके] सहचारी रूपसे रस-पोषक होनेपर उनको व्यभिचारिभाव कहा जाता है । और कार्यरूप होनेपर उनको अनुभाव कहा जाता है । इन [रत्यादि ] के विभाव और अनुभाव जो श्रृंगारादि रसों में कहे हैं वे ही [ यहाँ स्थायिभावों में] होते हैं इसलिए अलग नहीं कहे गए हैं । [ प्रर्थात् श्रृंगारादि रसोंमें जो विभाव अनुभाव कहे जा चुके हैं वे ही रत्यादि स्थायिभावोंके भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव होते हैं इसलिए यहाँ उनको दुबारा नहीं कहा है ] ॥ [२४] १२६ ॥
. स्थायिभावोंके बाद अगली तीन कारिकाथों में व्यभिचारिभाव दिखलाते हैं
[ सूत्र १८२ ] -- १. निर्वेद, २. ग्लानि, ३. अपस्मार, ४. शङ्का, ५. श्रसूया, ६. मद, ७. श्रम, ८. चिन्ता, ६. चपलता, १०. श्रावेग, ११. व्याधि, १२. मति, १३. स्मृति, १४. धृति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org