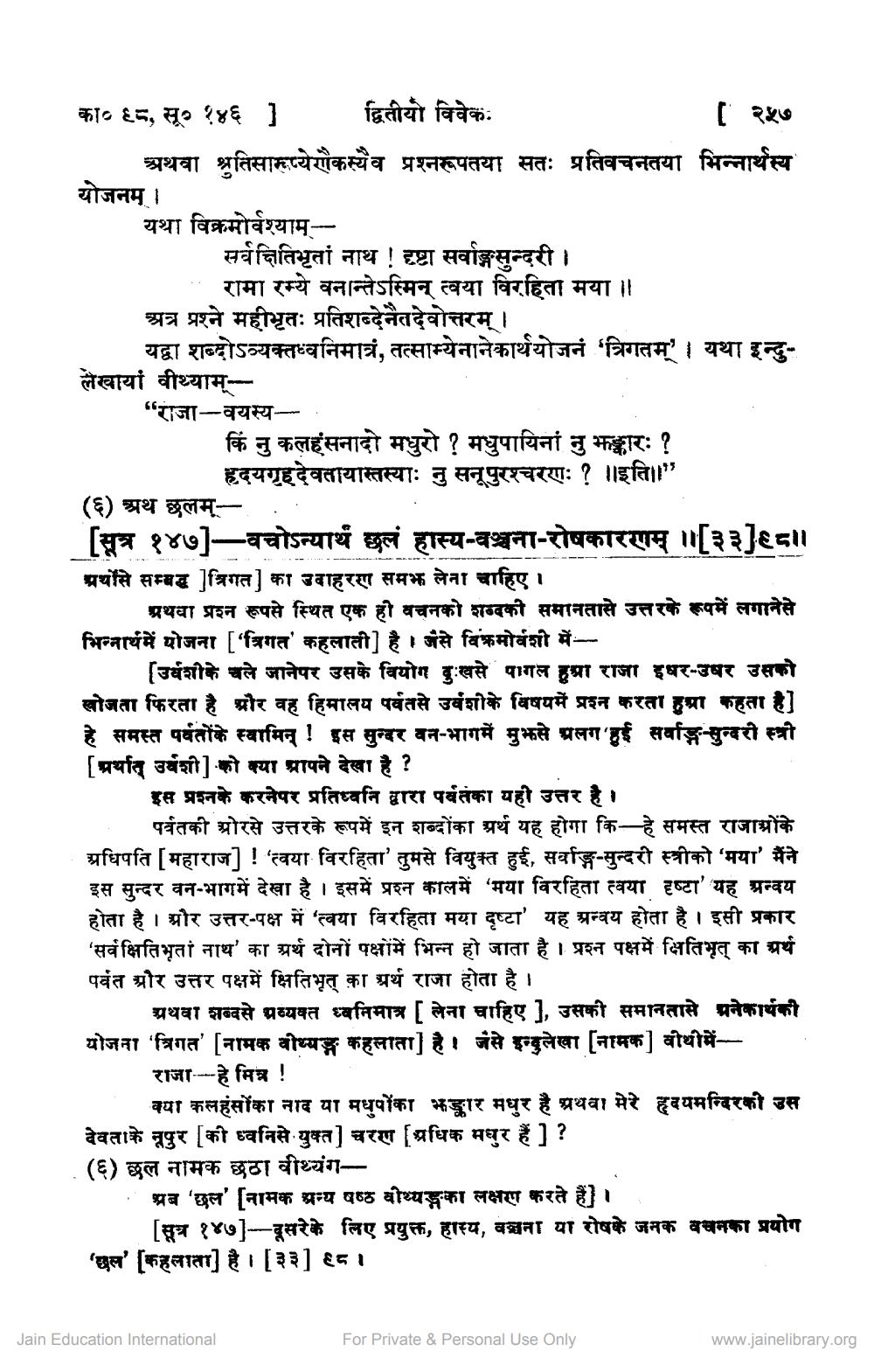________________
का०६८, सू० १४६ ] द्वितीयो विवेकः
[ २५७ अथवा श्रुतिसारूप्येणैकस्यैव प्रश्नरूपतया सतः प्रतिवचनतया भिन्नार्थस्य योजनम्। यथा विक्रमोर्वश्याम
सर्वक्षितिभृतां नाथ ! दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी। - रामा रम्ये वनान्तेऽस्मिन् त्वया विरहिता मया ॥ अत्र प्रश्ने महीभृतः प्रतिशब्देनैतदेवोत्तरम्।
यद्वा शब्दोऽव्यक्तध्वनिमात्रं, तत्साम्येनानेकार्थयोजनं 'त्रिगतम्' । यथा इन्दुलेखायां वीथ्याम्"राजा-वयस्य--
किं नु कलहंसनादो मधुरो ? मधुपायिनां नु झङ्कारः ?
हृदयगृहदेवतायास्तस्याः नु सनूपुरश्चरणः ? ॥इति।" (६) अथ छलम्[सूत्र १४७]-वचोऽन्यार्थ छलं हास्य-वञ्चना-रोषकारणम् ॥[३३]९८॥ प्रोंसे सम्बद्ध ]त्रिगत] का उदाहरण समझ लेना चाहिए।
अथवा प्रश्न रूपसे स्थित एक ही वचनको शब्दको समानतासे उत्तरके रूपमें लगानेसे भिन्नार्थ में योजना ["त्रिगत' कहलाती है। जैसे विक्रमोर्वशी में
(उर्वशीके चले जानेपर उसके वियोग दुःखसे पागल हुआ राजा इधर-उधर उसको खोजता फिरता है और वह हिमालय पर्वतसे उर्वशीके विषयमें प्रश्न करता हुमा कहता है] हे समस्त पर्वतोंके स्वामिन् ! इस सुन्दर वन-भागमें मुझसे अलग हुई सर्वाङ्ग-सुन्दरी स्त्री [प्रर्थात् उर्वशी] को क्या प्रापने देखा है ?
इस प्रश्नके करनेपर प्रतिध्वनि द्वारा पर्वतका यही उत्तर है।
पर्वतकी प्रोरसे उत्तरके रूपमें इन शब्दोंका अर्थ यह होगा कि हे समस्त राजाओंके अधिपति [महाराज] ! 'त्वया विरहिता' तुमसे वियुक्त हुई, सर्वाङ्ग-सुन्दरी स्त्रीको 'मया' मैंने इस सुन्दर वन-भागमें देखा है । इसमें प्रश्न कालमें 'मया विरहिता त्वया दृष्टा' यह अन्वय होता है । और उत्तर-पक्ष में 'त्वया विरहिता मया दृष्टा' यह अन्वय होता है । इसी प्रकार 'सर्वक्षितिभृतां नाथ' का अर्थ दोनों पक्षोंमें भिन्न हो जाता है। प्रश्न पक्षमें क्षितिभृत् का अर्थ पर्वत और उत्तर पक्षमें क्षितिभृत् का अर्थ राजा होता है ।
अथवा शब्दसे प्रव्यक्त ध्वनिमात्र [ लेना चाहिए ], उसकी समानतासे अनेकार्थकी योजना 'विगत' [नामक वीथ्यङ्ग कहलाता है। जैसे इन्दुलेखा [नामक] वीथीमें
राजा-हे मित्र !
क्या कलहंसोंका नाद या मधुपोंका झङ्कार मधुर है अथवा मेरे हृदयमन्दिरकी उस देवताके नूपुर [की ध्वनिसे युक्त] चरण [अधिक मधुर हैं ] ? (६) छल नामक छठा वीथ्यंग- अब 'छल' [नामक अन्य षष्ठ वीथ्यङ्गका लक्षण करते हैं।
[सूत्र १४७]-दूसरेके लिए प्रयुक्त, हास्य, वञ्चना या रोषके जनक वचनका प्रयोग 'छल' [कहलाता है । [३३] ९८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org