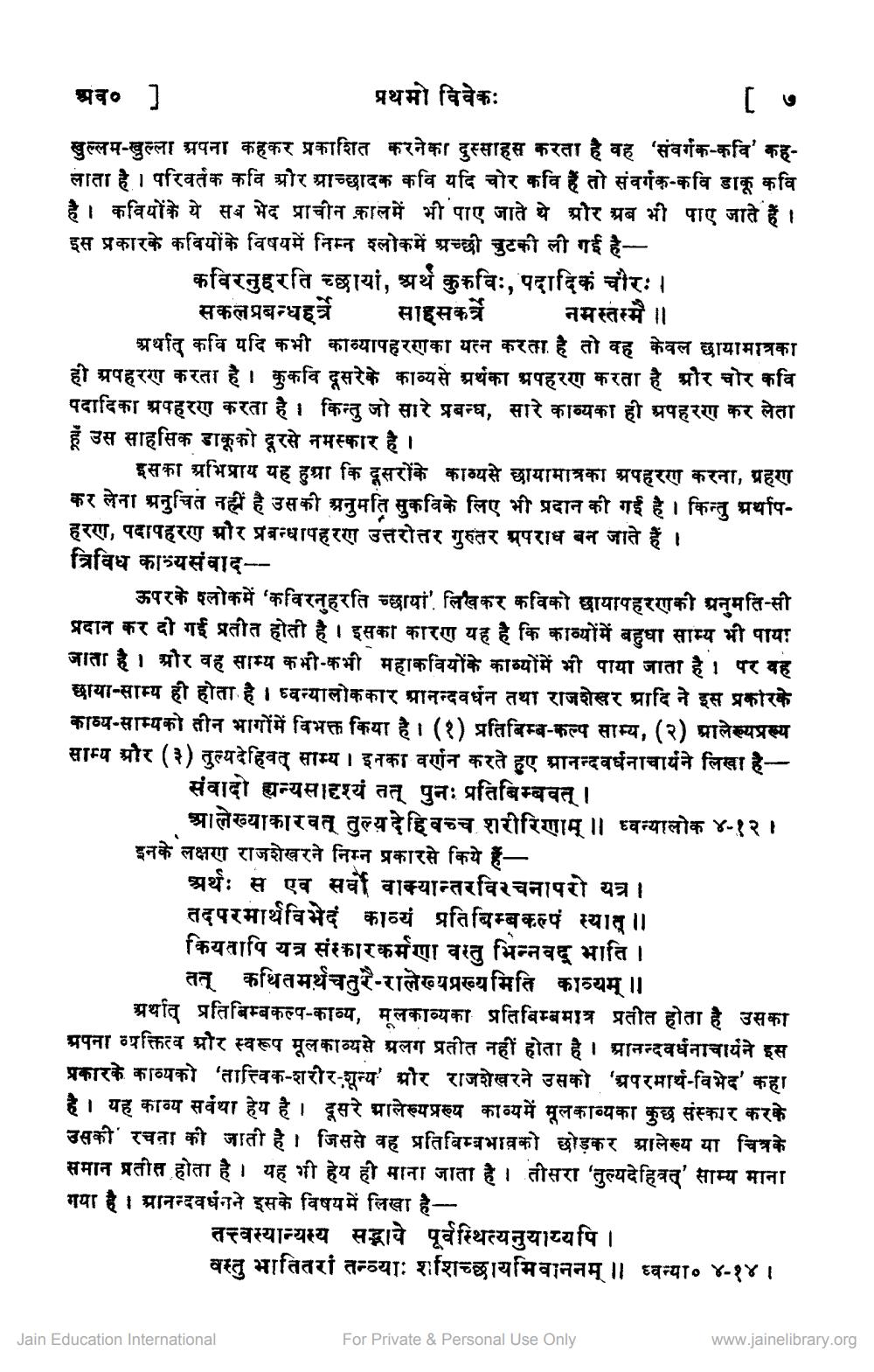________________
अव० ] प्रथमो विवेकः
[ ७ खुल्लम-खुल्ला अपना कहकर प्रकाशित करनेका दुस्साहस करता है वह 'संवर्गक-कवि' कहलाता है । परिवर्तक कवि और आच्छादक कवि यदि चोर कवि हैं तो संवर्गक-कवि डाकू कवि है। कवियोंके ये सब भेद प्राचीन काल में भी पाए जाते थे और अब भी पाए जाते हैं। इस प्रकारके कवियों के विषय में निम्न श्लोकमें अच्छी चुटकी ली गई है
कविरनुहरति च्छायां, अर्थ कुकविः, पदादिकं चौरः।
सकलप्रबन्धहत्रे साहसकर्त्रे नमस्तस्मै । अर्थात् कवि यदि कभी काव्यापहरणका यत्न करता है तो वह केवल छायामात्रका ही अपहरण करता है। कुकवि दूसरेके काव्य से अर्थका अपहरण करता है और चोर कवि पदादिका अपहरण करता है। किन्तु जो सारे प्रबन्ध, सारे काव्यका ही अपहरण कर लेता हूँ उस साहसिक डाकूको दूरसे नमस्कार है।
इसका अभिप्राय यह हुआ कि दूसरोंके काव्यसे छायामात्रका अपहरण करना, ग्रहण कर लेना अनुचित नहीं है उसकी अनुमति सुकविके लिए भी प्रदान की गई है। किन्तु अर्थापहरण, पदापहरण और प्रबन्धापहरण उत्तरोत्तर गुरुतर अपराध बन जाते हैं । त्रिविध काव्यसंवाद--
ऊपरके श्लोकमें 'कविरनुहरति च्छायां' लिखकर कविको छायापहरणको अनुमति-सी प्रदान कर दी गई प्रतीत होती है । इसका कारण यह है कि काव्योंमें बहुधा साम्य भी पाया जाता है। और वह साम्य कभी-कभी महाकवियोंके काव्योंमें भी पाया जाता है। पर वह छाया-साम्य ही होता है । ध्वन्यालोककार प्रानन्दवर्धन तथा राजशेखर प्रादि ने इस प्रकारके काव्य-साम्यको तीन भागोंमें विभक्त किया है। (१) प्रतिबिम्ब-कल्प साम्य, (२) प्रालेख्यप्रख्य साम्य और (३) तुल्यदेहिवत् साम्य । इनका वर्णन करते हुए मानन्दवर्धनाचार्यने लिखा है
संवादो धन्यसादृश्यं तत् पुनः प्रतिबिम्बवत् ।
आलेख्याकारवत् तुल्य देहिवच्च शरीरिणाम् ॥ ध्वन्यालोक ४.१२ । इनके लक्षण राजशेखरने निम्न प्रकारसे किये हैं
अर्थः स एव सर्वो वाक्यान्तरविरचनापरो यत्र । तदपरमार्थविभेदं काव्यं प्रतिबिम्बकल्पं स्यात् ॥ कियतापि यत्र संस्कारकर्मणा वस्तु भिन्नवद् भाति ।
तत् कथितमर्थचतुरै-रालेख्यप्रख्यमिति काव्यम् ।। अर्थात् प्रतिबिम्बकल्प-काव्य, मूलकाव्यका प्रतिविम्बमात्र प्रतीत होता है उसका अपना व्यक्तित्व और स्वरूप मूल काव्यसे अलग प्रतीत नहीं होता है । प्रानन्दवर्धनाचार्यने इस प्रकारके काव्यको 'तात्त्विक-शरीर-शून्य' और राजशेखरने उसको 'अपरमार्थ-विभेद' कहा है। यह काव्य सर्वथा हेय है। दूसरे भालेख्यप्रख्य काव्य में मूलकाव्यका कुछ संस्कार करके उसकी रचना की जाती है। जिससे वह प्रतिविम्बभावको छोड़कर आलेख्य या चित्रके समान प्रतीत होता है। यह भी हेय ही माना जाता है। तीसरा 'तुल्यदेहिवत्' साम्य माना गया है। मानन्दवर्धनने इसके विषय में लिखा है
तत्त्वस्यान्यस्य सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि । वस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम् ।। ध्वन्या० ४-१४ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org