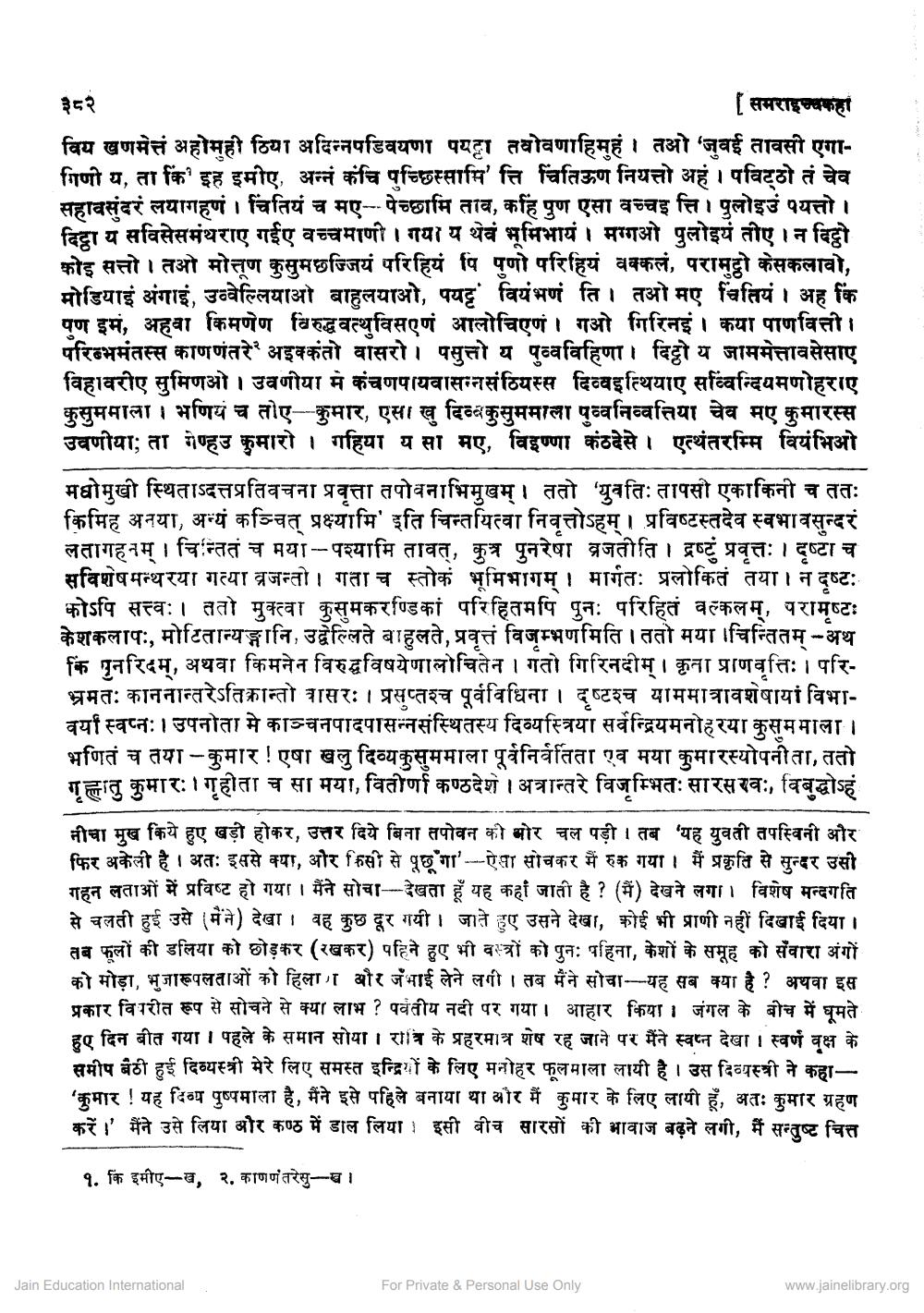________________
३८२
[ समराइच्चकहा
far खणमेतं अहोमुही ठिया अदिन्नपडिवयणा पट्टा तवोवणाहिमुहं । तओ 'जुवई तावसी एगागिणी य, ता कि इह इमीए, अन्नं कंचि पुच्छिस्सामि' त्ति चितिऊण नियत्तो अहं । पविट्ठो तं चैव सहावसुंदरं लयागहणं । चितियं च मए- पेच्छामि ताव, कहि पुण एसा वच्चइति । पुलोइउं पयत्तो । दिट्ठाय सविसेस मंथरा गईए वच्चमाणी । गया य थेवं भूमिभायं । मग्गओ पुलोइयं तीए । न दिट्ठो कोई सत्तो । तओ मोत्तूण कुसुमछज्जियं परिहियं पि पुणो परिहियं वक्कलं, परामुट्टो केसकलावो, मोडिया अंगाई, उब्वेल्लियाओ बाहुलयाओ, पयट्ट वियंभणं ति । तओ मए चितियं । अह कि पुण इमं अहवा किमणेण विरुद्धवत्युविसरणं आलोचिएणं । गओ गिरिनदं । कया पाणवित्ती | परिब्भमंतस्स काणणंतरे' अइक्कतो वासरो । पसुत्तो य पुव्वविहिणा । दिट्टो य जाममेत्तावसेसाए विहावरीए सुमिणओ । उवणीया मे कंचणपायवासन्नसंठियस्स दिव्वइत्थियाए सव्विन्दियमणोहराए कुसुममाला | भणियं च तोए-कुमार, एसा खु दिव्वकुसुममाला पुव्वनिव्वत्तिया चेव मए कुमारस्स उवणीया; ता गेहउ कुमारो । गहिया य सा मए, विइण्णा कंठदेसे । एत्थंतरम्मि वियंभिओ
मोमुखी स्थिताऽदत्तप्रतिवचना प्रवृत्ता तपोवनाभिमुखम् । ततो 'युवतिः तापसी एकाकिनी च ततः किमिह अनया, अन्यं कञ्चित् प्रक्ष्यामि इति चिन्तयित्वा निवृत्तोऽहम् । प्रविष्टस्तदेव स्वभावसुन्दरं लतागहनम् । चिन्तितं च मया - पश्यामि तावत्, कुत्र पुनरेषा व्रजतीति । द्रष्टुं प्रवृत्तः । दृष्टा च सविशेषमन्थरया गत्या व्रजन्तो । गता च स्तोकं भूमिभागम् । मार्गतः प्रलोकितं तया । न दृष्टः कोऽपि सत्त्वः । ततो मुक्त्वा कुसुमकरण्डिकां परिहितमपि पुनः परिहितं वल्कलम्, परामृष्टः केशकलापः, मोटितान्यङ्गानि, उद्वेल्लिते बाहुलते, प्रवृत्तं विजृम्भणमिति । ततो मया । चिन्तितम् - अथ किं पुनरिदम्, अथवा किमनेन विरुद्धविषयेणालोचितेन । गतो गिरिनदीम् । कृता प्राणवृत्तिः । परिभ्रमतः काननान्तरेऽतिक्रान्तो वासरः । प्रसुप्तश्च पूर्वविधिना । दृष्टश्च याममात्रावशेषायां विभावर्यां स्वप्नः । उपनोता मे काञ्चनपादपासन्नसंस्थितस्य दिव्यस्त्रिया सर्वेन्द्रियमनोहरया कुसुममाला । भणितं च तया - कुमार ! एषा खलु दिव्यकुसुममाला पूर्वनिर्वर्तिता एव मया कुमारस्योपनीता, ततो गृह्णातु कुमारः । गृहीता च सा मया, वितीर्णा कण्ठदेशे । अत्रान्तरे विजृम्भितः सारसवः, विबुद्धोऽहं
।
नीचा मुख किये हुए खड़ी होकर, उत्तर दिये बिना तपोवन की मोर चल पड़ी। तब 'यह युवती तपस्विनी और फिर अकेली है । अतः इससे क्या, और किसी से पूछूंगा' - ऐसा सोचकर मैं रुक गया। मैं प्रकृति से सुन्दर उसी गहन लताओं में प्रविष्ट हो गया। मैंने सोचा - देखता हूँ यह कहाँ जाती है ? (मैं) देखने लगा । विशेष मन्दगति से चलती हुई उसे (मैंने) देखा। वह कुछ दूर गयी । जाते हुए उसने देखा, कोई भी प्राणी नहीं दिखाई दिया तब फूलों की डलिया को छोड़कर (रखकर) पहिने हुए भी वस्त्रों को पुनः पहिना, केशों के समूह को सँवारा अंगों को मोड़ा, भुजारूपलताओं को हिलाग और जंभाई लेने लगी। तब मैंने सोचा -- यह सब क्या है ? अथवा इस प्रकार विपरीत रूप से सोचने से क्या लाभ ? पर्वतीय नदी पर गया । आहार किया । जंगल के बीच में घूमते हुए दिन बीत गया । पहले के समान सोया । रात्रि के प्रहरमात्र शेष रह जाने पर मैंने स्वप्न देखा । स्वर्ण वृक्ष के समीप बैठी हुई दिव्यस्त्री मेरे लिए समस्त इन्द्रियों के लिए मनोहर फूलमाला लायी है । उस दिव्यस्त्री ने कहा'कुमार ! यह दिव्य पुष्पमाला है, मैंने इसे पहिले बनाया था और मैं कुमार के लिए लायी हूँ, अतः कुमार ग्रहण करें।' मैंने उसे लिया और कण्ठ में डाल लिया। इसी बीच सारसों की आवाज बढ़ने लगी, मैं सन्तुष्ट चित्त
१. कि इमीए - ख, २. काणणंतरेसु – ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org