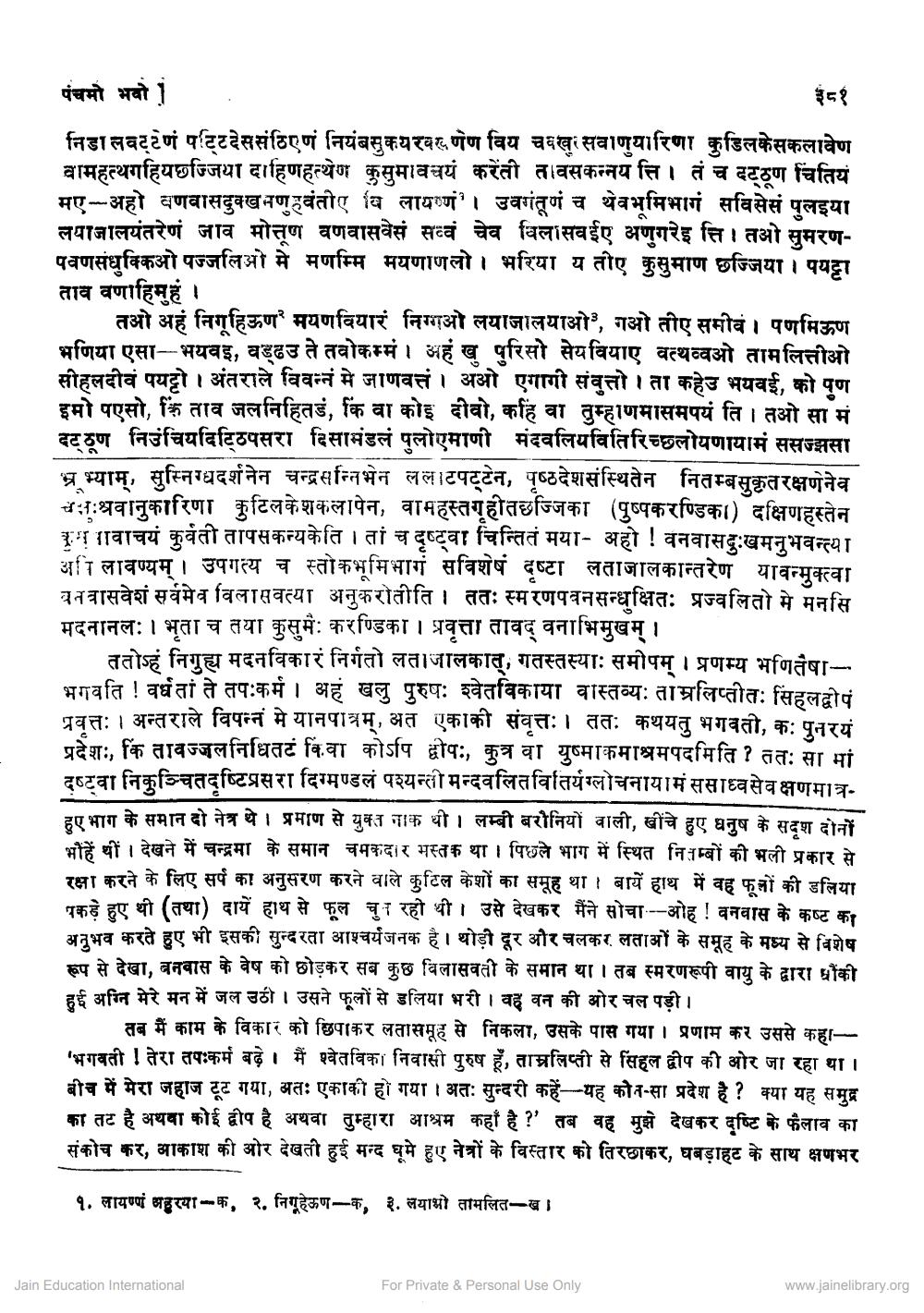________________
पंचमो भवो
३८१ निडा लवटेणं पट्टिदेससंठिएणं नियंबसुकयरवर णेण विय चवखुर सवाणुयारिणा कुडिलकेसकलावेण वामहत्थगहियछज्जिया दाहिणहत्थेण कुसुमावचयं करेंती तावसकन्नय ति। तं च ठूण चितियं मए-अहो वणवासदुक्ख नणुहवंतीए वि लायण'। उवगंतूणं च थेवभूमिभागं सविसेसं पुलइया लयाजालयंतरेणं जाव मोत्तूण वणवासवेसं सव्वं चेव विलासवईए अणुगरेइ त्ति । तओ सुमरणपवणसंधुक्किओ पज्जलिओ मे मणम्मि मयणाणलो। भरिया य तीए कुसुमाण छज्जिया। पयट्टा ताव वणाहिमुहं।
तओ अहं निहिऊण मयणक्यिारं निग्गओ लयाजालयाओ', गओ तीए समीवं । पणमिऊण भणिया एसा--भयवइ, वड्ढउ ते तवोकम्मं । अहं खु पुरिसो सेयवियाए वत्थव्वओ तामलित्तीओ सीहलदीवं पयट्टो । अंतराले विवन्नं मे जाणवत्तं । अओ एगागी संवुत्तो। ता कहेउ भयवई, को पुण इमो पएसो, किं ताव जलनिहितडं, कि वा कोइ दीवो, कहिं वा तुम्हाणमासमपयं ति । तओ सा में दळूण निउंचियदिट्ठिपसरा दिसामंडलं पुलोएमाणी मंदवलियवितिरिच्छलोयणायाम ससज्झसा भ्र भ्याम, सुस्निग्धदर्शनेन चन्द्रसन्निभेन ललाटपट्टेन, पृष्ठदेशसंस्थितेन नितम्बसूकृतरक्षणेनेव सःश्रवानुकारिणा कुटिलकेशकलापेन, वामहस्तगृहीतछज्जिका (पुष्पकरण्डिका) दक्षिणहस्तेन मावाचयं कुर्वती तापसकन्यकेति । तां च दृष्ट्वा चिन्तितं मया- अहो ! वनवासदुःखमनूभवन्त्या अगि लावण्यम्। उपगत्य च स्तोकभूमिभागं सविशेष दृष्टा लताजालकान्तरेण यावन्मुक्त्वा वनवासवेशं सर्वमेव विलासवत्या अनुकरोतीति । ततः स्मरणपवनसन्धक्षितः प्रज्वलितो मे मनसि मदनानलः । भृता च तया कुसुमैः करण्डिका । प्रवृत्ता तावद् वनाभिमुखम् ।
ततोऽहं निगुह्य मदनविकारं निर्गतो लताजालकात्, गतस्तस्याः समीपम् । प्रणम्य भणितैषाभगवति ! वर्धतां ते तपःकर्म । अहं खलु पुरुषः श्वेतविकाया वास्तव्यः ताम्रलिप्तीतः सिंहलदो प्रवत्तः । अन्तराले विपन्नं मे यानपात्रम्, अत एकाकी संवृत्तः। ततः कथयतु भगवती, कः पूनरयं प्रदेशः, किं तावज्जलनिधितटं किंवा कोऽपि द्वीपः, कुत्र वा युष्माकमाश्रमपदमिति ? ततः सा मां दष्टवा निकुञ्चितदष्टिप्रसरा दिग्मण्डलं पश्यन्ती मन्दवलितवितिर्यग्लोचनायामं ससाध्व सेवक्षणमात्र. हुए भाग के समान दो नेत्र थे। प्रमाण से युक्त नाक थी। लम्बी बरौनियों वाली, खींचे हुए धनुष के सदृश दोनों
। देखने में चन्द्रमा के समान चमकदार मस्तक था। पिछले भाग में स्थित नितम्बों की भली प्रकार से रक्षा करने के लिए सर्प का अनुसरण करने वाले कुटिल केशों का समूह था। बायें हाथ में वह फूलों की डलिया पकडे हए थी (तथा) दायें हाथ से फूल चुन रही थी। उसे देखकर मैंने सोचा--ओह ! वनवार
भव करते हुए भी इसकी सुन्दरता आश्चर्यजनक है। थोड़ी दूर और चलकर लताओं के समूह के मध्य से विशेष रूप से देखा, बनवास के वेष को छोड़कर सब कुछ विलासवती के समान था। तब स्मरणरूपी वायु के द्वारा धौंकी हई अग्नि मेरे मन में जल उठी। उसने फूलों से डलिया भरी । वह वन की ओर चल पड़ी।
तब मैं काम के विकार को छिपाकर लतासमूह से निकला, उसके पास गया। प्रणाम कर उससे कहा'भगवती ! तेरा तपःकर्म बढ़े। मैं श्वेतविका निवासी पुरुष हूँ, ताम्रलिप्ती से सिंहल द्वीप की ओर जा रहा था। बीच में मेरा जहाज टूट गया, अतः एकाकी हो गया । अतः सुन्दरी कहें-यह कोन-सा प्रदेश है ? क्या यह समुद्र का तट है अथवा कोई द्वीप है अथवा तुम्हारा आश्रम कहाँ है ?' तब वह मुझे देखकर दृष्टि के फैलाव का संकोच कर, आकाश की ओर देखती हुई मन्द घूमे हुए नेत्रों के विस्तार को तिरछाकर, घबड़ाहट के साथ क्षणभर
१. लायण्णं अहरया-क, २. निगृहेऊण-क, ३. लयानो तामलित-ख ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org