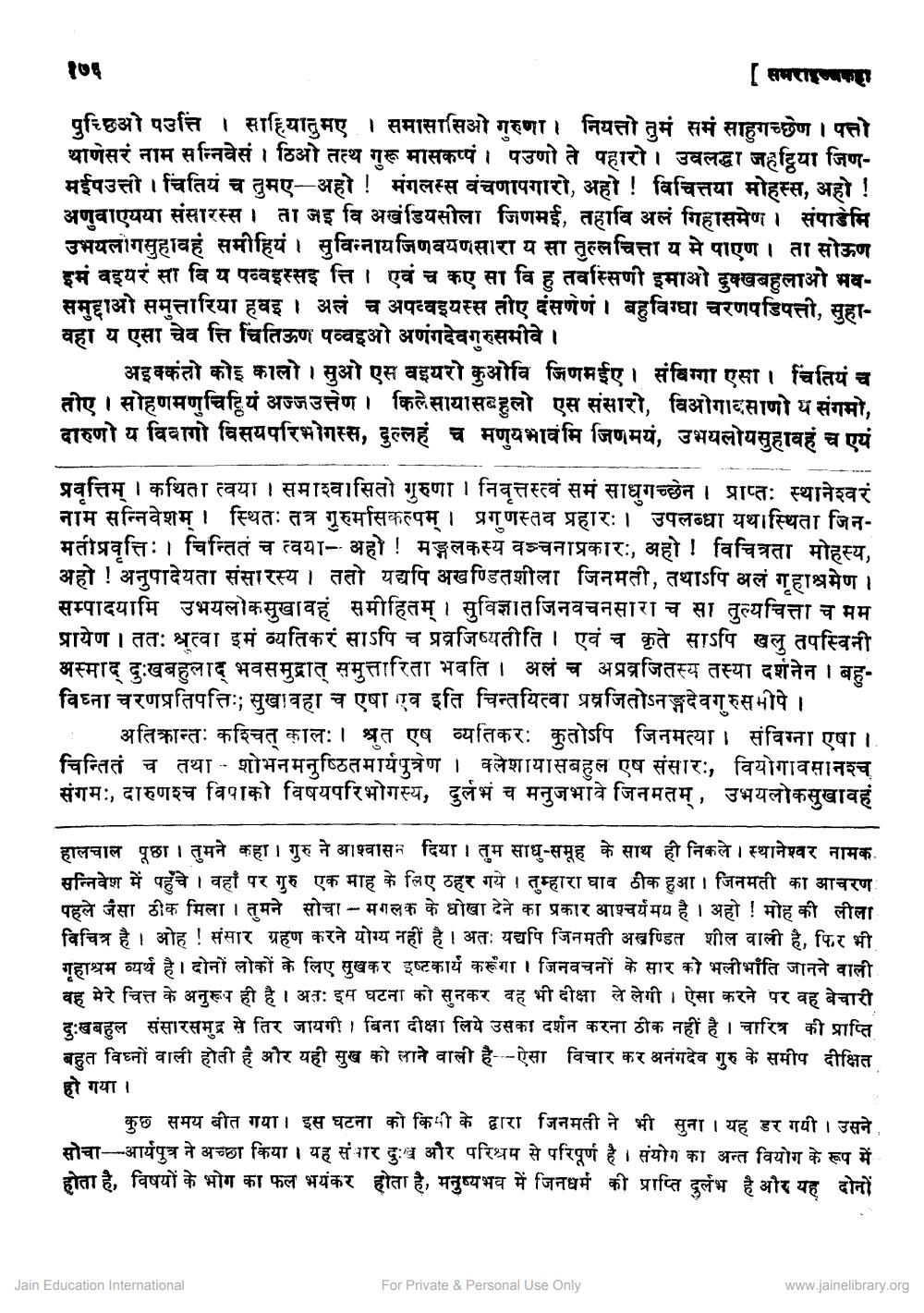________________
१७६
[समराहकहा पुच्छिओ पउत्ति । साहियातुमए । समासासिओ गुरुणा। नियत्तो तुमं समं साहुगच्छेण । पत्तो थाणेसरं नाम सन्निवेसं । ठिओ तत्थ गुरू मासकप्पं । पउणो ते पहारो। उवलद्धा जहटिया जिणमईपउत्ती। चितियं च तुमए-अहो ! मंगलस्स वेचणापगारो, अहो ! विचित्तया मोहस्स, अहो ! अणुवाएयया संसारस्स। ता जइ वि अखंडियसीला जिणमई, तहावि अलं गिहासमेण । संपाडेमि उभयलोगसुहावहं समीहियं । सुविन्नाय जिणवयणसारा य सा तुल्लचित्ता य मे पाएण। ता सोऊण इमं वइयरं सा वि य पव्वइस्सइ त्ति । एवं च कए सा वि हु तस्सिणी इमाओ दुक्खबहुलाओ भवसमुद्दाओ समुत्तारिया हवइ । अलं च अपव्वइयस्स तीए दसणेणं । बहुविग्घा चरणपडिपत्ती, सुहावहा य एसा चेव त्ति चितिऊण पव्वइओ अणंगदेवगुरुसमीवे ।
___ अइक्कंतो कोई कालो। सुओ एस वइयरो कुओवि जिणमईए। संविग्गा एसा। चितियं च तीए । सोहणमणुचिट्टियं अज्ज उत्तेण । किलेसायासबहुलो एस संसारो, विओगावसाणो य संगमो, दारुणो य विवागो विसयपरिभोगस्स, दुल्लहं च मणुयभाव मि जिणमयं, उभयलोयसुहावहं च एवं
प्रवृत्तिम् । कथिता त्वया । समाश्वासितो गुरुणा । निवृत्तस्त्वं समं साधुगच्छेन । प्राप्तः स्थानेश्वरं नाम सन्निवेशम् । स्थितः तत्र गुरुर्मासकल्पम्। प्रगुणस्तव प्रहारः। उपलब्धा यथास्थिता जिनमतीप्रवृत्तिः। चिन्तितं च त्वया-- अहो ! मङ्गलकस्य वञ्चनाप्रकारः, अहो ! विचित्रता मोहस्य, अहो ! अनुपादेयता संसारस्य । ततो यद्यपि अखण्डितशीला जिनमती, तथाऽपि अलं गहाश्रमेण । सम्पादयामि उभयलोकसुखावहं समीहितम् । सुविज्ञात जिनवचनसारा च सा तुल्यचित्ता च मम प्रायेण । ततः श्रुत्वा इमं व्यतिकरं साऽपि च प्रव्रजिष्यतीति । एवं च कृते साऽपि खलु तपस्विनी अस्माद् दुःखबहुलाद् भवसमुद्रात् समुत्तारिता भवति । अलं च अप्रव्रजितस्य तस्या दर्शनेन । बहविघ्ना चरणप्रतिपत्तिः; सुखावहा च एषा एव इति चिन्तयित्वा प्रवजितोऽनङ्गदेवगरुसमीपे । - अतिक्रान्तः कश्चित् कालः। श्रुत एष व्यतिकरः कुतोऽपि जिनमत्या। संविग्ना एषा। चिन्तितं च तथा- शोभन मनुष्ठितमार्यपुत्रेण । क्लेशायासबहुल एष संसारः, वियोगावसानश्च संगमः, दारुणश्च विपाको विषयपरिभोगस्य, दुर्लभं च मनुजभावे जिनमतम् , उभयलोकसुखावहं
--
हालचाल पूछा । तुमने कहा । गुरु ने आश्वासन दिया। तुम साधु-समूह के साथ ही निकले। स्थानेश्वर नामक. सन्निवेश में पहुँचे । वहाँ पर गुरु एक माह के लिए ठहर गये । तुम्हारा घाव ठीक हुआ। जिनमती का आचरण पहले जैसा ठीक मिला । तुमने सोचा-मगलक के धोखा देने का प्रकार आश्चर्यमय है । अह विचित्र है। ओह ! संसार ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः यद्यपि जिनमती अखण्डित शील वाली है. फिर भी गृहाश्रम व्यर्थ है। दोनों लोकों के लिए सुखकर इष्टकार्य करूंगा। जिनवचनों के सार को भलीभांति जानने वाली वह मेरे चित्त के अनुरूप ही है। अत: इस घटना को सुनकर वह भी दीक्षा ले लेगी। ऐसा करने पर वह बेचारी दुःखबहुल संसारसमुद्र से तिर जायगी। बिना दीक्षा लिये उसका दर्शन करना ठीक नहीं है । चारित्र की प्राप्ति बहत विघ्नों वाली होती है और यही सुख को लाने वाली है---ऐसा विचार कर अनंगदेव गुरु के समीप दीक्षित हो गया।
कुछ समय बीत गया। इस घटना को किसी के द्वारा जिनमती ने भी सुना । यह डर गयी। उसने सोचा-आर्यपुत्र ने अच्छा किया। यह संभार दुःख और परिश्रम से परिपूर्ण है । संयोग का अन्त वियोग के रूप में होता है, विषयों के भोग का फल भयंकर होता है, मनुष्यभव में जिनधर्म की प्राप्ति दुर्लभ है और यह दोनों
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org