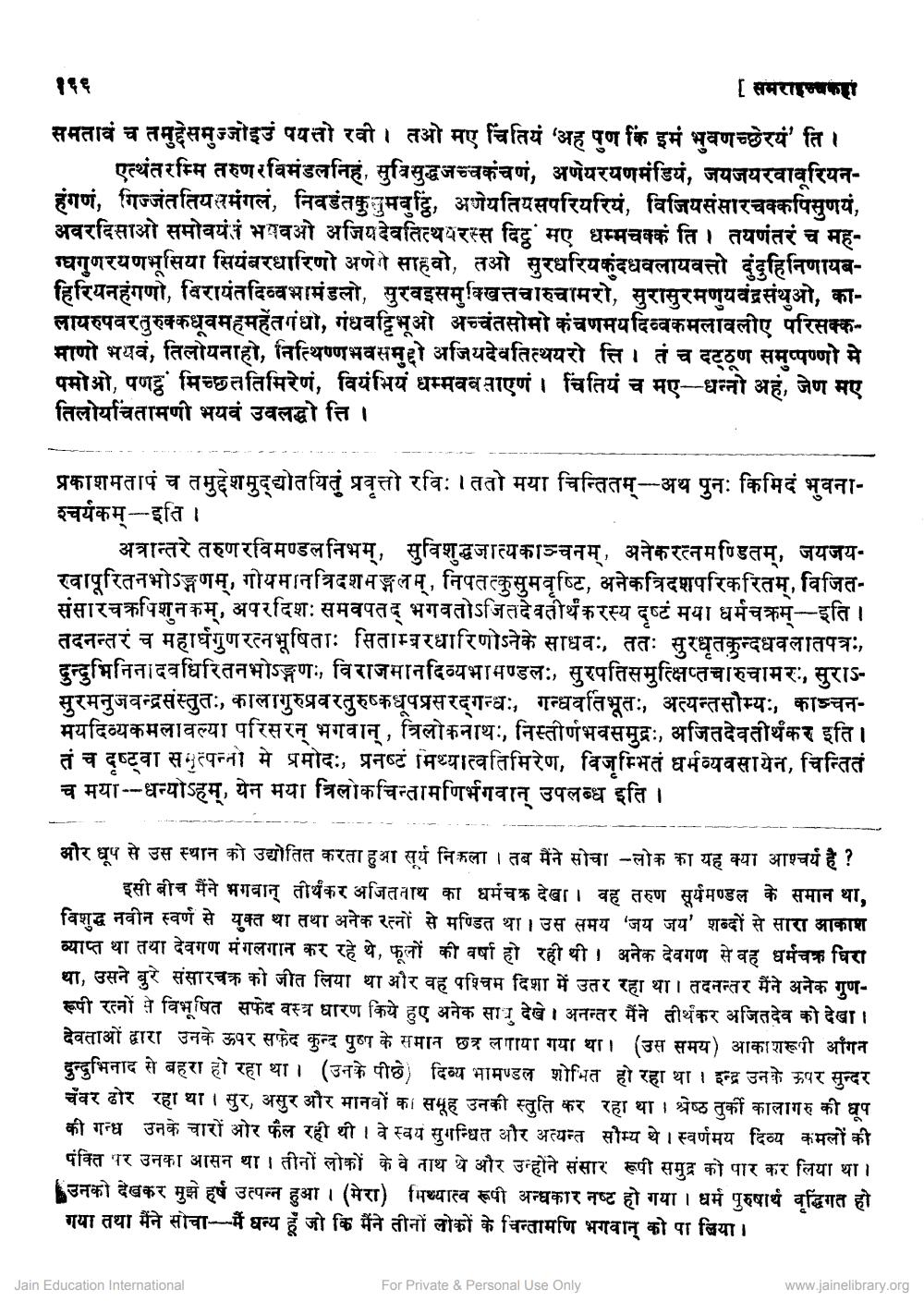________________
१६६
[ समराइज्यका
समतावं च तमुद्देसमुज्जोइउं पयतो रवी । तओ मए चितिथं 'अह पुण कि इमं भुवणच्छेरयं' ति ।
एत्थंतरम्मि तरुण रविमंडलनिहं, सुविसुद्ध जच्चकंचणं, अणेयरयणमंडियं, जयजयरवावूरियनहंगणं, गिज्जंततिय समंगलं, निवडंतकुसुमबुद्धि, अणेयतियसपरियरियं विजियसंसारचक्कपिसुणयं, अवरदिसाओ समोवयं तं भगवओ अजियदेवतित्थवरस्स दिट्ठ मए धम्मचक्कं ति । तयणंतरं च महगुणरयणभूसिया सियंबरधारिणो अगे साहवो, तओ सुरधरियकुंदधवलायवत्तो दुंदुहिनिणायब - हिरियनहंगणो, विरायंत दिव्वभामंडलो, सुरवइसमुक्खित्तचारुचामरो, सुरासुर मणुयवंद्रसंधुओ, कालायरुपवर तुरुक्क धूव महमहंत गंधो, गंधवट्टिभूओ अच्चतसोमो कंचणमय दिव्वकमलावलीए परिसक्कमाणो भयवं, तिलोयनाहो, नित्थिण्णभवसमुद्दो अजियदेवतित्थयरोति । तं च दट्ठूण समुप्पण्णो मे पमोओ, पणट्ठ मिच्छत तिमिरेणं, वियंभियं धम्मववताएणं । चितियं च मए-धन्नो अहं, जेण मए तिलोर्याचतामणी भयवं उवलद्धो त्ति |
प्रकाशमतापं च तमुद्देशमुद्द्द्योतयितुं प्रवृत्तो रविः । ततो मया चिन्तितम् - अथ पुनः किमिदं भुवनाश्चर्यकम् - इति ।
अत्रान्तरे तरुण रविमण्डलनिभम्, सुविशुद्ध जात्यकाञ्चनम्, अनेकरत्नमण्डितम्, जयजयपूरित भोऽङ्गणम्, गोयमानत्रिदशमङ्गलम्, निपतत्कुसुमवृष्टि, अनेकत्रिदशपरिकरितम्, विजितसंसारचक्रपिशुनकम्, अपरदिशः समवपतद् भगवतोऽजितदेवतीर्थंकरस्य दृष्टं मया धर्मचक्रम् - इति । तदनन्तरं च महार्घ गुणरत्नभूषिताः सिताम्बरधारिणोऽनेके साधवः, ततः सुरधृतकुन्दधवलातपत्रः, दुन्दुभिनिनादवधिरितनभोऽङ्गणः, विराजमानदिव्यभामण्डलः, सुरपतिसमुत्क्षिप्तचारुचामरः, सुरा - सुरमनुजवन्द्रसंस्तुतः, कालागुरुप्रवरतुरुष्क धूपप्रस रद्गन्धः, गन्धवर्तिभूतः, अत्यन्तसौम्यः, काञ्चनमयदिव्य कमलावल्या परिसरन् भगवान्, त्रिलोकनाथः, निस्तीर्णभवसमुद्रः, अजितदेवतीर्थंकर इति । तं च दृष्ट्वा समुत्पन्नो में प्रमोदः, प्रनष्टं मिथ्यात्वतिमिरेण, विजृम्भितं धर्मव्यवसायेन, चिन्तितं च मया -- धन्योऽहम् येन मया त्रिलोकचिन्तामणिर्भगवान् उपलब्ध इति ।
और धूप
से उस स्थान को उद्योतित करता हुआ सूर्य निकला । तब मैंने सोचा -लोक का यह क्या आश्चर्य है ? इसी बीच मैंने भगवान् तीर्थंकर अजितनाथ का धर्मचक्र देखा । वह तरुण सूर्यमण्डल के समान था, विशुद्ध नवीन स्वर्ण से युक्त था तथा अनेक रत्नों से मण्डित था । उस समय 'जय जय' शब्दों से सारा आकाश व्याप्त था तथा देवगण मंगलगान कर रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। अनेक देवगण से वह धर्मचक्र घिरा था, उसने बुरे संसारचक्र को जीत लिया था और वह पश्चिम दिशा में उतर रहा था । तदनन्तर मैंने अनेक गुणरूपी रत्नों से विभूषित सफेद वस्त्र धारण किये हुए अनेक साधु देखे । अनन्तर मैंने तीर्थंकर अजितदेव को देखा । देवताओं द्वारा उनके ऊपर सफेद कुन्द पुष्प के समान छत्र लगाया गया था। ( उस समय ) आकाशरूपी आँगन दुन्दुभिनाद से बहरा हो रहा था । (उनके पीछे ) दिव्य भामण्डल शोभित हो रहा था । इन्द्र उनके ऊपर सुन्दर चंवर ढोर रहा था। सुर, असुर और मानवों का समूह उनकी स्तुति कर रहा था । श्रेष्ठ तुर्की कालागरू की धूप की गन्ध उनके चारों ओर फैल रही थी । वे स्वयं सुगन्धित और अत्यन्त सौम्य थे । स्वर्णमय दिव्य कमलों की पंक्ति पर उनका आसन था। तीनों लोकों के वे नाथ थे और उन्होंने संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया था । उनको देखकर मुझे हर्ष उत्पन्न हुआ । ( मेरा मिथ्यात्व रूपी अन्धकार नष्ट हो गया । धर्म पुरुषार्थ वृद्धिगत हो गया तथा मैंने सोचा --- मैं धन्य हूँ जो कि मैंने तीनों लोकों के चिन्तामणि भगवान् को पा लिया ।
1
)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org