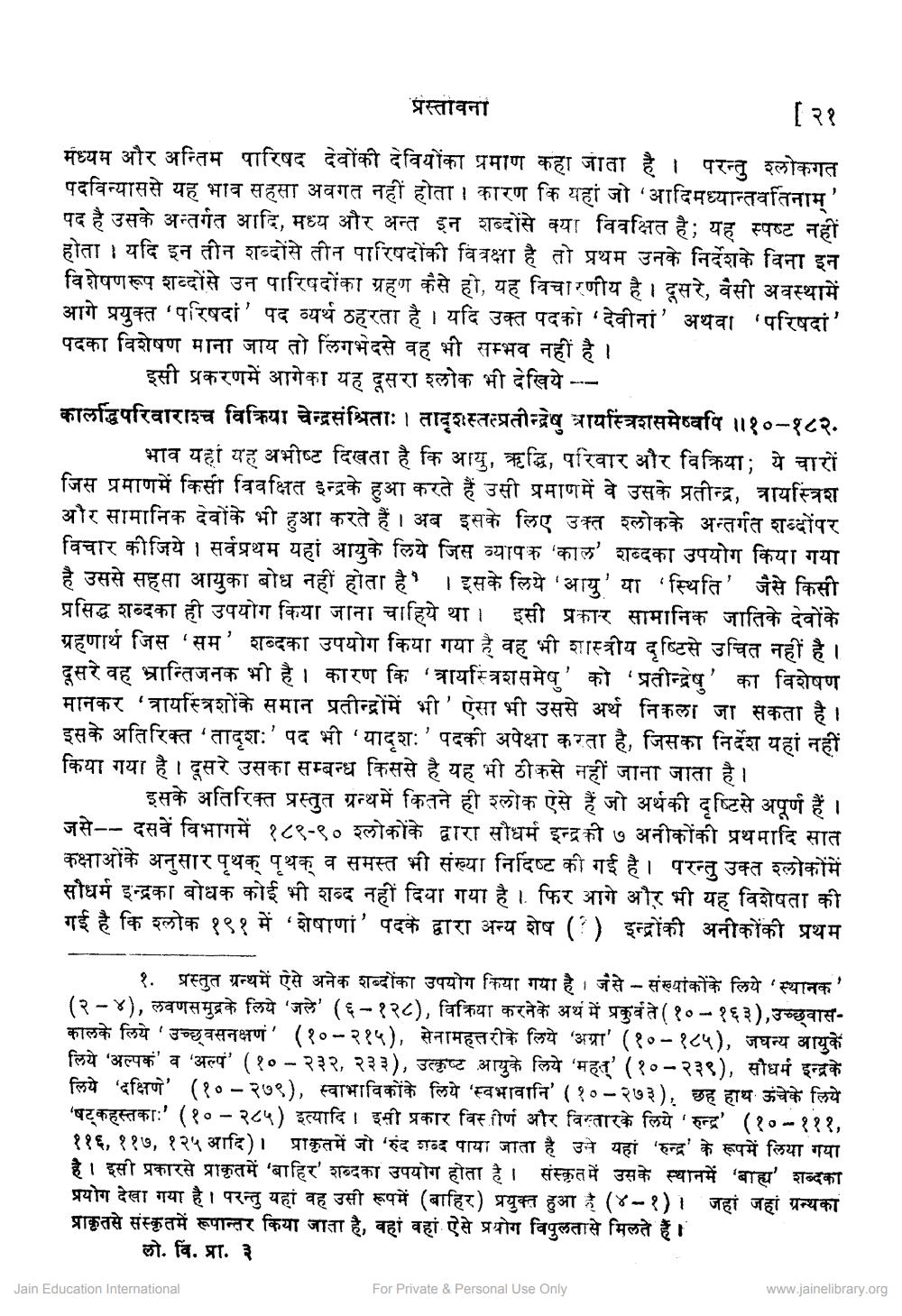________________
प्रस्तावना
[ २१
मध्यम और अन्तिम पारिषद देवोंकी देवियोंका प्रमाण कहा जाता है । परन्तु श्लोकगत पदविन्यास से यह भाव सहसा अवगत नहीं होता। कारण कि यहां जो 'आदिमध्यान्तवर्तिनाम् ' पद है उसके अन्तर्गत आदि, मध्य और अन्त इन शब्दोंसे क्या विवक्षित है; यह स्पष्ट नहीं होता । यदि इन तीन शब्दोंसे तीन पारिषदोंकी विवक्षा है तो प्रथम उनके निर्देशके विना इन विशेषणरूप शब्दों से उन पारिषदोंका ग्रहण कैसे हो, यह विचारणीय है । दूसरे, वैसी अवस्थामें आगे प्रयुक्त 'परिषदां' पद व्यर्थ ठहरता है । यदि उक्त पदको 'देवीनां' अथवा 'परिषदां' पदका विशेषण माना जाय तो लिंगभेदसे वह भी सम्भव नहीं है ।
इसी प्रकरणमें आगेका यह दूसरा श्लोक भी देखिये -
कार्लाद्धपरिवाराश्च विक्रिया चेन्द्रसंश्रिताः । तादृशस्तत्प्रतीन्द्रेषु त्रायस्त्रशसमेष्वपि ॥१०- १८२. भाव यहां यह अभीष्ट दिखता है कि आयु, ऋद्धि, परिवार और विक्रिया; ये चारों जिस प्रमाण में किसी विवक्षित इन्द्रके हुआ करते हैं उसी प्रमाणमें वे उसके प्रतीन्द्र, त्रायस्त्रिश और सामानिक देवोंके भी हुआ करते हैं। अब इसके लिए उक्त श्लोकके अन्तर्गत शब्दोंपर विचार कीजिये । सर्वप्रथम यहां आयुके लिये जिस व्यापक 'काल' शब्दका उपयोग किया गया है उससे सहसा आयुका बोध नहीं होता है । इसके लिये 'आयु' या 'स्थिति' जैसे किसी प्रसिद्ध शब्दका ही उपयोग किया जाना चाहिये था । इसी प्रकार सामानिक जातिके देवोंके ग्रहणार्थ जिस 'सम' शब्दका उपयोग किया गया है वह भी शास्त्रीय दृष्टिसे उचित नहीं है । दूसरे वह भ्रान्तिजनक भी है। कारण कि ' त्रायस्त्रिशसमेषु' को 'प्रतीन्द्रेषु' का विशेषण मानकर ' त्रास्त्रिशोंके समान प्रतीन्द्रोंमें भी ' ऐसा भी उससे अर्थ निकला जा सकता है । इसके अतिरिक्त ' तादृश: ' पद भी 'यादृश: ' पदकी अपेक्षा करता है, जिसका निर्देश यहां नहीं किया गया है । दूसरे उसका सम्बन्ध किससे है यह भी ठीकसे नहीं जाना जाता है ।
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थ में कितने ही श्लोक ऐसे हैं जो अर्थकी दृष्टिसे अपूर्ण हैं । जसे -- दसवें विभागमें १८९-९० श्लोकोंके द्वारा सौधर्म इन्द्रकी ७ अनीकोंकी प्रथमादि सात कक्षाओं के अनुसार पृथक् पृथक् व समस्त भी संख्या निर्दिष्ट की गई है । परन्तु उक्त श्लोकों में सौधर्म इन्द्रका बोधक कोई भी शब्द नहीं दिया गया है । फिर आगे और भी यह विशेषता की गई है कि श्लोक १९१ में 'शेषाणां' पदके द्वारा अन्य शेष ( ? ) इन्द्रोंकी अनीकों की प्रथम
"
१. प्रस्तुत ग्रन्थ में ऐसे अनेक शब्दोंका उपयोग किया गया है। जैसे - संख्यांकोंके लिये 'स्थानक ' ( २ - ४ ), लवणसमुद्रके लिये 'जले' (६- १२८), विक्रिया करनेके अर्थ में प्रकुर्वते ( १० - १६३), उच्छ्वासकालके लिये 'उच्छ्वसनक्षणं' (१०-२१५), सेनामहत्तरीके लिये 'अग्रा' (१०- १८५), जघन्य आयुके लिये 'अल्पक' व 'अल्प' (१०-२३२, २३३), उत्कृष्ट आयुके लिये ' महत्' ( १०-२३९), सौधर्म इन्द्रके लिये 'दक्षिणे' (१०- २७९), स्वाभाविकोंके लिये 'स्वभावानि' ( १०- २७३ ), छह हाथ ऊंचेके लिये 'षट् कहस्तका: ' ( १०- २८५ ) इत्यादि । इसी प्रकार विस्तीर्ण और विस्तारके लिये ' रुन्द्र' (१०-१११, ११६, १७, १२५ आदि) । प्राकृतमें जो 'रुंद शब्द पाया जाता है उसे यहां 'रुन्द्र' के रूपमें लिया गया है । इसी प्रकारसे प्राकृत में 'बाहिर' शब्दका उपयोग होता है । संस्कृत में उसके स्थानमें 'बाह्य' शब्दका प्रयोग देखा गया है । परन्तु यहां वह उसी रूपमें (बाहिर) प्रयुक्त हुआ है ( ४- १) । जहां जहां ग्रन्थका प्राकृतसे संस्कृतमें रूपान्तर किया जाता है, वहां वहां ऐसे प्रयोग विपुलतासे मिलते हैं।
लो. वि. प्रा. ३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org