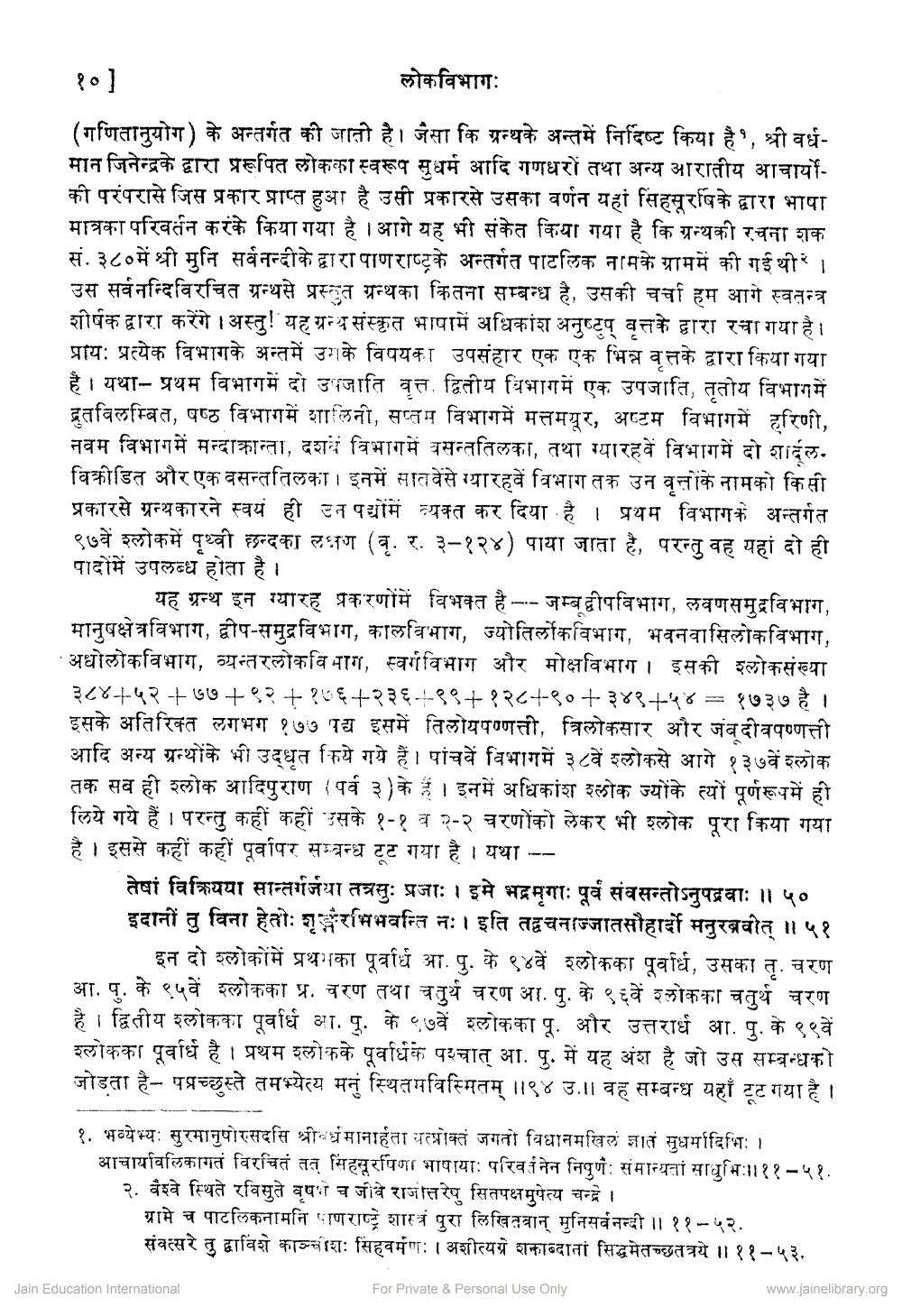________________
१०]
लोकविभागः (गणितानुयोग) के अन्तर्गत की जाती है। जैसा कि ग्रन्थके अन्तमें निर्दिष्ट किया है', श्री वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा प्ररूपित लोकका स्वरूप सुधर्म आदि गणधरों तथा अन्य आरातीय आचार्योकी परंपरासे जिस प्रकार प्राप्त हुआ है उसी प्रकारसे उसका वर्णन यहां सिंहसूषिके द्वारा भाषा मात्रका परिवर्तन करके किया गया है । आगे यह भी संकेत किया गया है कि ग्रन्थकी रचना शक सं. ३८०में श्री मुनि सर्वनन्दीके द्वारा पाणराष्ट्र के अन्तर्गत पाटलिक नामके ग्राममें की गई थी । उस सर्वनन्दिविरचित ग्रन्थसे प्रस्तुत ग्रन्थका कितना सम्बन्ध है, उसकी चर्चा हम आगे स्वतन्त्र शीर्षक द्वारा करेंगे । अस्तु! यह ग्रन्य संस्कृत भाषामें अधिकांश अनुष्टुप् वृत्तके द्वारा रचा गया है। प्रायः प्रत्येक विभागके अन्तमें उगके विषयका उपसंहार एक एक भिन्न वृत्तके द्वारा किया गया है। यथा- प्रथम विभागमें दो उपजाति वृत्त, द्वितीय विभाग में एक उपजाति, तृतीय विभागमें द्रुतविलम्बित, षष्ठ विभागमें शालिनी, सप्तम विभागमें मत्तमयुर, अष्टम विभागमें हरिणी, नवम विभागमें मन्दाक्रान्ता, दश विभागमें वसन्ततिलका, तथा ग्यारहवें विभागमें दो शार्दूल. विक्रीडित और एक वसन्ततिलका। इनमें सातवेंसे ग्यारहवें विभाग तक उन वृत्तोंके नामको किसी प्रकारसे ग्रन्थकारने स्वयं ही उन पद्योंमें व्यक्त कर दिया है । प्रथम विभागके अन्तर्गत ९७वें श्लोकमें पृथ्वी छन्दका लक्षण (वृ. र. ३-१२४) पाया जाता है, परन्तु वह यहां दो ही पादोंमें उपलब्ध होता है।
यह ग्रन्थ इन ग्यारह प्रकरणोंमें विभक्त है --- जम्ब द्वीपविभाग, लवणसमुद्रविभाग, मानुषक्षेत्रविभाग, द्वीप-समुद्र विभाग, कालविभाग, ज्योतिर्लोकविभाग, भवनवासिलोकविभाग, 'अधोलोकविभाग, व्यन्तरलोकवि भाग, स्वर्गविभाग और मोक्षविभाग। इसकी श्लोकसंख्या ३८४--५२ -- ७७ +९२ + १७६+२३६.-९९+ १२८५-९० +३४९-+-५४ = १७३७ है । इसके अतिरिक्त लगभग १७७ पद्य इसमें तिलोयपण्णत्ती, त्रिलोकसार और जंब दीवपण्णत्ती आदि अन्य ग्रन्थोंके भी उद्धृत किये गये हैं। पांचवें विभागमें ३८वें श्लोकसे आगे १३७वें श्लोक तक सब ही श्लोक आदिपुराण (पर्व ३) के हैं। इनमें अधिकांश श्लोक ज्योंके त्यों पूर्णरूपमें ही लिये गये हैं । परन्तु कहीं कहीं उसके १-१ व २-२ चरणोंको लेकर भी श्लोक पूरा किया गया है। इससे कहीं कहीं पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया है । यथा ---
तेषां विक्रियया सान्तर्गर्जया तत्रसुः प्रजाः । इमे भद्रमृगाः पूर्व संवसन्तोऽनुपद्रवाः ॥ ५० इदानीं तु विना हेतोः शृङ्गरभिभवन्ति नः। इति तद्वचनाज्जातसौहार्दो मनुरब्रवीत् ॥ ५१
इन दो श्लोकों में प्रथम का पूर्वार्ध आ. पु. के ९४वें श्लोकका पूर्वार्ध, उसका तृ. चरण आ. पु. के ९५वें श्लोकका प्र. चरण तथा चतुर्थ चरण आ. पु. के ९६वें श्लोकका चतुर्थ चरण है । द्वितीय श्लोकका पूर्वार्ध आ. पु. के ९७वें श्लोकका पू. और उत्तरार्ध आ. पु. के ९९वें श्लोकका पूर्वार्ध है । प्रथम श्लोकके पूर्वार्धके पश्चात् आ. पु. में यह अंश है जो उस सम्बन्धको जोडता है- पप्रच्छुस्ते तमभ्येत्य मनुं स्थितमविस्मितम् ।।९४ उ.।। वह सम्बन्ध यहाँ टूट गया है ।
१. भव्येभ्यः सुरमानुषोरसदसि श्रीवर्धमानार्हता यत्प्रोक्तं जगतो विधानमखिलं ज्ञातं सुधर्मादिभिः । आचार्यावलिकागतं विरचितं तत् सिंहसूरपिणा भाषायाः परिवर्तनेन निपुणः संमान्यतां साधुभिः।।११ -५१. २. वैश्वे स्थिते रविसुते वृषणे च जीवे राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । ग्रामे च पाटलिकनामनि राणराष्ट्रे शास्त्रं पुरा लिखितवान् मुनिसर्वनन्दी ।। ११ - ५२. संवत्सरे तु द्वाविशे काञ्चाशः सिंहवर्मणः । अशीत्यग्रेशकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ।। ११-५३.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org