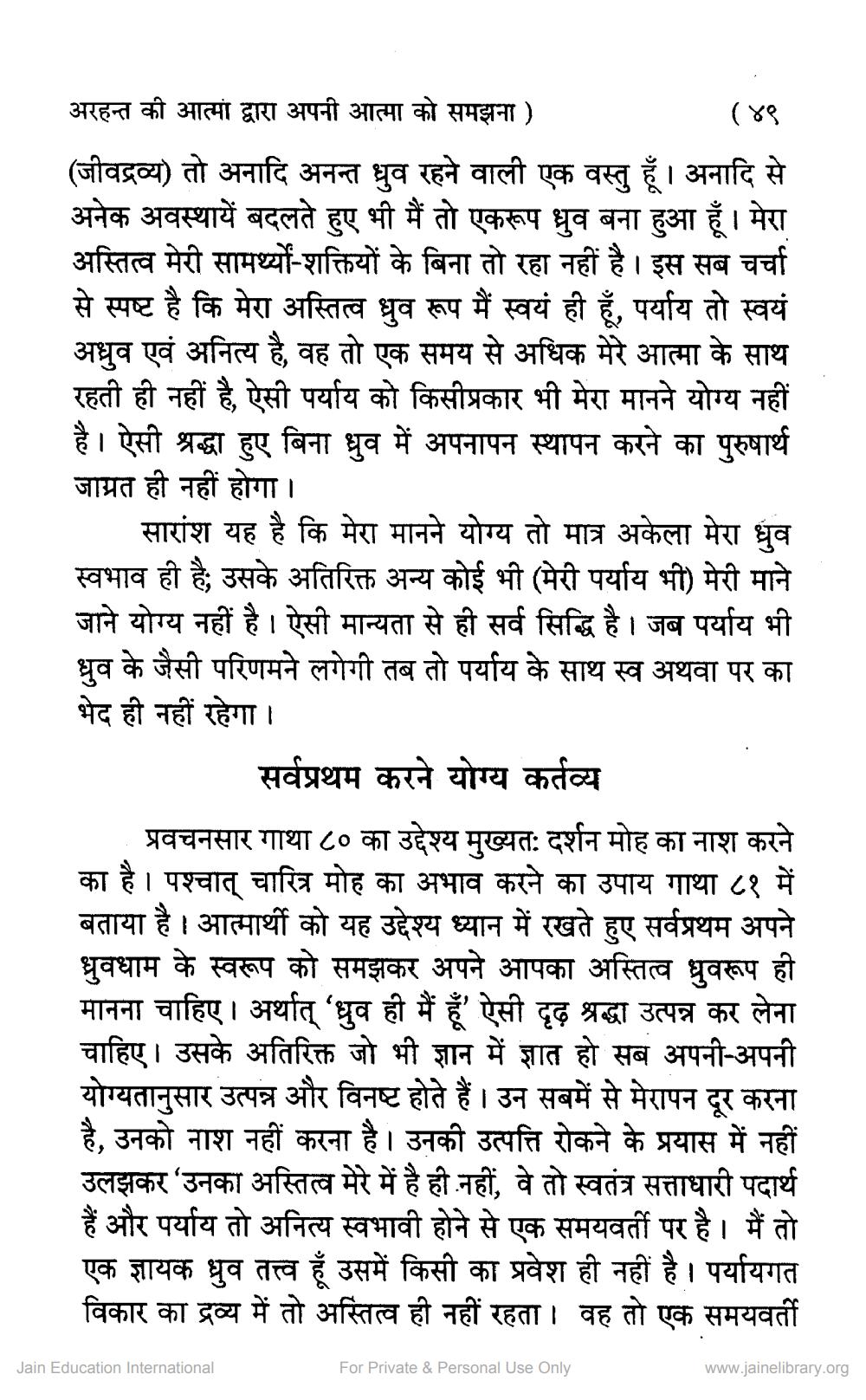________________
अरहन्त की आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को समझना )
(४९ (जीवद्रव्य) तो अनादि अनन्त ध्रुव रहने वाली एक वस्तु हूँ। अनादि से अनेक अवस्थायें बदलते हुए भी मैं तो एकरूप ध्रुव बना हुआ हूँ। मेरा अस्तित्व मेरी सामर्थ्यो-शक्तियों के बिना तो रहा नहीं है। इस सब चर्चा से स्पष्ट है कि मेरा अस्तित्व ध्रुव रूप मैं स्वयं ही हूँ, पर्याय तो स्वयं अध्रुव एवं अनित्य है, वह तो एक समय से अधिक मेरे आत्मा के साथ रहती ही नहीं है, ऐसी पर्याय को किसीप्रकार भी मेरा मानने योग्य नहीं है। ऐसी श्रद्धा हुए बिना ध्रुव में अपनापन स्थापन करने का पुरुषार्थ जाग्रत ही नहीं होगा।
सारांश यह है कि मेरा मानने योग्य तो मात्र अकेला मेरा ध्रुव स्वभाव ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी (मेरी पर्याय भी) मेरी माने जाने योग्य नहीं है। ऐसी मान्यता से ही सर्व सिद्धि है। जब पर्याय भी ध्रुव के जैसी परिणमने लगेगी तब तो पर्याय के साथ स्व अथवा पर का भेद ही नहीं रहेगा।
सर्वप्रथम करने योग्य कर्तव्य प्रवचनसार गाथा ८० का उद्देश्य मुख्यत: दर्शन मोह का नाश करने का है। पश्चात् चारित्र मोह का अभाव करने का उपाय गाथा ८१ में बताया है। आत्मार्थी को यह उद्देश्य ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम अपने ध्रुवधाम के स्वरूप को समझकर अपने आपका अस्तित्व ध्रुवरूप ही मानना चाहिए। अर्थात् 'ध्रुव ही मैं हूँ' ऐसी दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो भी ज्ञान में ज्ञात हो सब अपनी-अपनी योग्यतानुसार उत्पन्न और विनष्ट होते हैं। उन सबमें से मेरापन दूर करना है, उनको नाश नहीं करना है। उनकी उत्पत्ति रोकने के प्रयास में नहीं उलझकर 'उनका अस्तित्व मेरे में है ही नहीं, वे तो स्वतंत्र सत्ताधारी पदार्थ हैं और पर्याय तो अनित्य स्वभावी होने से एक समयवर्ती पर है। मैं तो एक ज्ञायक ध्रुव तत्त्व हूँ उसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। पर्यायगत विकार का द्रव्य में तो अस्तित्व ही नहीं रहता। वह तो एक समयवर्ती
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org