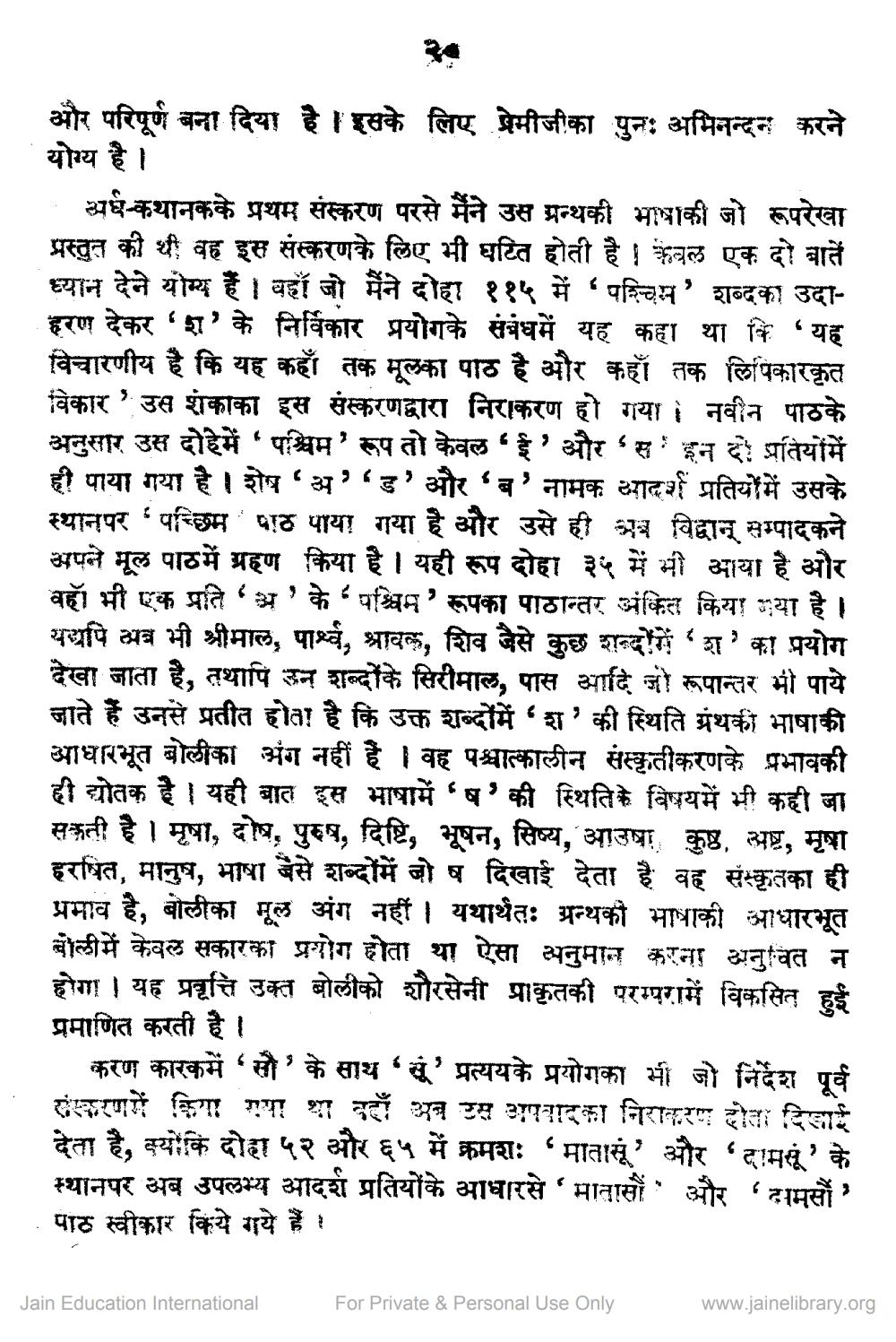________________
और परिपूर्ण बना दिया है। इसके लिए प्रेमीजीका पुनः अभिनन्दन करने योग्य है। - अर्घ-कथानकके प्रथम संस्करण परसे मैंने उस ग्रन्थकी भाषाकी जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी वह इस संस्करणके लिए भी घटित होती है। केवल एक दो बातें ध्यान देने योग्य हैं । वहाँ जो मैंने दोहा ११५ में 'पश्चिम' शब्दका उदाहरण देकर 'श' के निर्विकार प्रयोगके संबंधमें यह कहा था कि यह विचारणीय है कि यह कहाँ तक मूलका पाठ है और कहाँ तक लिपिकारकृत विकार' उस शंकाका इस संस्करणद्वारा निराकरण हो गया। नवीन पाठके अनुसार उस दोहेमें 'पश्चिम' रूप तो केवल 'ई' और 'स इन दो प्रतियोंमें ही पाया गया है। शेष 'अ''ड' और 'ब' नामक आदर्श प्रतियों में उसके स्थानपर 'पच्छिम पाठ पाया गया है और उसे ही अब विद्वान सम्पादकने अपने मूल पाठमें ग्रहण किया है। यही रूप दोहा ३५ में भी आया है और वहाँ भी एक प्रति 'अ' के 'पश्चिम' रूपका पाठान्तर अंकित किया गया है । यद्यपि अब भी श्रीमाल, पार्श्व, श्रावल, शिव जैसे कुछ शब्दों में 'श' का प्रयोग देखा जाता है, तथापि उन शब्दोंके सिरीमाल, पास आदि जो रूपान्तर भी पाये जाते हैं उनसे प्रतीत होता है कि उक्त शब्दोंमें 'श' की स्थिति ग्रंथकी भाषाकी आधारभूत बोलीका अंग नहीं है । वह पश्चात्कालीन संस्कृतीकरणके प्रभावकी ही द्योतक है। यही बात इस भाषामें 'ष' की स्थिति के विषयमें भी कही जा सकती है। मृषा, दोष, पुरुष, दिष्टि, भूषन, सिष्य, आउषा कुष्ठ, अष्ट, मृषा हरषित, मानुष, भाषा बसे शब्दोंमें जो ष दिखाई देता है वह संस्कृतका ही प्रमाव है, बोलीका मूल अंग नहीं । यथार्थतः अन्थको भाषाकी आधारभूत बोली में केवल सकारका प्रयोग होता था ऐसा अनुमान करना अनुचित न होगा। यह प्रवृत्ति उक्त बोलीको शौरसेनी प्राकृतकी परम्परामें विकसित हुई प्रमाणित करती है।
करण कारकमें 'सौ' के साथ 'सू' प्रत्ययके प्रयोगका भी जो निर्देश पूर्व संस्करण में किया गया था वहाँ अब उस अपवादका निराकरण होता दिखाई देता है, क्योंकि दोहा ५२ और ६५ में क्रमशः 'मातासू' और 'दामसू' के स्थानपर अब उपलभ्य आदर्श प्रतियोंके आधारसे 'मातासौं' और 'दामसौं' पाठ स्वीकार किये गये हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org