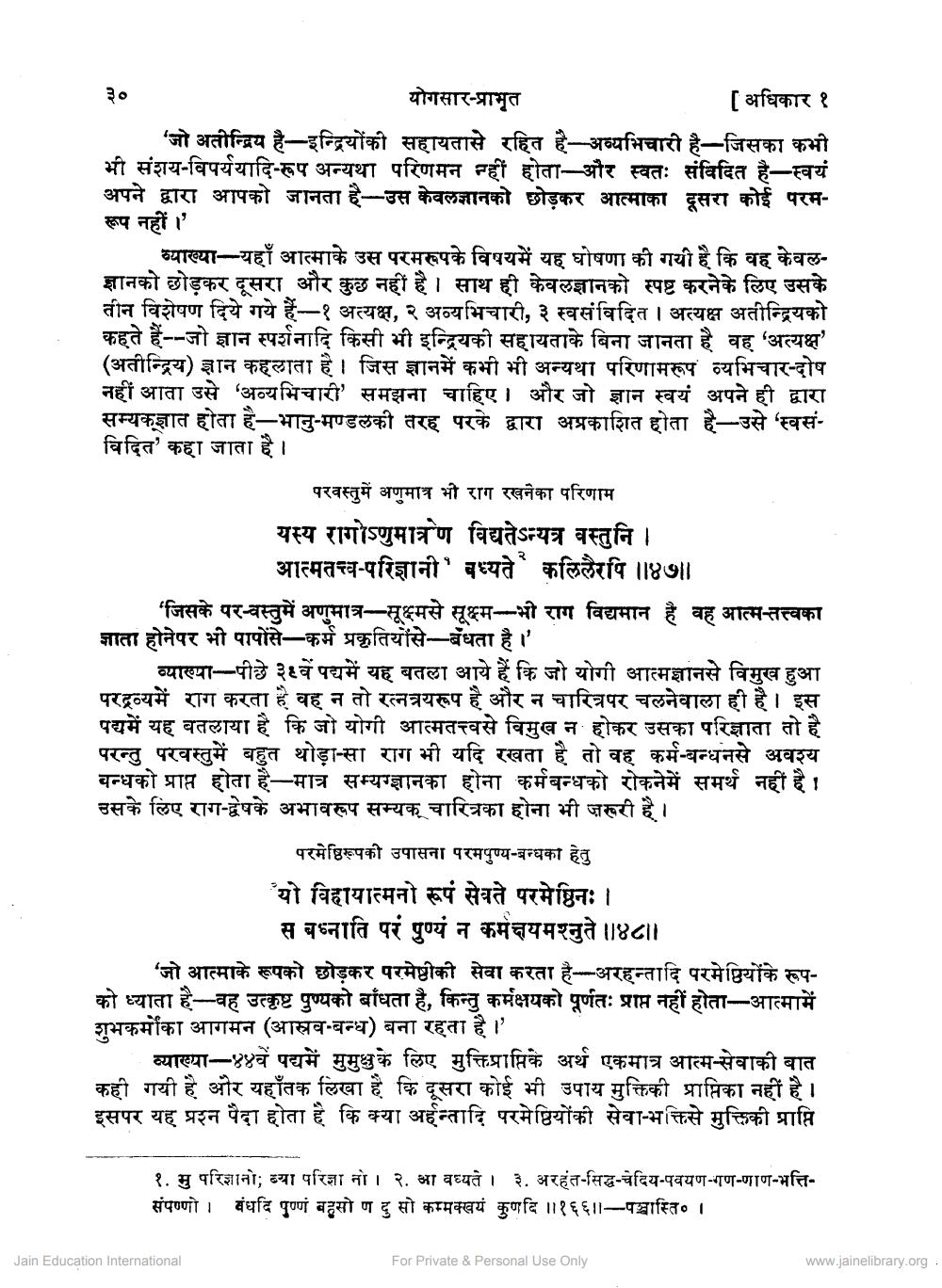________________
योगसार-प्राभूत
[ अधिकार १ 'जो अतीन्द्रिय है-इन्द्रियोंकी सहायतासे रहित है-अव्यभिचारी है-जिसका कभी भी संशय-विपर्ययादि-रूप अन्यथा परिणमन नहीं होता और स्वतः संविदित है-स्वयं अपने द्वारा आपको जानता है-उस केवलज्ञानको छोड़कर आत्माका दूसरा कोई परमरूप नहीं।'
व्याख्या-यहाँ आत्माके उस परमरूपके विषयमें यह घोषणा की गयी है कि वह केवलज्ञानको छोड़कर दूसरा और कुछ नहीं है। साथ ही केवलज्ञानको स्पष्ट करनेके लिए उसके तीन विशेषण दिये गये हैं-१ अत्यक्ष, २ अव्यभिचारी, ३ स्वसंविदित । अत्यक्ष अतीन्द्रियको कहते है--जो ज्ञान स्पर्शनादि किसी भी इन्द्रियकी सहायताके बिना जानता है वह 'अत्यक्ष' (अतीन्द्रिय) ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञानमें कभी भी अन्यथा परिणामरूप व्यभिचार-दोष नहीं आता उसे 'अव्यभिचारी' समझना चाहिए। और जो ज्ञान स्वयं अपने ही द्वारा सम्यकज्ञात होता है-भानु-मण्डलकी तरह परके द्वारा अप्रकाशित होता है-उसे 'स्वसंविदित' कहा जाता है।
परवस्तुमें अणुमात्र भी राग रखनैका परिणाम यस्य रागोऽणुमात्रण विद्यतेऽन्यत्र वस्तुनि ।
आत्मतत्त्व-परिज्ञानी' बध्यते' कलिलैरपि ॥४७॥ 'जिसके पर-वस्तुमें अणुमात्र-सूक्ष्मसे सूक्ष्म-भी राग विद्यमान है वह आत्म-तत्त्वका ज्ञाता होनेपर भी पापोंसे-कर्म प्रकृतियोंसे-बंधता है।'
व्याख्या-पीछे ३६वें पद्यमें यह बतला आये हैं कि जो योगी आत्मज्ञानसे विमुख हुआ परद्रव्यमें राग करता है वह न तो रत्नत्रयरूप है और न चारित्रपर चलनेवाला ही है। इस पद्यमें यह बतलाया है कि जो योगी आत्मतत्त्वसे विमुख न होकर उसका परिज्ञाता तो है परन्तु परवस्तुमें बहुत थोड़ा-सा राग भी यदि रखता है तो वह कर्म-बन्धनसे अवश्य वन्धको प्राप्त होता है-मात्र सम्यग्ज्ञानका होना कर्मबन्धको रोकनेमें समर्थ नहीं है। उसके लिए राग-द्वेषके अभावरूप सम्यक चारित्रका होना भी जरूरी है।
परमेष्ठिरूपकी उपासना परमपुण्य-बन्धका हेतु 'यो विहायात्मनो रूपं सेवते परमेष्ठिनः ।
स बध्नाति परं पुण्यं न कर्मक्षयमश्नुते ॥४८॥ 'जो आत्माके रूपको छोड़कर परमेष्ठीको सेवा करता है-अरहन्तादि परमेष्ठियोंके रूपको ध्याता है-वह उत्कृष्ट पुण्यको बाँधता है, किन्तु कर्मक्षयको पूर्णतः प्राप्त नहीं होता-आत्मामें शुभकर्मोका आगमन (आस्रव-बन्ध) बना रहता है।'
व्याख्या-४४वें पद्यमें मुमुक्षु के लिए मुक्तिप्राप्तिके अर्थ एकमात्र आत्म-सेवाकी बात कही गयी है और यहाँतक लिखा है कि दूसरा कोई भी उपाय मुक्तिकी प्राप्तिका नहीं है। इसपर यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या अर्हन्तादि परमेष्ठियोंकी सेवा-भक्तिसे मुक्तिकी प्राप्ति
१. मु परिज्ञानो; व्या परिज्ञा नो। २. आ वध्यते । ३. अरहंत-सिद्ध-चेदिय-पवयण-गण-णाण-भत्तिसंपण्णो। बंधदि पुण्णं बहुसो ण दु सो कम्मक्खयं कुणादि ॥१६६।।-पञ्चास्ति ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org .