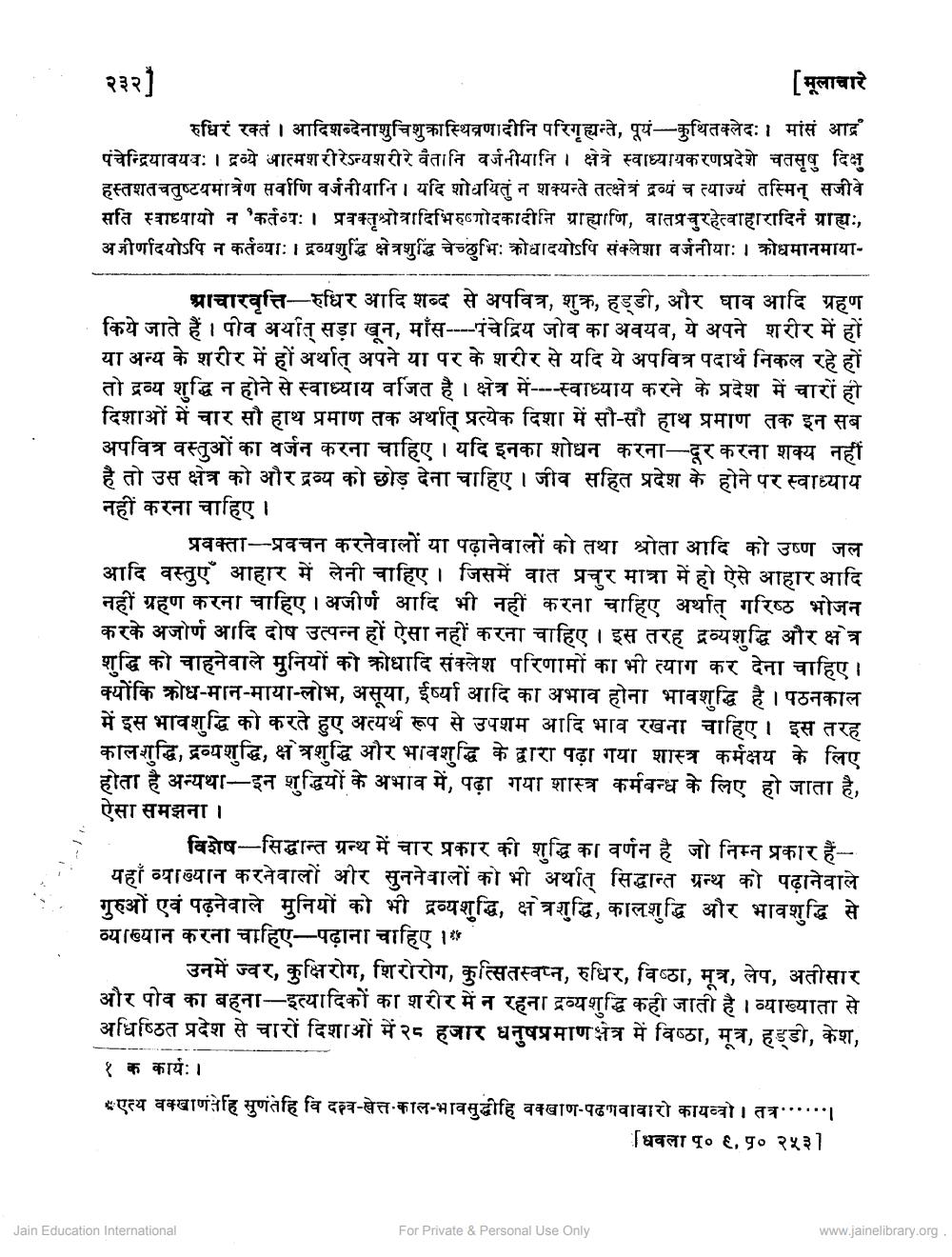________________
२३२]
[मूलाचारे रुधिरं रक्तं । आदिशब्देनाशुचिशुक्रा स्थिवणादीनि परिगृह्यन्ते, पूयं-कथितक्लेदः। मांसं आद्र पंचेन्द्रियावयवः । द्रव्ये आत्मशरीरेऽन्यशरीरे वैतानि वर्जनीयानि। क्षेत्रे स्वाध्यायकरणप्रदेशे चतसष दिक्ष हस्तशतचतुष्टयमात्रेण सर्वाणि वर्जनीयानि । यदि शोधयितुं न शक्यन्ते तत्क्षेत्रं द्रव्यं च त्याज्यं तस्मिन सजीवे सति स्वाध्यायो न 'कर्तव्यः । प्रवक्तृश्रोत्रादिभिरुष्णोदकादीनि ग्राह्याणि, वातप्रचुरहेत्वाहारादिर्न ग्राह्यः, अजीर्णादयोऽपि न कर्तव्याः । द्रव्यशुद्धि क्षेत्रशुद्धि चेच्छुभिः क्रोधादयोऽपि संक्लेशा वर्जनीयाः । क्रोधमानमाया
प्राचारवृत्ति-रुधिर आदि शब्द से अपवित्र, शुक्र, हड्डी, और घाव आदि ग्रहण किये जाते हैं । पीव अर्थात् सड़ा खून, माँस----पंचेद्रिय जोव का अवयव, ये अपने शरीर में हों या अन्य के शरीर में हो अर्थात् अपने या पर के शरीर से यदि ये अपवित्र पदार्थ निकल रहे हों तो द्रव्य शुद्धि न होने से स्वाध्याय वजित है । क्षेत्र में----स्वाध्याय करने के प्रदेश में चारों ही दिशाओं में चार सौ हाथ प्रमाण तक अर्थात् प्रत्येक दिशा में सौ-सौ हाथ प्रमाण तक इन सब अपवित्र वस्तुओं का वर्जन करना चाहिए। यदि इनका शोधन करना-दूर करना शक्य नहीं है तो उस क्षेत्र को और द्रव्य को छोड़ देना चाहिए। जीव सहित प्रदेश के होने पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।
प्रवक्ता--प्रवचन करनेवालों या पढ़ानेवालों को तथा श्रोता आदि को उष्ण जल आदि वस्तुएँ आहार में लेनी चाहिए। जिसमें वात प्रचुर मात्रा में हो ऐसे आहार आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए। अजीर्ण आदि भी नहीं करना चाहिए अर्थात् गरिष्ठ भोजन करके अजोर्ण आदि दोष उत्पन्न हों ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह द्रव्यशुद्धि और क्षेत्र शुद्धि को चाहनेवाले मुनियों को क्रोधादि संक्लेश परिणामों का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि क्रोध-मान-माया-लोभ, असूया, ईर्ष्या आदि का अभाव होना भावशुद्धि है। पठनकाल में इस भावशुद्धि को करते हुए अत्यर्थ रूप से उपशम आदि भाव रखना चाहिए। इस तरह कालशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि और भावशुद्धि के द्वारा पढ़ा गया शास्त्र कर्मक्षय के लिए होता है अन्यथा-इन शुद्धियों के अभाव में, पढ़ा गया शास्त्र कर्मबन्ध के लिए हो जाता है, ऐसा समझना।
विशेष—सिद्धान्त ग्रन्थ में चार प्रकार की शुद्धि का वर्णन है जो निम्न प्रकार हैंयहाँ व्याख्यान करनेवालों और सुननेवालों को भी अर्थात् सिद्धान्त ग्रन्थ को पढ़ानेवाले गुरुओं एवं पढ़नेवाले मुनियों को भी द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, कालशुद्धि और भावशुद्धि से व्याख्यान करना चाहिए-पढ़ाना चाहिए ।
उनमें ज्वर, कुक्षिरोग, शिरोरोग, कुत्सितस्वप्न, रुधिर, विष्ठा, मूत्र, लेप, अतीसार और पोव का बहना-इत्यादिकों का शरीर में न रहना द्रव्यशुद्धि कही जाती है । व्याख्याता से अधिष्ठित प्रदेश से चारों दिशाओं में २८ हजार धनुषप्रमाण क्षेत्र में विष्ठा, मूत्र, हड्डी, केश, १ क कार्यः। *एत्य वक्खाणतेहि सुणतेहि वि दत्व-खेत्त-काल-भावसुद्धीहि वक्खाण-पढणवावारो कायवो। तत्र......।
[धवला पु. ६, पृ० २५३]
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org .