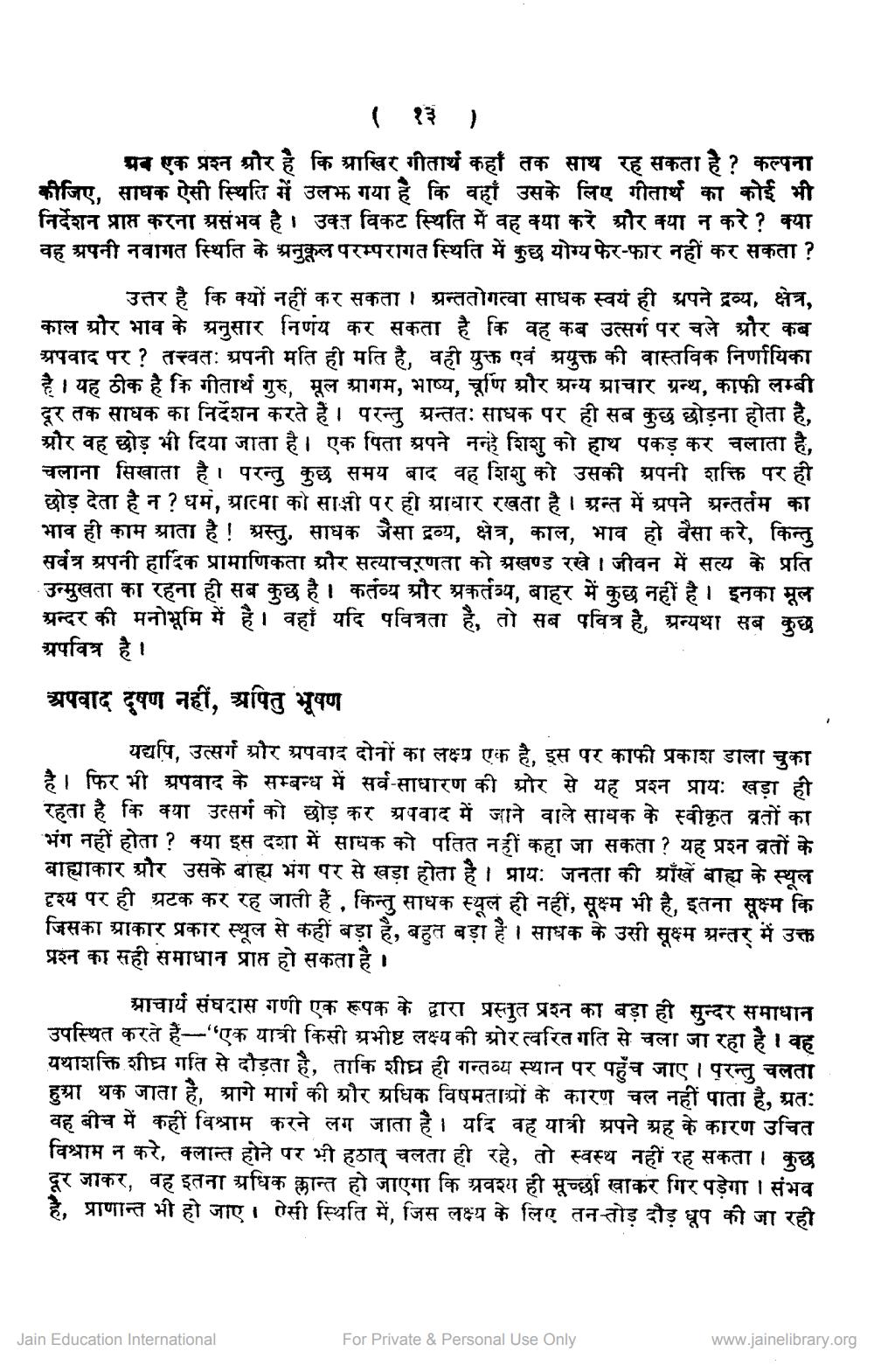________________
अब एक प्रश्न और है कि आखिर गीतार्थ कहाँ तक साथ रह सकता है ? कल्पना कीजिए, साधक ऐसी स्थिति में उलझ गया है कि वहाँ उसके लिए गीतार्थ का कोई भी निर्देशन प्राप्त करना असंभव है। उक्त विकट स्थिति में वह क्या करे और क्या न करे? क्या वह अपनी नवागत स्थिति के अनुकूल परम्परागत स्थिति में कुछ योग्य फेर-फार नहीं कर सकता ?
उत्तर है कि क्यों नहीं कर सकता। अन्ततोगत्वा साधक स्वयं ही अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार निर्णय कर सकता है कि वह कब उत्सर्ग पर चले और कब अपवाद पर ? तत्त्वतः अपनी मति ही मति है, वही युक्त एवं प्रयुक्त की वास्तविक निर्णायिका है। यह ठीक है कि गीतार्थ गुरु, मूल पागम, भाष्य, चूर्णि और अन्य प्राचार ग्रन्थ, काफी लम्बी दूर तक साधक का निर्देशन करते हैं। परन्तु अन्ततः साधक पर ही सब कुछ छोड़ना होता है, और वह छोड़ भी दिया जाता है। एक पिता अपने नन्हे शिशु को हाथ पकड़ कर चलाता है, चलाना सिखाता है। परन्तु कुछ समय बाद वह शिशु को उसकी अपनी शक्ति पर ही छोड़ देता है न ? धर्म, प्रात्मा को साझी पर ही प्राधार रखता है । अन्त में अपने अन्तर्तम का भाव ही काम आता है ! अस्तु, साधक जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हो वैसा करे, किन्तु सर्वत्र अपनी हार्दिक प्रामाणिकता और सत्याचरणता को अखण्ड रखे । जीवन में सत्य के प्रति उन्मुखता का रहना ही सब कुछ है। कर्तव्य और अकर्तव्य, बाहर में कुछ नहीं है। इनका मूल अन्दर की मनोभूमि में है। वहाँ यदि पवित्रता है, तो सब पवित्र है, अन्यथा सब कुछ अपवित्र है। अपवाद दुषण नहीं, अपितु भूषण
यद्यपि, उत्सर्ग और अपवाद दोनों का लक्ष्य एक है, इस पर काफी प्रकाश डाला चुका है। फिर भी अपवाद के सम्बन्ध में सर्व-साधारण की ओर से यह प्रश्न प्रायः खड़ा ही रहता है कि क्या उत्सर्ग को छोड़ कर अपवाद में जाने वाले साधक के स्वीकृत व्रतों का भंग नहीं होता? क्या इस दशा में साधक को पतित नहीं कहा जा सकता? यह प्रश्न व्रतों के बाह्याकार और उसके बाह्य भंग पर से खड़ा होता है। प्रायः जनता की अाँखें बाह्य के स्थूल दृश्य पर ही अटक कर रह जाती हैं , किन्तु साधक स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म भी है, इतना सूक्ष्म कि जिसका आकार प्रकार स्थूल से कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है । साधक के उसी सूक्ष्म अन्तर् में उक्त प्रश्न का सही समाधान प्राप्त हो सकता है।
आचार्य संघदास गणी एक रूपक के द्वारा प्रस्तुत प्रश्न का बड़ा ही सुन्दर समाधान उपस्थित करते हैं-"एक यात्री किसी अभीष्ट लक्ष्य की ओर त्वरित गति से चला जा रहा है। वह यथाशक्ति शीघ्र गति से दौड़ता है, ताकि शीघ्र ही गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाए। परन्तु चलता हुआ थक जाता है, आगे मार्ग की और अधिक विषमतामों के कारण चल नहीं पाता है, अतः वह बीच में कहीं विश्राम करने लग जाता है। यदि वह यात्री अपने अह के कारण उचित विश्राम न करे, क्लान्त होने पर भी हठात् चलता ही रहे, तो स्वस्थ नहीं रह सकता। कुछ दूर जाकर, वह इतना अधिक क्लान्त हो जाएगा कि अवश्य ही मूर्छा खाकर गिर पड़ेगा । संभव है, प्राणान्त भी हो जाए। ऐसी स्थिति में, जिस लक्ष्य के लिए तन-तोड़ दौड़ धूप की जा रही
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org