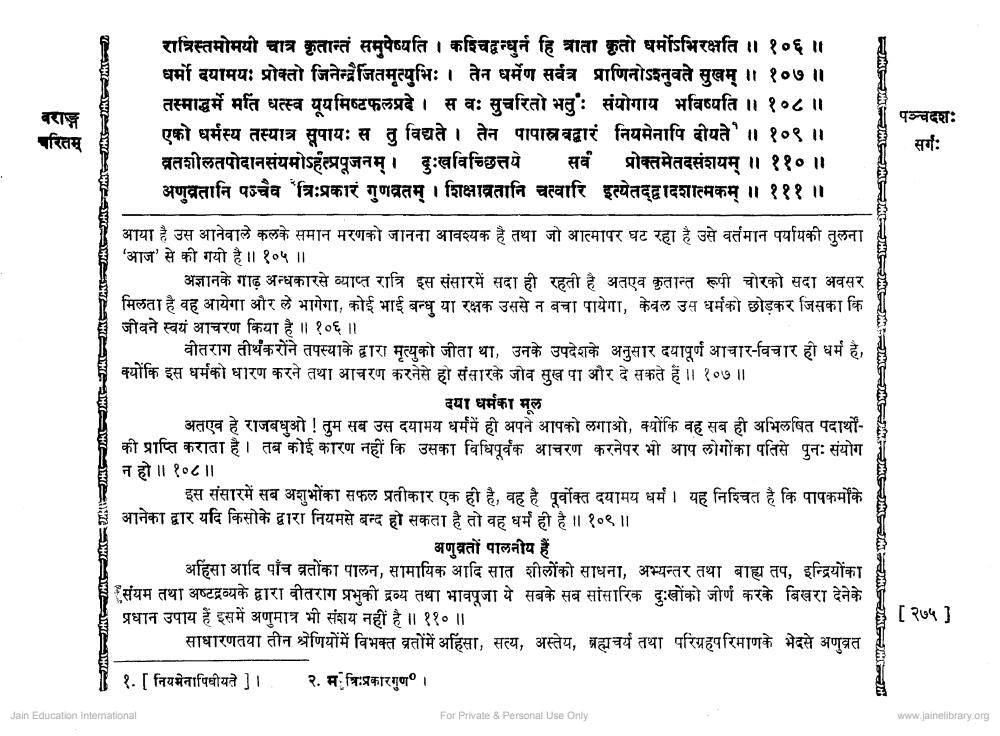________________
बराङ्ग चरितम्
= S
रात्रिस्तमोमयी चात्र कृतान्तं समुपेष्यति । कश्चिद्वन्धुर्न हि त्राता कृतो धर्मोऽभिरक्षति ।। धर्मो दयामयः प्रोक्तो जिनेन्द्रजितमृत्युभिः । तेन धर्मेण सर्वत्र प्राणिनोऽश्नुवते सुखम् ॥ तस्माद्धर्मे धत्स्व यूयमिष्टफलप्रदे । स वः सुचरितो भतुः संयोगाय भविष्यति ॥ एको धर्मस्य तस्यात्र सुपायः स तु विद्यते । तेन पापात्रबद्वारं नियमेनापि दीयते ॥ व्रतशीलतपोदान संयमोऽहंत्प्रपूजनम् । दुःखविच्छित्तये सर्व प्रोक्तमेतदसंशयम् ॥ अणुव्रतानि पञ्चैव त्रिःप्रकारं गुणव्रतम् । शिक्षाव्रतानि चत्वारि इत्येतद्द्द्वादशात्मकम् ॥ १११ ॥
११० ॥
आया है उस आनेवाले कलके समान मरणको जानना आवश्यक है तथा जो आत्मापर घट रहा है उसे वर्तमान पर्यायकी तुलना 'आज' से की गयी है ।। १०५ ।।
१०६ ।।
१०७ ॥
१०८ ॥
१०९ ॥
अज्ञानके गाढ़ अन्धकारसे व्याप्त रात्रि इस संसार में सदा ही रहती है अतएव कृतान्त रूपी चोरको सदा अवसर मिलता है वह आयेगा और ले भागेगा, कोई भाई बन्धु या रक्षक उससे न बचा पायेगा, केवल उस धर्मको छोड़कर जिसका कि जीवने स्वयं आचरण किया है ।। १०६ ।।
वीतराग तीर्थंकरोंने तपस्याके द्वारा मृत्युको जीता था, उनके उपदेशके अनुसार दयापूर्ण आचार-विचार ही धर्म है, क्योंकि इस धर्मको धारण करने तथा आचरण करनेसे हो संसारके जोव सुख पा और दे सकते हैं ।। १०७ ।।
दया धर्मका मूल
अतएव हे राजबधुओ ! तुम सब उस दयामय धर्मं में ही अपने आपको लगाओ, क्योंकि वह सब ही अभिलषित पदार्थोंप्राप्ति कराता है । तब कोई कारण नहीं कि उसका विधिपूर्वक आचरण करनेपर भी आप लोगोंका पतिसे पुनः संयोग न हो ॥ १०८ ॥
इस संसार में सब अशुभोंका सफल प्रतीकार एक ही है, वह है पूर्वोक्त दयामय धर्मं । यह निश्चित है कि पापकर्मो के आनेका द्वार यदि किसके द्वारा नियमसे बन्द हो सकता है तो वह धर्म ही है ।। १०९ ।।
Jain Education International
अणुव्रतों पालनीय हैं।
अहिंसा आदि पाँच व्रतोंका पालन, सामायिक आदि सात शीलोंको साधना, अभ्यन्तर तथा बाह्य तप, इन्द्रियोंका संयम तथा अष्टद्रव्यके द्वारा वीतराग प्रभुकी द्रव्य तथा भावपूजा ये सबके सब सांसारिक दुःखोंको जीर्णं करके बिखरा देने के प्रधान उपाय हैं इसमें अणुमात्र भी संशय नहीं है ।। ११० ।।
साधारणतया तीन श्रेणियों में विभक्त व्रतों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रहपरिमाणके भेदसे अणुव्रत
१. [ नियमेनाविधीयते ] | २. त्रिःप्रकार गुण ।
For Private Personal Use Only
पञ्चदशः
सर्गः
[ २७५ ]
www.jainelibrary.org