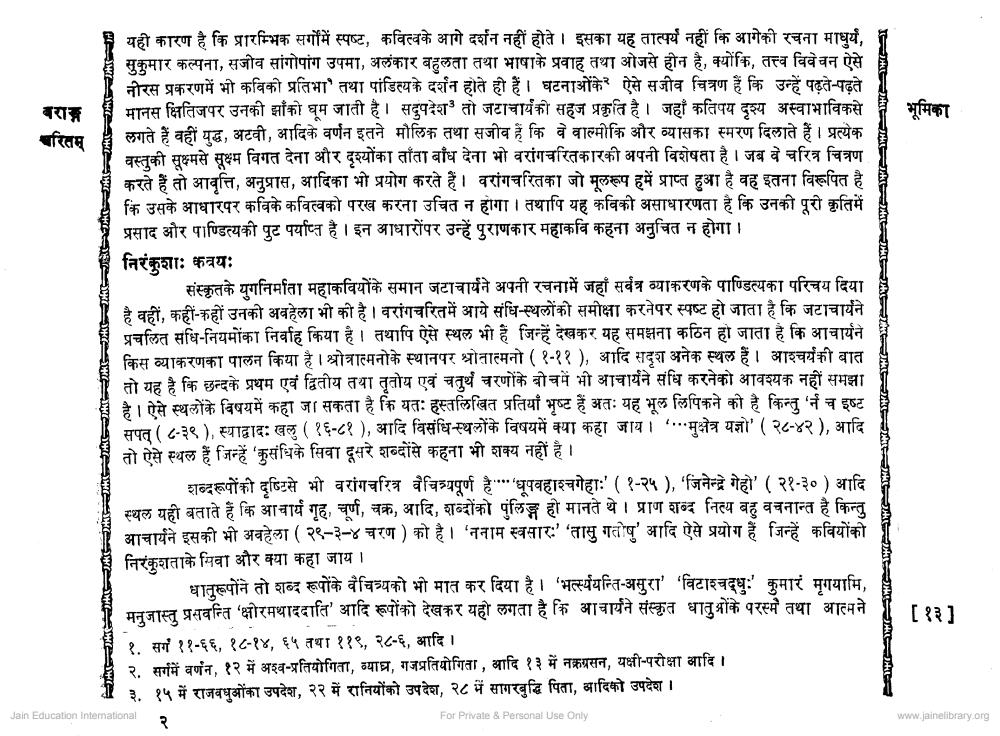________________
बराङ्ग चरितम्
यही कारण है कि प्रारम्भिक सर्गों में स्पष्ट, कवित्वके आगे दर्शन नहीं होते। इसका यह तात्पर्य नहीं कि आगेकी रचना माधुर्य, न सुकुमार कल्पना, सजीव सांगोपांग उपमा, अलंकार बहुलता तथा भाषाके प्रवाह तथा ओजसे होन है, क्योंकि, तत्त्व विवेचन ऐसे नीरस प्रकरणमें भी कविको प्रतिभा तथा पांडित्यके दर्शन होते ही हैं। घटनाओंके ऐसे सजीव चित्रण हैं कि उन्हें पढ़ते-पढ़ते मानस क्षितिजपर उनकी झाँको घूम जाती है। सदुपदेश' तो जटाचार्यको सहज प्रकृति है। जहाँ कतिपय दृश्य अस्वाभाविकसे । भूमिका लगत लगते हैं वहीं युद्ध, अटवी, आदिके वर्णन इतने मौलिक तथा सजीव है कि वे वाल्मीकि और व्यासका स्मरण दिलाते हैं। प्रत्येक वस्तुकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म विगत देना और दृश्योंका ताँता बाँध देना भो वरांगचरितकारकी अपनी विशेषता है । जब वे चरित्र चित्रण करते हैं तो आवृत्ति, अनुप्रास, आदिका भी प्रयोग करते हैं। वरांगचरितका जो मूलरूप हमें प्राप्त हुआ है वह इतना विरूपित है कि उसके आधारपर कविके कवित्वको परख करना उचित न होगा । तथापि यह कविकी असाधारणता है कि उनकी पूरी कृतिमें प्रसाद और पाण्डित्यकी पुट पर्याप्त है । इन आधारोंपर उन्हें पुराणकार महाकवि कहना अनुचित न होगा। निरंकुशाः कवयः
संस्कृतके युगनिर्माता महाकवियोंके समान जटाचार्यने अपनी रचनामें जहाँ सर्वत्र व्याकरणके पाण्डित्यका परिचय दिया है वहीं, कहीं-कहीं उनको अबहेला भी की है। वरांगचरितमें आये संधि-स्थलोंकी समीक्षा करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि जटाचार्यने प्रचलित संधि-नियमोंका निर्वाह किया है। तथापि ऐसे स्थल भी हैं जिन्हें देखकर यह समझना कठिन हो जाता है कि आचार्यने किस व्याकरणका पालन किया है । श्रोत्राल्मनोके स्थानपर श्रोतात्मनो (१-११), आदि सदृश अनेक स्थल हैं। आश्चर्यकी बात तो यह है कि छन्दके प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणोंके बीच में भी आचार्यने संधि करनेको आवश्यक नहीं समझा है। ऐसे स्थलोंके विषयमें कहा जा सकता है कि यतः हस्तलिखित प्रतियाँ भृष्ट हैं अतः यह भूल लिपिकने को है किन्तु 'नं च इष्ट सपत ( ८-३९), स्याद्वादः खलु (१६-८१), आदि विसंधि-स्थलोंके विषयमें क्या कहा जाय । '.."मुक्षेत्र यज्ञो' ( २८-४२), आदि तो ऐसे स्थल हैं जिन्हें 'कुसंधिके सिवा दूसरे शब्दोंसे कहना भी शक्य नहीं है। - शब्दरूपोंकी दृष्टिसे भी वरांगचरित्र वैचित्र्यपूर्ण है 'धूपवहाश्चगेहाः' (१-२५ ), 'जिनेन्द्र गेहो' ( २१-३०) आदि स्थल यही बताते हैं कि आचार्य गृह, चूर्ण, चक्र, आदि, शब्दोंको पुंलिङ्ग हो मानते थे। प्राण शब्द नित्य बहु वचनान्त है किन्तु आचार्यने इसकी भी अवहेला ( २९-३-४ चरण ) को है। 'ननाम स्वसारः' 'तासु गतोषु' आदि ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें कवियोंको निरंकुशताके सिवा और क्या कहा जाय ।।
धातुरूपोंने तो शब्द रूपोंके वैचित्र्यको भी मात कर दिया है। 'भपयन्ति-असुरा' 'विटाश्चधुः' कुमारं मृगयामि, मनजास्तू प्रसवन्ति क्षीरमथाददाति' आदि रूपोंको देखकर यही लगता है कि आचार्यने संस्कृत धातुओंके परस्मै तथा आत्मने
[१३] १. सर्ग ११-६६, १८-१४, ६५ तथा ११९, २८-६, आदि ।
२. सर्गमें वर्णन, १२ में अश्व-प्रतियोगिता, व्याघ्र, गजप्रतियोगिता, आदि १३ में नक्रासन, यक्षी-परीक्षा आदि । 1 ३. १५ में राजवधुओंका उपदेश, २२ में रानियोंको उपदेश, २८ में सागरबुद्धि पिता, आदिको उपदेश ।
For Private & Personal Use Only
mawareneumsprese
arera
Jain Education International
www.jainelibrary.org