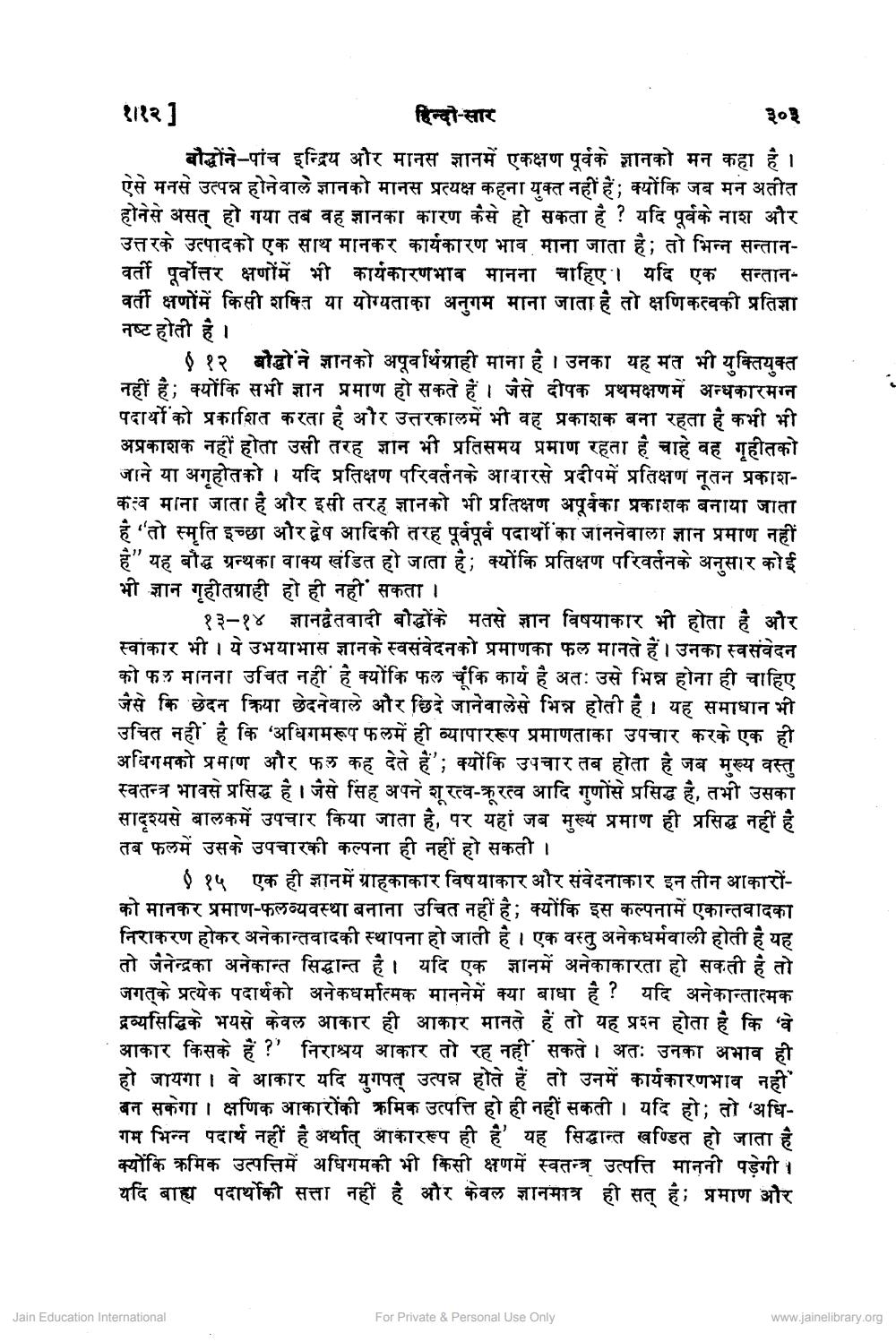________________
१।१२]
हिन्दो-सार बौद्धोंने-पांच इन्द्रिय और मानस ज्ञानमें एकक्षण पूर्वके ज्ञानको मन कहा है। ऐसे मनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मानस प्रत्यक्ष कहना युक्त नहीं हैं; क्योंकि जब मन अतीत होनेसे असत् हो गया तब वह ज्ञानका कारण कैसे हो सकता है ? यदि पूर्वके नाश और उत्तरके उत्पादको एक साथ मानकर कार्यकारण भाव माना जाता है; तो भिन्न सन्तानवर्ती पूर्वोत्तर क्षणोंमें भी कार्यकारणभाव मानना चाहिए। यदि एक सन्तानवर्ती क्षणोंमें किसी शक्ति या योग्यताका अनुगम माना जाता है तो क्षणिकत्वकी प्रतिज्ञा नष्ट होती है।
६१२ बौद्धों ने ज्ञानको अपूर्थिग्राही माना है । उनका यह मत भी युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि सभी ज्ञान प्रमाण हो सकते हैं। जैसे दीपक प्रथमक्षणमें अन्धकारमग्न पदार्थों को प्रकाशित करता है और उत्तरकालमें भी वह प्रकाशक बना रहता है कभी भी अप्रकाशक नहीं होता उसी तरह ज्ञान भी प्रतिसमय प्रमाण रहता है चाहे वह गृहीतको जाने या अगृहोतको। यदि प्रतिक्षण परिवर्तनके आवारसे प्रदीप में प्रतिक्षण नूतन प्रकाशकत्व माना जाता है और इसी तरह ज्ञानको भी प्रतिक्षण अपूर्वका प्रकाशक बनाया जाता है 'तो स्मृति इच्छा और द्वेष आदिकी तरह पूर्वपूर्व पदार्थो का जाननेवाला ज्ञान प्रमाण नहीं है" यह बौद्ध ग्रन्थका वाक्य खंडित हो जाता है; क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तनके अनुसार कोई भी ज्ञान गृहीतग्राही हो ही नहीं सकता।
१३-१४ ज्ञानद्वैतवादी बौद्धोंके मतसे ज्ञान विषयाकार भी होता है और स्वांकार भी। ये उभयाभास ज्ञानके स्वसंवेदनको प्रमाणका फल मानते हैं। उनका स्वसंवेदन को फल मानना उचित नहीं है क्योंकि फल चूंकि कार्य है अतः उसे भिन्न होना ही चाहिए जैसे कि छेदन क्रिया छेदनेवाले और छिदे जानेवालेसे भिन्न होती है। यह समाधान भी उचित नहीं है कि 'अधिगमरूप फलमें ही व्यापाररूप प्रमाणताका उपचार करके एक ही अधिगमको प्रमाण और फल कह देते हैं'; क्योंकि उपचार तब होता है जब मुख्य वस्तु स्वतन्त्र भावसे प्रसिद्ध है। जैसे सिंह अपने शूरत्व-क्रूरत्व आदि गुणोंसे प्रसिद्ध है, तभी उसका सादृश्यसे बालकमें उपचार किया जाता है, पर यहां जब मुख्य प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं है तब फलमें उसके उपचारकी कल्पना ही नहीं हो सकती।
१५ एक ही ज्ञानमें ग्राहकाकार विषयाकार और संवेदनाकार इन तीन आकारोंको मानकर प्रमाण-फलव्यवस्था बनाना उचित नहीं है; क्योंकि इस कल्पनामें एकान्तवादका निराकरण होकर अनेकान्तवादकी स्थापना हो जाती है । एक वस्तु अनेकधर्मवाली होती है यह तो जनेन्द्रका अनेकान्त सिद्धान्त है। यदि एक ज्ञानमें अनेकाकारता हो सकती है तो जगत्के प्रत्येक पदार्थको अनेकधर्मात्मक माननेमें क्या बाधा है ? यदि अनेकान्तात्मक द्रव्यसिद्धिके भयसे केवल आकार ही आकार मानते हैं तो यह प्रश्न होता है कि वे आकार किसके हैं ?' निराश्रय आकार तो रह नहीं सकते। अतः उनका अभाव ही हो जायगा। वे आकार यदि युगपत् उत्पन्न होते हैं तो उनमें कार्यकारणभाव नहीं' बन सकेगा। क्षणिक आकारोंकी क्रमिक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यदि हो; तो 'अधिगम भिन्न पदार्थ नहीं है अर्थात् आकाररूप ही है' यह सिद्धान्त खण्डित हो जाता है क्योंकि क्रमिक उत्पत्तिमें अधिगमकी भी किसी क्षणमें स्वतन्त्र उत्पत्ति माननी पड़ेगी। यदि बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं है और केवल ज्ञानमात्र ही सत् है; प्रमाण और
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org