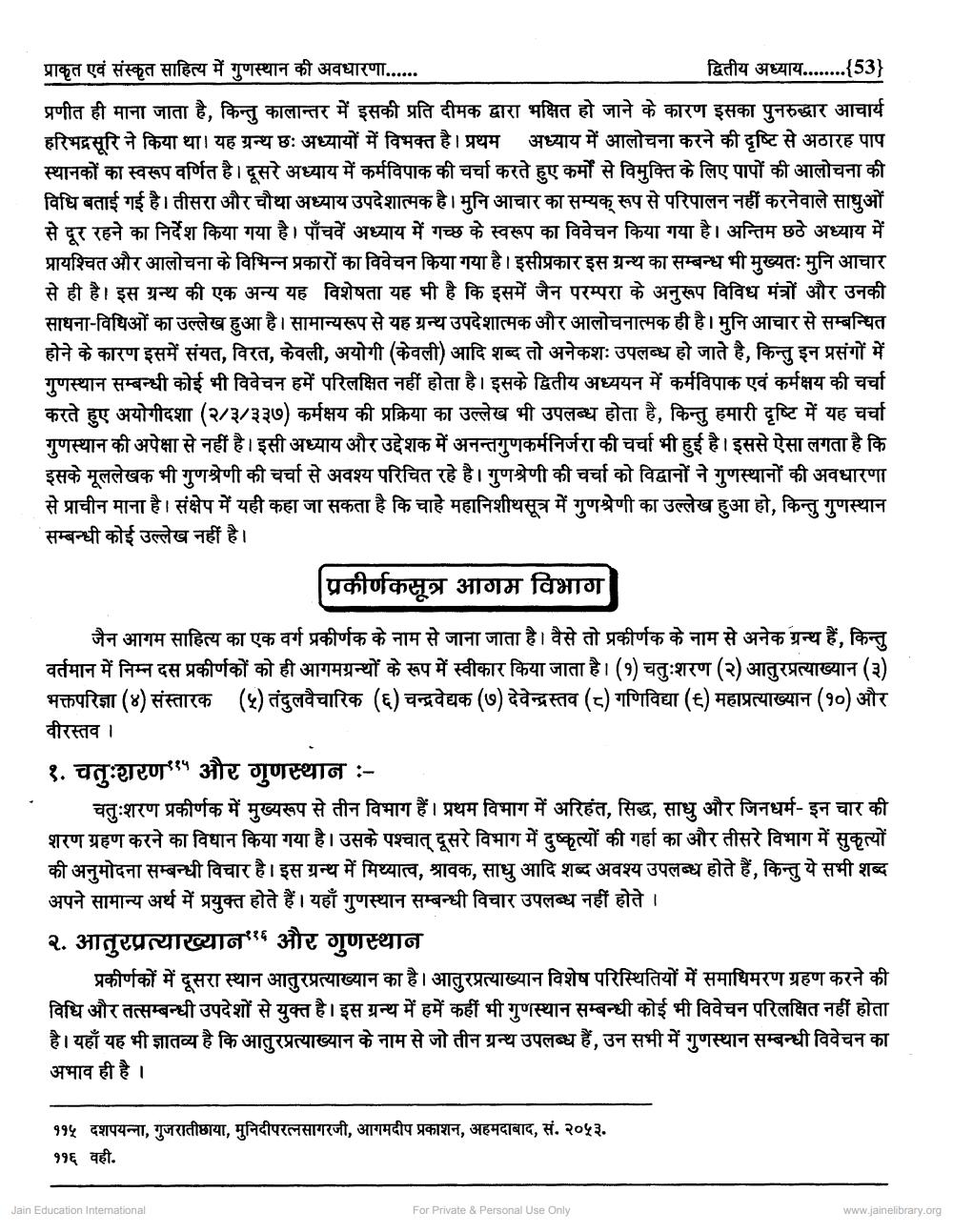________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा......
द्वितीय अध्याय........{53}
प्रणीत ही माना जाता है, किन्तु कालान्तर में इसकी प्रति दीमक द्वारा भक्षित हो जाने के कारण इसका पुनरुद्धार आचार्य हरिभद्रसूरि ने किया था। यह ग्रन्थ छः अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में आलोचना करने की दृष्टि से अठारह पाप स्थानकों का स्वरूप वर्णित है। दूसरे अध्याय में कर्मविपाक की चर्चा करते हुए कर्मों से विमुक्ति के लिए पापों की आलोचना की विधि बताई गई है। तीसरा और चौथा अध्याय उपदेशात्मक है। मुनि आचार का सम्यक् रूप से परिपालन नहीं करनेवाले साधुओं से दूर रहने का निर्देश किया गया है। पाँचवें अध्याय में गच्छ के स्वरूप का विवेचन किया गया है। अन्तिम छठे अध्याय में प्रायश्चित और आलोचना के विभिन्न प्रकारों का विवेचन किया गया है। इसीप्रकार इस ग्रन्थ का सम्बन्ध भी मुख्यतःमुनि आचार से ही है। इस ग्रन्थ की एक अन्य यह विशेषता यह भी है कि इसमें जैन परम्परा के अनुरूप विविध मंत्रों और उनकी साधना-विधिओं का उल्लेख हुआ है। सामान्यरूप से यह ग्रन्थ उपदेशात्मक और आलोचनात्मक ही है। मुनि आचार से सम्बन्धित होने के कारण इसमें संयत, विरत, केवली, अयोगी (केवली) आदि शब्द तो अनेकशः उपलब्ध हो जाते है, किन्तु इन प्रसंगों में गुणस्थान सम्बन्धी कोई भी विवेचन हमें परिलक्षित नहीं होता है। इसके द्वितीय अध्ययन में कर्मविपाक एवं कर्मक्षय की चर्चा करते हुए अयोगीदशा (२/३/३३७) कर्मक्षय की प्रक्रिया का उल्लेख भी उपलब्ध होता है, किन्तु हमारी दृष्टि में यह चर्चा गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं है। इसी अध्याय और उद्देशक में अनन्तगुणकर्मनिर्जरा की चर्चा भी हुई है। इससे ऐसा लगता है कि इसके मूललेखक भी गुणश्रेणी की चर्चा से अवश्य परिचित रहे है। गुणश्रेणी की चर्चा को विद्वानों ने गुणस्थानों की अवधारणा से प्राचीन माना है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि चाहे महानिशीथसूत्र में गुणश्रेणी का उल्लेख हुआ हो, किन्तु गुणस्थान सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं है।
प्रकीर्णकसूत्र आगम विभाग जैन आगम साहित्य का एक वर्ग प्रकीर्णक के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रकीर्णक के नाम से अनेक ग्रन्थ हैं, किन्तु वर्तमान में निम्न दस प्रकीर्णकों को ही आगमग्रन्थों के रूप में स्वीकार किया जाता है। (१) चतुःशरण (२) आतुरप्रत्याख्यान (३) भक्तपरिज्ञा (४) संस्तारक (५) तंदुलवैचारिक (६) चन्द्रवेद्यक (७) देवेन्द्रस्तव (८) गणिविद्या (६) महाप्रत्याख्यान (१०) और वीरस्तव । १. चतुःशरण५ और गुणस्थान :
चतुःशरण प्रकीर्णक में मुख्यरूप से तीन विभाग हैं। प्रथम विभाग में अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिनधर्म- इन चार की शरण ग्रहण करने का विधान किया गया है। उसके पश्चात् दूसरे विभाग में दुष्कृत्यों की गर्दा का और तीसरे विभाग में सुकृत्यों की अनुमोदना सम्बन्धी विचार है। इस ग्रन्थ में मिथ्यात्व, श्रावक, साधु आदि शब्द अवश्य उपलब्ध होते हैं, किन्तु ये सभी शब्द अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ गुणस्थान सम्बन्धी विचार उपलब्ध नहीं होते। २. आतुरप्रत्याख्यान और गुणस्थान
प्रकीर्णकों में दूसरा स्थान आतुरप्रत्याख्यान का है। आतुरप्रत्याख्यान विशेष परिस्थितियों में समाधिमरण ग्रहण करने की विधि और तत्सम्बन्धी उपदेशों से युक्त है। इस ग्रन्थ में हमें कहीं भी गुणस्थान सम्बन्धी कोई भी विवेचन परिलक्षित नहीं होता है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि आतुरप्रत्याख्यान के नाम से जो तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उन सभी में गुणस्थान सम्बन्धी विवेचन का अभाव ही है।
११५ दशपयन्ना, गुजरातीछाया, मुनिदीपरत्नसागरजी, आगमदीप प्रकाशन, अहमदाबाद, सं. २०५३. ११६ वही.
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org