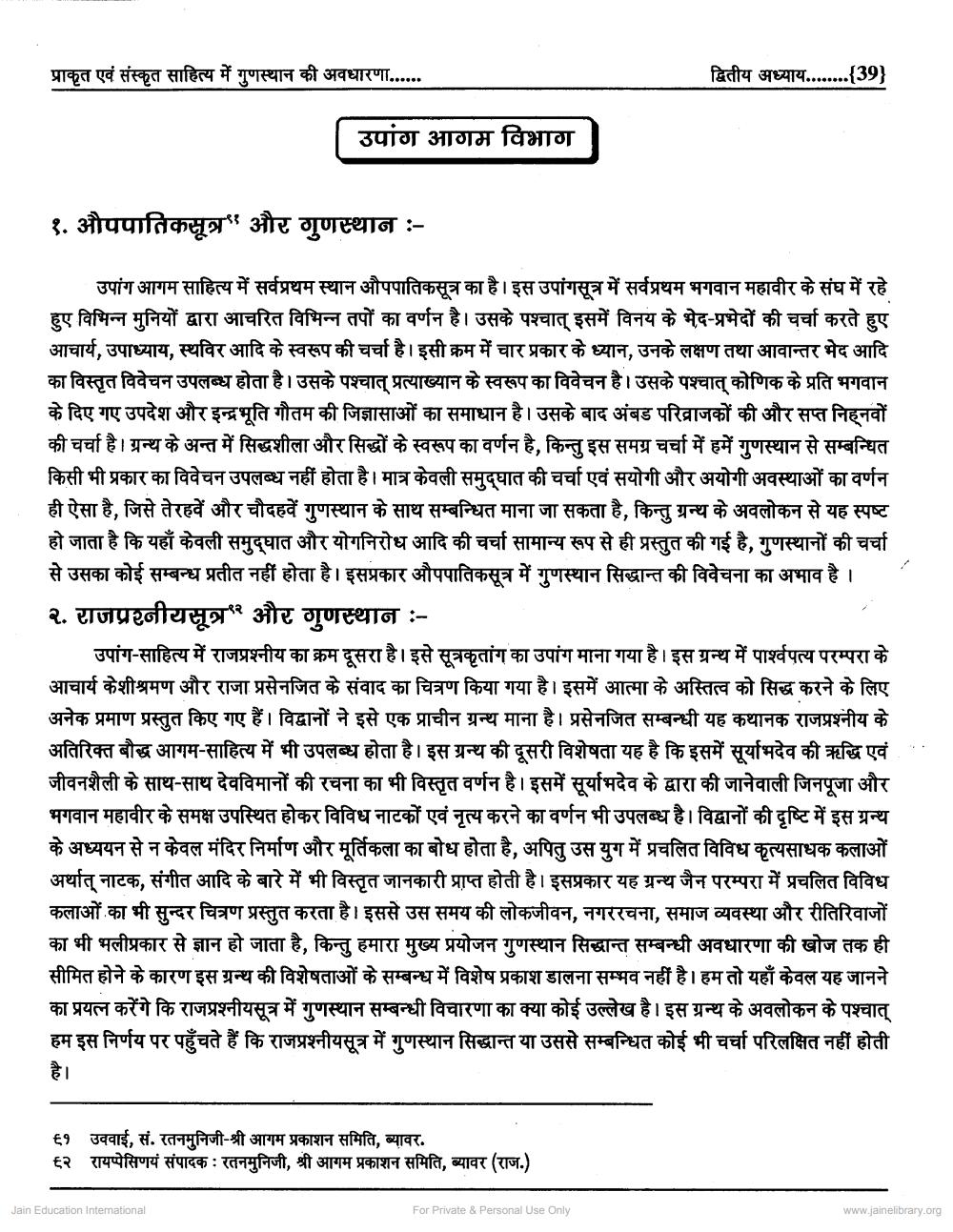________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा..
द्वितीय अध्याय........{39)
| उपांग आगम विभाग |
१. औपपातिकसूत्र और गुणस्थान :
उपांग आगम साहित्य में सर्वप्रथम स्थान औपपातिकसूत्र का है। इस उपांगसूत्र में सर्वप्रथम भगवान महावीर के संघ में रहे हुए विभिन्न मुनियों द्वारा आचरित विभिन्न तपों का वर्णन है। उसके पश्चात् इसमें विनय के भेद-प्रभेदों की चर्चा करते हुए आचार्य, उपाध्याय, स्थविर आदि के स्वरूप की चर्चा है। इसी क्रम में चार प्रकार के ध्यान, उनके लक्षण तथा आवान्तर भेद आदि का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। उसके पश्चात् प्रत्याख्यान के स्वरूप का विवेचन है। उसके पश्चात् कोणिक के प्रति भगवान के दिए गए उपदेश और इन्द्रभूति गौतम की जिज्ञासाओं का समाधान है। उसके बाद अंबड परिव्राजकों की और सप्त निह्नवों की चर्चा है। ग्रन्थ के अन्त में सिद्धशीला और सिद्धों के स्वरूप का वर्णन है, किन्तु इस समग्र चर्चा में हमें गुणस्थान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवेचन उपलब्ध नहीं होता है। मात्र केवली समुद्घात की चर्चा एवं सयोगी और अयोगी अवस्थाओं का वर्णन ही ऐसा है, जिसे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान के साथ सम्बन्धित माना जा सकता है, किन्तु ग्रन्थ के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ केवली समुद्घात और योगनिरोध आदि की चर्चा सामान्य रूप से ही प्रस्तुत की गई है, गुणस्थानों की चर्चा से उसका कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है। इसप्रकार औपपातिकसूत्र में गुणस्थान सिद्धान्त की विवेचना का अभाव है। २. राजप्रश्नीयसूत्र और गुणस्थान :
उपांग-साहित्य में राजप्रश्नीय का क्रम दूसरा है। इसे सूत्रकृतांग का उपांग माना गया है। इस ग्रन्थ में पार्श्वपत्य परम्परा के आचार्य केशीश्रमण और राजा प्रसेनजित के संवाद का चित्रण किया गया है। इसमें आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। विद्वानों ने इसे एक प्राचीन ग्रन्थ माना है। प्रसेनजित सम्बन्धी यह कथानक राजप्रश्नीय के अतिरिक्त बौद्ध आगम-साहित्य में भी उपलब्ध होता है। इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें सय
री विशेषता यह है कि इसमें सूर्याभदेव की ऋद्धि एवं जीवनशैली के साथ-साथ देवविमानों की रचना का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें सूर्याभदेव के द्वारा की जानेवाली जिनपूजा और भगवान महावीर के समक्ष उपस्थित होकर विविध नाटकों एवं नृत्य करने का वर्णन भी उपलब्ध है। विद्वानों की दृष्टि में इस ग्रन्थ के अध्ययन से न केवल मंदिर निर्माण और मूर्तिकला का बोध होता है, अपितु उस युग में प्रचलित विविध कृत्यसाधक कलाओं अर्थात् नाटक, संगीत आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसप्रकार यह ग्रन्थ जैन परम्परा में प्रचलित विविध कलाओं का भी सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करता है। इससे उस समय की लोकजीवन, नगररचना, समाज व्यवस्था और रीतिरिवाजों का भी भलीप्रकार से ज्ञान हो जाता है, किन्तु हमारा मुख्य प्रयोजन गुणस्थान सिद्धान्त सम्बन्धी अवधारणा की खोज तक ही सीमित होने के कारण इस ग्रन्थ की विशेषताओं के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालना सम्भव नहीं है। हम तो यहाँ केवल यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि राजप्रश्नीयसूत्र में गुणस्थान सम्बन्धी विचारणा का क्या कोई उल्लेख है। इस ग्रन्थ के अवलोकन के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि राजप्रश्नीयसूत्र में गुणस्थान सिद्धान्त या उससे सम्बन्धित कोई भी चर्चा परिलक्षित नहीं होती
है।
६१ उववाई, सं. रतनमुनिजी-श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर. ६२ रायप्पेसिणयं संपादक : रतनमुनिजी, श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर (राज.)
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org