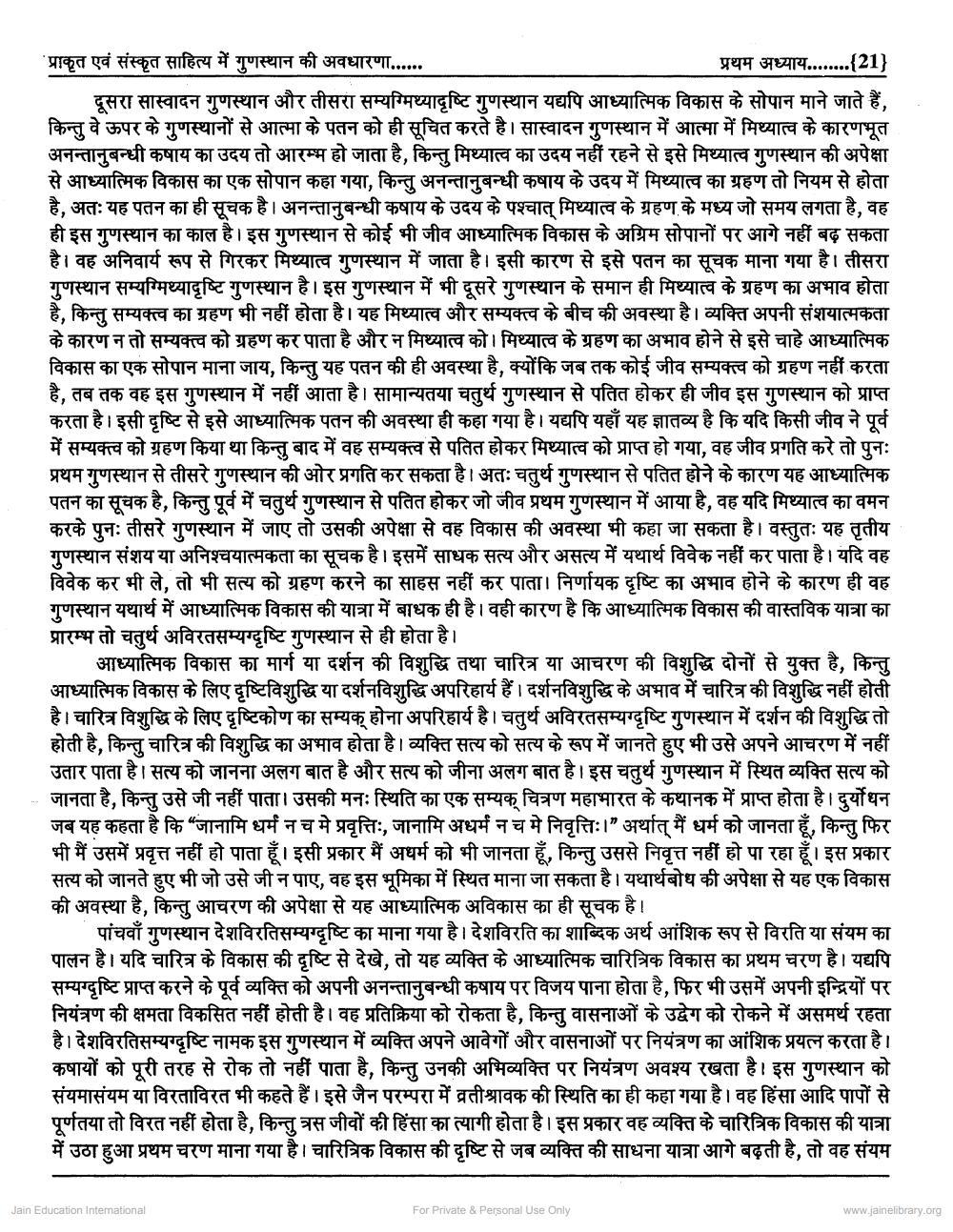________________
'प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा......
प्रथम अध्याय........{21} दूसरा सास्वादन गुणस्थान और तीसरा सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थान यद्यपि आध्यात्मिक विकास के सोपान माने जाते हैं. किन्तु वे ऊपर के गुणस्थानों से आत्मा के पतन को ही सूचित करते है। सास्वादन गुणस्थान में आत्मा में मिथ्यात्व के कारणभूत अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय तो आरम्भ हो जाता है, किन्तु मिथ्यात्व का उदय नहीं रहने से इसे मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा से आध्यात्मिक विकास का एक सोपान कहा गया, किन्तु अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय में मिथ्यात्व का ग्रहण तो नियम से होता है, अतः यह पतन का ही सूचक है। अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय के पश्चात् मिथ्यात्व के ग्रहण के मध्य जो समय लगता है, वह ही इस गुणस्थान का काल है। इस गुणस्थान से कोई भी जीव आध्यात्मिक विकास के अग्रिम सोपानों पर आगे नहीं बढ़ सकता है। वह अनिवार्य रूप से गिरकर मिथ्यात्व गुणस्थान में जाता है। इसी कारण से इसे पतन का सूचक माना गया है। तीसरा गुणस्थान सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है। इस गुणस्थान में भी दूसरे गुणस्थान के समान ही मिथ्यात्व के ग्रहण का अभाव होता है, किन्तु सम्यक्त्व का ग्रहण भी नहीं होता है। यह मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच की अवस्था है। व्यक्ति अपनी संशयात्मकता के कारण न तो सम्यक्त्व को ग्रहण कर पाता है और न मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व के ग्रहण का अभाव होने से इसे चाहे आध्यात्मिक विकास का एक सोपान माना जाय, किन्तु यह पतन की ही अवस्था है, क्योंकि जब तक कोई जीव सम्यक्त्व को ग्रहण नहीं करता है, तब तक वह इस गुणस्थान में नहीं आता है। सामान्यतया चतुर्थ गुणस्थान से पतित होकर ही जीव इस गुणस्थान को प्राप्त करता है। इसी दृष्टि से इसे आध्यात्मिक पतन की अवस्था ही कहा गया है। यद्यपि यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यदि किसी जीव ने पूर्व में सम्यक्त्व को ग्रहण किया था किन्तु बाद में वह सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, वह जीव प्रगति करे तो पुनः प्रथम गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान की ओर प्रगति कर सकता है। अतः चतुर्थ गुणस्थान से पतित होने के कारण यह आध्यात्मिक पतन का सूचक है, किन्तु पूर्व में चतुर्थ गुणस्थान से पतित होकर जो जीव प्रथम गुणस्थान में आया है, वह यदि मिथ्यात्व का वमन करके पुनः तीसरे गुणस्थान में जाए तो उसकी अपेक्षा से वह विकास की अवस्था भी कहा जा सकता है। वस्तुतः यह तृतीय गुणस्थान संशय या अनिश्चयात्मकता का सूचक है। इसमें साधक सत्य और असत्य में यथार्थ विवेक नहीं कर पाता है। यदि वह विवेक कर भी ले, तो भी सत्य को ग्रहण करने का साहस नहीं कर पाता। निर्णायक दृष्टि का अभाव होने के कारण ही वह गुणस्थान यथार्थ में आध्यात्मिक विकास की यात्रा में बाधक ही है। वही कारण है कि आध्यात्मिक विकास की वास्तविक यात्रा का प्रारम्भ तो चतुर्थ अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान से ही होता है।
आध्यात्मिक विकास का मार्ग या दर्शन की विशुद्धि तथा चारित्र या आचरण की विशुद्धि दोनों से युक्त है, किन्तु आध्यात्मिक विकास के लिए दृष्टिविशुद्धि या दर्शनविशुद्धि अपरिहार्य हैं। दर्शनविशुद्धि के अभाव में चारित्र की विशुद्धि नहीं होती है। चारित्र विशुद्धि के लिए दृष्टिकोण का सम्यक् होना अपरिहार्य है। चतुर्थ अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान में दर्शन की विशुद्धि तो होती है, किन्तु चारित्र की विशुद्धि का अभाव होता है। व्यक्ति सत्य को सत्य के रूप में जानते हुए भी उसे अपने आचरण में नहीं उतार पाता है। सत्य को जानना अलग बात है और सत्य को जीना अलग बात है। इस चतुर्थ गुणस्थान में स्थित व्यक्ति सत्य को जानता है, किन्तु उसे जी नहीं पाता। उसकी मनः स्थिति का एक सम्यक् चित्रण महाभारत के कथानक में प्राप्त होता है। दुर्योधन जब यह कहता है कि “जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्म न च मे निवृत्तिः।" अर्थात् मैं धर्म को जानता हूँ, किन्तु फिर भी मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता हूँ। इसी प्रकार मैं अधर्म को भी जानता हूँ, किन्तु उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। इस प्रकार सत्य को जानते हुए भी जो उसे जी न पाए, वह इस भूमिका में स्थित माना जा सकता है। यथार्थबोध की अपेक्षा से यह एक विकास की अवस्था है, किन्तु आचरण की अपेक्षा से यह आध्यात्मिक अविकास का ही सूचक है।
पांचवाँ गुणस्थान देशविरतिसम्यग्दृष्टि का माना गया है। देशविरति का शाब्दिक अर्थ आंशिक रूप से विरति या संयम का
। यदि चारित्र के विकास की दृष्टि से देखे, तो यह व्यक्ति के आध्यात्मिक चारित्रिक विकास का प्रथम चरण है। यद्यपि सम्यग्दृष्टि प्राप्त करने के पूर्व व्यक्ति को अपनी अनन्तानुबन्धी कषाय पर विजय पाना होता है, फिर भी उसमें अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण की क्षमता विकसित नहीं होती है। वह प्रतिक्रिया को रोकता है, किन्तु वासनाओं के उद्वेग को रोकने में असमर्थ रहता है। देशविरतिसम्यग्दृष्टि नामक इस गुणस्थान में व्यक्ति अपने आवेगों और वासनाओं पर नियंत्रण का आंशिक प्रयत्न करता है। कषायों को पूरी तरह से रोक तो नहीं पाता है, किन्तु उनकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण अवश्य रखता है। इस गुणस्थान को संयमासंयम या विरताविरत भी कहते हैं। इसे जैन परम्परा में व्रतीश्रावक की स्थिति का ही कहा गया है। वह हिंसा आदि पापों से पूर्णतया तो विरत नहीं होता है, किन्तु त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी होता है। इस प्रकार वह व्यक्ति के चारित्रिक विकास की यात्रा में उठा हुआ प्रथम चरण माना गया है। चारित्रिक विकास की दृष्टि से जब व्यक्ति की साधना यात्रा आगे बढ़ती है, तो वह संयम
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org