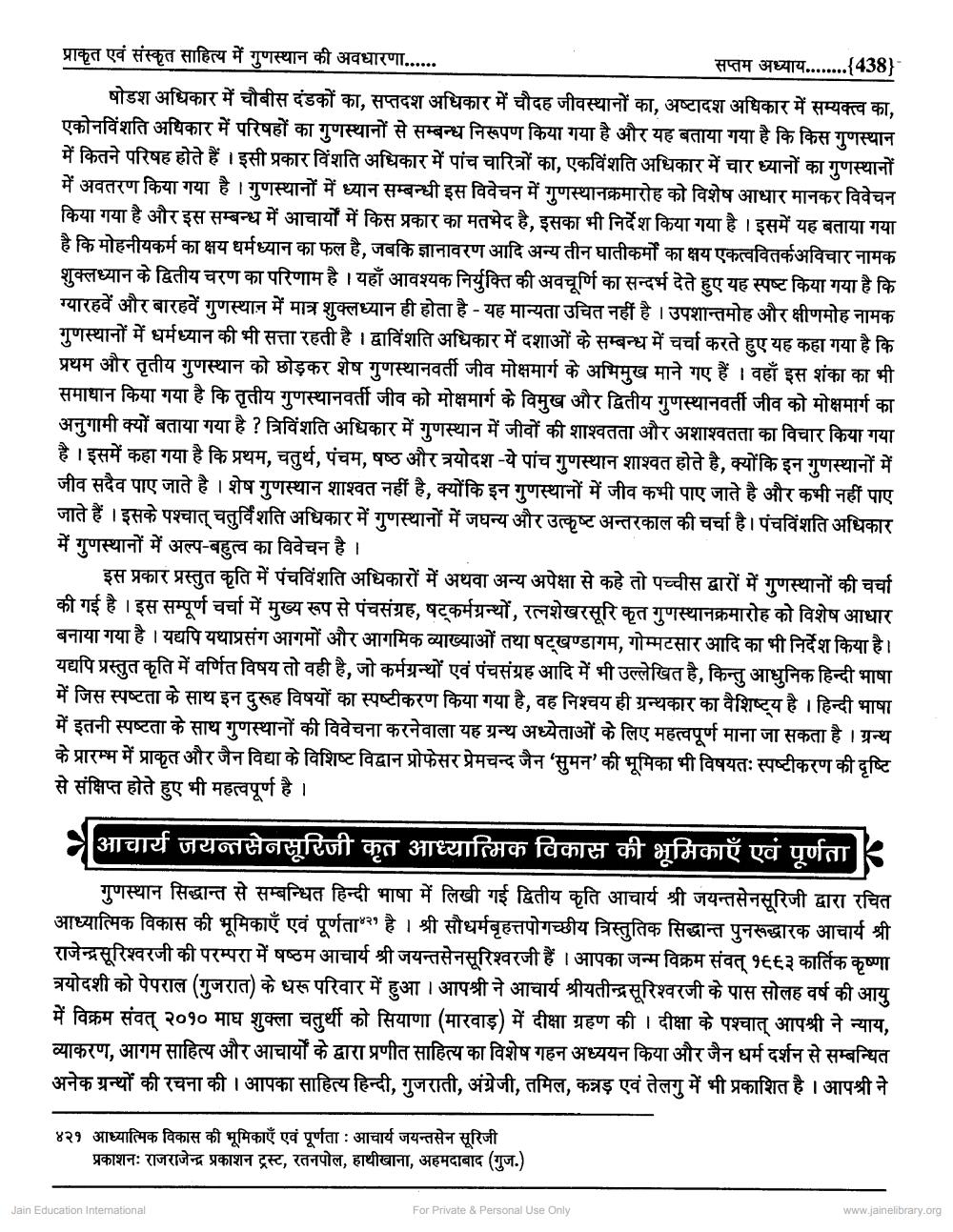________________
प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में गुणस्थान की अवधारणा...
सप्तम अध्याय........{438} ___षोडश अधिकार में चौबीस दंडकों का, सप्तदश अधिकार में चौदह जीवस्थानों का, अष्टादश अधिकार में सम्यक्त्व का, एकोनविंशति अधिकार में परिषहों का गुणस्थानों से सम्बन्ध निरूपण किया गया है और यह बताया गया है कि किस गुणस्थान में कितने परिषह होते हैं । इसी प्रकार विंशति अधिकार में पांच चारित्रों का, एकविंशति अधिकार में चार ध्यानों का गुणस्थानों में अवतरण किया गया है । गुणस्थानों में ध्यान सम्बन्धी इस विवेचन में गुणस्थानक्रमारोह को विशेष आधार मानकर विवेचन किया गया है और इस सम्बन्ध में आचार्यों में किस प्रकार का मतभेद है, इसका भी निर्देश किया गया है । इसमें यह बताया गया है कि मोहनीयकर्म का क्षय धर्मध्यान का फल है, जबकि ज्ञानावरण आदि अन्य तीन घातीकर्मों का क्षय एकत्ववितर्क शुक्लध्यान के द्वितीय चरण का परिणाम है । यहाँ आवश्यक नियुक्ति की अवचूर्णि का सन्दर्भ देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में मात्र शुक्लध्यान ही होता है - यह मान्यता उचित नहीं है । उपशान्तमोह और क्षीणमोह नामक गुणस्थानों में धर्मध्यान की भी सत्ता रहती है । द्वाविंशति अधिकार में दशाओं के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि प्रथम और तृतीय गुणस्थान को छोड़कर शेष गुणस्थानवी जीव मोक्षमार्ग के अभिमुख माने गए हैं । वहाँ इस शंका का भी समाधान किया गया है कि तृतीय गुणस्थानवी जीव को मोक्षमार्ग के विमुख और द्वितीय गुणस्थानवी जीव को मोक्षमार्ग का अनुगामी क्यों बताया गया है ? त्रिविंशति अधिकार में गुणस्थान में जीवों की शाश्वतता और अशाश्वतता का विचार किया गया है । इसमें कहा गया है कि प्रथम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और त्रयोदश -ये पांच गुणस्थान शाश्वत होते है, क्योंकि इन गुणस्थानों में जीव सदैव पाए जाते है । शेष गुणस्थान शाश्वत नहीं है, क्योंकि इन गुणस्थानों में जीव कभी पाए जाते है और कभी नहीं पाए जाते हैं । इसके पश्चात् चतुर्विंशति अधिकार में गुणस्थानों में जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल की चर्चा है। पंचविंशति अधिकार में गुणस्थानों में अल्प-बहुत्व का विवेचन है।।
इस प्रकार प्रस्तुत कृति में पंचविंशति अधिकारों में अथवा अन्य अपेक्षा से कहे तो पच्चीस द्वारों में गुणस्थानों की चर्चा की गई है । इस सम्पूर्ण चर्चा में मुख्य रूप से पंचसंग्रह, षट्कर्मग्रन्थों, रत्नशेखरसूरि कृत गुणस्थानक्रमारोह को विशेष आधार बनाया गया है । यद्यपि यथाप्रसंग आगमों और आगमिक व्याख्याओं तथा षट्खण्डागम, गोम्मटसार आदि का भी निर्देश किया है। यद्यपि प्रस्तुत कृति में वर्णित विषय तो वही है, जो कर्मग्रन्थों एवं पंचसंग्रह आदि में भी उल्लेखित है, किन्तु आधुनिक हिन्दी भाषा में जिस स्पष्टता के साथ इन दुरूह विषयों का स्पष्टीकरण किया गया है, वह निश्चय ही ग्रन्थकार का वैशिष्ट्य है । हिन्दी भाषा में इतनी स्पष्टता के साथ गुणस्थानों की विवेचना करनेवाला यह ग्रन्थ अध्येताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्राकृत और जैन विद्या के विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर प्रेमचन्द जैन 'सुमन' की भूमिका भी विषयतः स्पष्टीकरण की दृष्टि से संक्षिप्त होते हुए भी महत्वपूर्ण है ।
आचार्य जयन्तसेनसूरिजी कृत आध्यात्मिक विकास की भूमिकाएँ एवं पूर्णता
गुणस्थान सिद्धान्त से सम्बन्धित हिन्दी भाषा में लिखी गई द्वितीय कृति आचार्य श्री जयन्तसेनसूरिजी द्वारा रचित आध्यात्मिक विकास की भूमिकाएँ एवं पूर्णता है । श्री सौधर्मबृहत्तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक सिद्धान्त पुनरूद्धारक आचार्य श्री राजेन्द्रसूरिश्वरजी की परम्परा में षष्ठम आचार्य श्री जयन्तसेनसूरिश्वरजी हैं । आपका जन्म विक्रम संवत् १६६३ कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को पेपराल (गुजरात) के धरू परिवार में हुआ । आपश्री ने आचार्य श्रीयतीन्द्रसूरिश्वरजी के पास सोलह वर्ष की आयु में विक्रम संवत् २०१० माघ शुक्ला चतुर्थी को सियाणा (मारवाड़) में दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा के पश्चात् आपश्री ने न्याय, व्याकरण, आगम साहित्य और आचार्यों के द्वारा प्रणीत साहित्य का विशेष गहन अध्ययन किया और जैन धर्म दर्शन से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों की रचना की। आपका साहित्य हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़ एवं तेलगु में भी प्रकाशित है । आपश्री ने
४२१ आध्यात्मिक विकास की भूमिकाएँ एवं पूर्णता : आचार्य जयन्तसेन सूरिजी
प्रकाशनः राजराजेन्द्र प्रकाशन ट्रस्ट, रतनपोल, हाथीखाना, अहमदाबाद (गुज.)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org